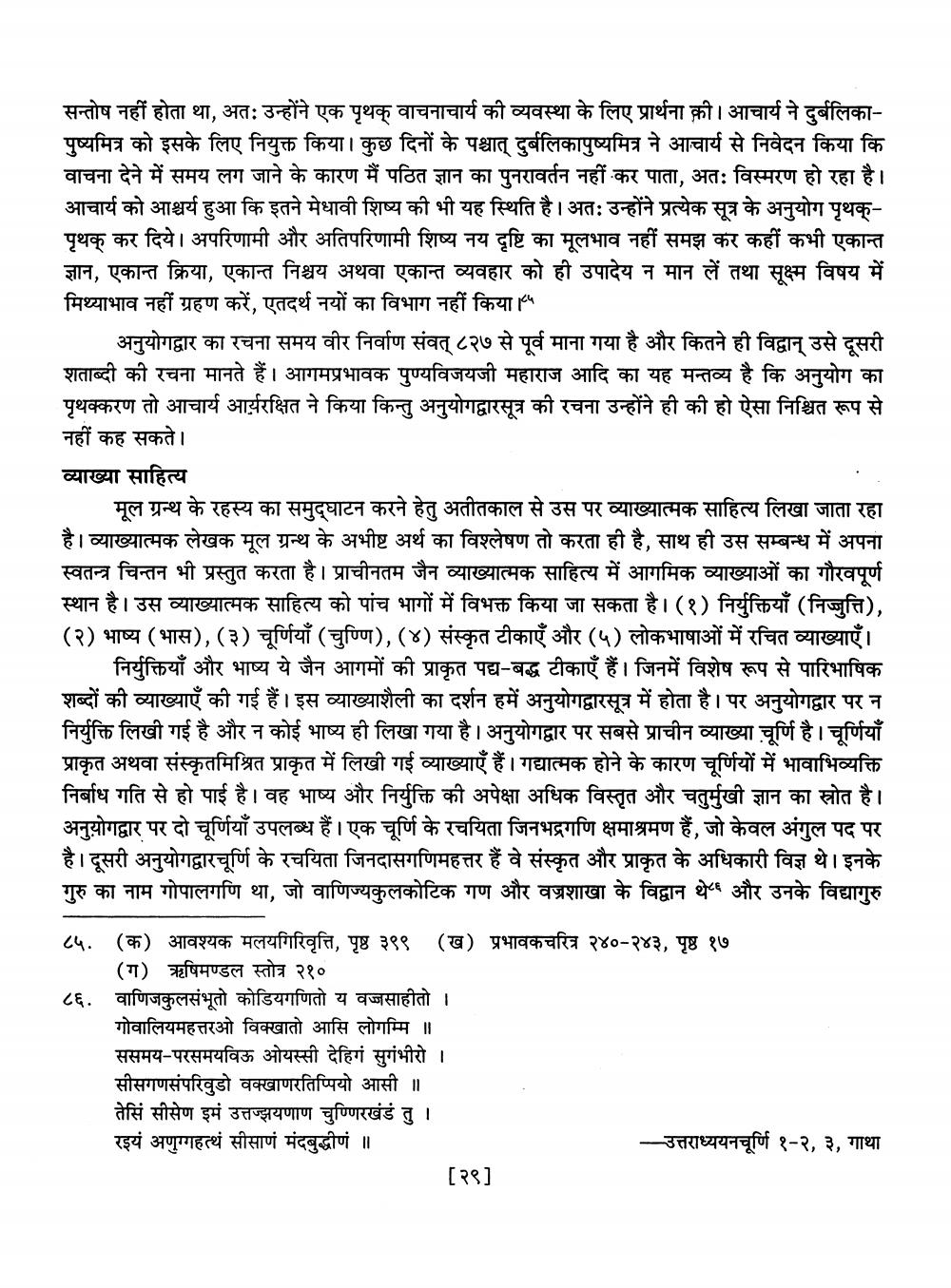________________
सन्तोष नहीं होता था, अतः उन्होंने एक पृथक् वाचनाचार्य की व्यवस्था के लिए प्रार्थना की। आचार्य ने दुर्बलिकापुष्यमित्र को इसके लिए नियुक्त किया। कुछ दिनों के पश्चात् दुर्बलिकापुष्यमित्र ने आचार्य से निवेदन किया कि वाचना देने में समय लग जाने के कारण मैं पठित ज्ञान का पुनरावर्तन नहीं कर पाता, अतः विस्मरण हो रहा है। आचार्य को आश्चर्य हुआ कि इतने मेधावी शिष्य की भी यह स्थिति है। अतः उन्होंने प्रत्येक सूत्र के अनुयोग पृथक्पृथक् कर दिये। अपरिणामी और अतिपरिणामी शिष्य नय दृष्टि का मूलभाव नहीं समझ कर कहीं कभी एकान्त ज्ञान, एकान्त क्रिया, एकान्त निश्चय अथवा एकान्त व्यवहार को ही उपादेय न मान लें तथा सूक्ष्म विषय में मिथ्याभाव नहीं ग्रहण करें, एतदर्थ नयों का विभाग नहीं किया।५।।
___ अनुयोगद्वार का रचना समय वीर निर्वाण संवत् ८२७ से पूर्व माना गया है और कितने ही विद्वान् उसे दूसरी शताब्दी की रचना मानते हैं। आगमप्रभावक पुण्यविजयजी महाराज आदि का यह मन्तव्य है कि अनुयोग का पृथक्करण तो आचार्य आरक्षित ने किया किन्तु अनुयोगद्वारसूत्र की रचना उन्होंने ही की हो ऐसा निश्चित रूप से नहीं कह सकते। व्याख्या साहित्य
मूल ग्रन्थ के रहस्य का समुद्घाटन करने हेतु अतीतकाल से उस पर व्याख्यात्मक साहित्य लिखा जाता रहा है। व्याख्यात्मक लेखक मल ग्रन्थ के अभीष्ट अर्थ का विश्लेषण तो करता ही है, साथ ही उस सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र चिन्तन भी प्रस्तुत करता है। प्राचीनतम जैन व्याख्यात्मक साहित्य में आगमिक व्याख्याओं का गौरवपूर्ण स्थान है। उस व्याख्यात्मक साहित्य को पांच भागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) नियुक्तियाँ (निज्जुत्ति), (२) भाष्य (भास), (३) चूर्णियाँ (चुण्णि), (४) संस्कृत टीकाएँ और (५) लोकभाषाओं में रचित व्याख्याएँ।
नियुक्तियाँ और भाष्य ये जैन आगमों की प्राकृत पद्य-बद्ध टीकाएँ हैं। जिनमें विशेष रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्याएँ की गई हैं। इस व्याख्याशैली का दर्शन हमें अनुयोगद्वारसूत्र में होता है। पर अनुयोगद्वार पर न नियुक्ति लिखी गई है और न कोई भाष्य ही लिखा गया है। अनुयोगद्वार पर सबसे प्राचीन व्याख्या चूर्णि है। चूर्णियाँ प्राकृत अथवा संस्कृतमिश्रित प्राकृत में लिखी गई व्याख्याएँ हैं। गद्यात्मक होने के कारण चूर्णियों में भावाभिव्यक्ति निर्बाध गति से हो पाई है। वह भाष्य और नियुक्ति की अपेक्षा अधिक विस्तृत और चतुर्मुखी ज्ञान का स्रोत है। अनुयोगद्वार पर दो चूर्णियाँ उपलब्ध हैं। एक चूर्णि के रचयिता जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं, जो केवल अंगुल पद पर है। दूसरी अनुयोगद्वारचूर्णि के रचयिता जिनदासगणिमहत्तर हैं वे संस्कृत और प्राकृत के अधिकारी विज्ञ थे। इनके गुरु का नाम गोपालगणि था, जो वाणिज्यकुलकोटिक गण और वज्रशाखा के विद्वान थे और उनके विद्यागुरु
८५. (क) आवश्यक मलयगिरिवृत्ति, पृष्ठ ३९९ (ख) प्रभावकचरित्र २४०-२४३, पृष्ठ १७
(ग) ऋषिमण्डल स्तोत्र २१० ८६. वाणिजकुलसंभूतो कोडियगणितो य वज्जसाहीतो ।
गोवालियमहत्तरओ विक्खातो आसि लोगम्मि ॥ ससमय-परसमयविऊ ओयस्सी देहिगं सुगंभीरो । सीसगणसंपरिवुडो वक्खाणरतिप्पियो आसी ॥ तेसिं सीसेण इमं उत्तज्झयणाण चुण्णिरखंडं तु । रइयं अणुग्गहत्थं सीसाणं मंदबुद्धीणं ॥
-उत्तराध्ययनचूर्णि १-२, ३, गाथा [२९]