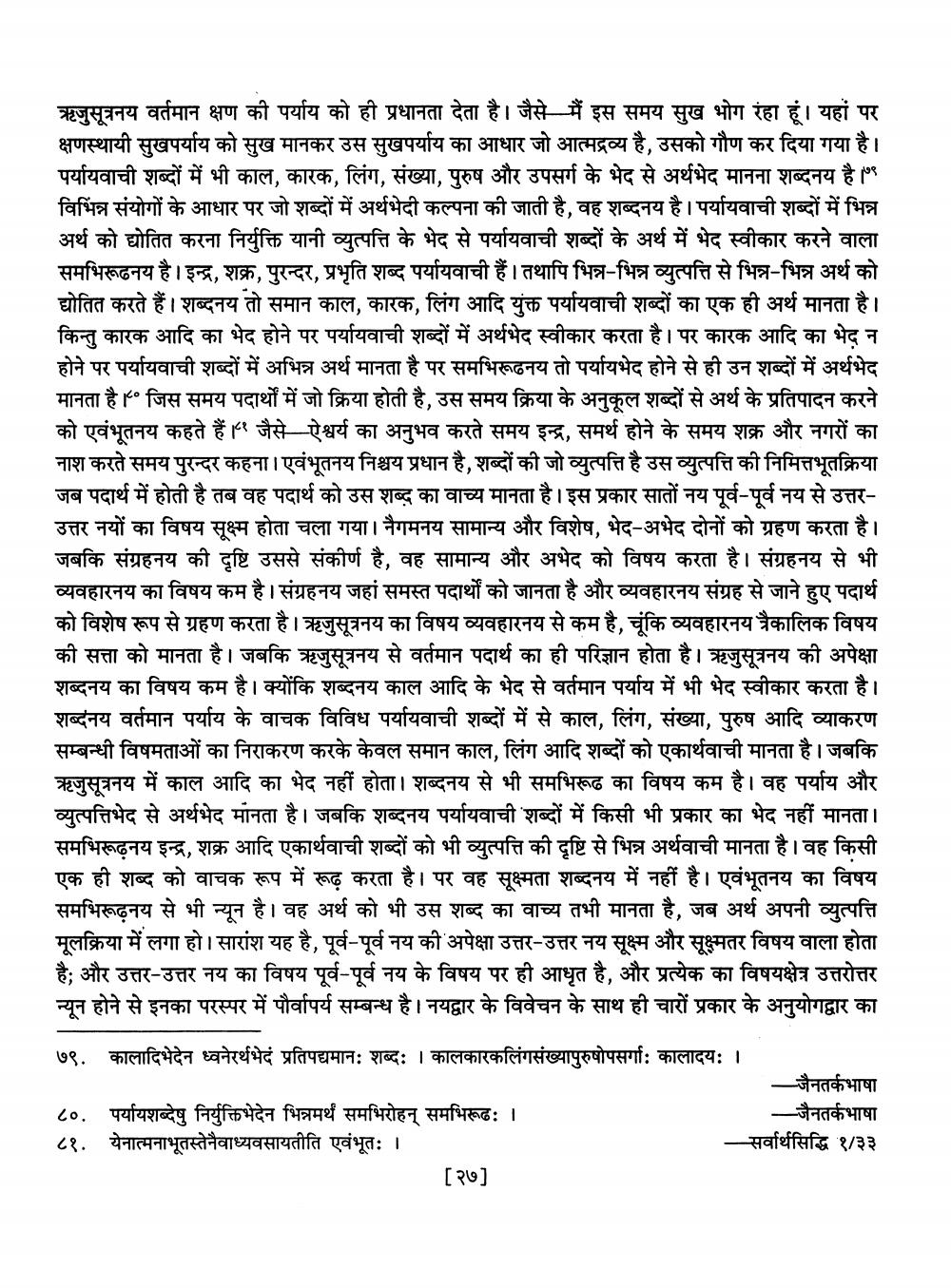________________
ऋजुसूत्रनय वर्तमान क्षण की पर्याय को ही प्रधानता देता है। जैसे मैं इस समय सुख भोग रहा हूं। यहां पर क्षणस्थायी सुखपर्याय को सुख मानकर उस सुखपर्याय का आधार जो आत्मद्रव्य है, उसको गौण कर दिया गया है। पर्यायवाची शब्दों में भी काल, कारक, लिंग, संख्या, पुरुष और उपसर्ग के भेद से अर्थभेद मानना शब्दनय है।" विभिन्न संयोगों के आधार पर जो शब्दों में अर्थभेदी कल्पना की जाती है, वह शब्दनय है। पर्यायवाची शब्दों में भिन्न अर्थ को द्योतित करना नियुक्ति यानी व्युत्पत्ति के भेद से पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में भेद स्वीकार करने वाला समभिरूढनय है। इन्द्र, शक्र, पुरन्दर, प्रभृति शब्द पर्यायवाची हैं। तथापि भिन्न-भिन्न व्युत्पत्ति से भिन्न-भिन्न अर्थ को द्योतित करते हैं। शब्दनय तो समान काल, कारक, लिंग आदि युक्त पर्यायवाची शब्दों का एक ही अर्थ मानता है। किन्तु कारक आदि का भेद होने पर पर्यायवाची शब्दों में अर्थभेद स्वीकार करता है। पर कारक आदि का भेद न होने पर पर्यायवाची शब्दों में अभिन्न अर्थ मानता है पर समभिरूढनय तो पर्यायभेद होने से ही उन शब्दों में अर्थभेद मानता है। जिस समय पदार्थों में जो क्रिया होती है, उस समय क्रिया के अनुकूल शब्दों से अर्थ के प्रतिपादन करने को एवंभूतनय कहते हैं। जैसे ऐश्वर्य का अनुभव करते समय इन्द्र, समर्थ होने के समय शक्र और नगरों का नाश करते समय पुरन्दर कहना। एवंभूतनय निश्चय प्रधान है, शब्दों की जो व्युत्पत्ति है उस व्युत्पत्ति की निमित्तभूतक्रिया जब पदार्थ में होती है तब वह पदार्थ को उस शब्द का वाच्य मानता है। इस प्रकार सातों नय पूर्व-पूर्व नय से उत्तरउत्तर नयों का विषय सूक्ष्म होता चला गया। नैगमनय सामान्य और विशेष, भेद-अभेद दोनों को ग्रहण करता है। जबकि संग्रहनय की दृष्टि उससे संकीर्ण है, वह सामान्य और अभेद को विषय करता है। संग्रहनय से भी व्यवहारनय का विषय कम है। संग्रहनय जहां समस्त पदार्थों को जानता है और व्यवहारनय संग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से ग्रहण करता है। ऋजुसूत्रनय का विषय व्यवहारनय से कम है, चूंकि व्यवहारनय त्रैकालिक विषय की सत्ता को मानता है। जबकि ऋजुसूत्रनय से वर्तमान पदार्थ का ही परिज्ञान होता है। ऋजुसूत्रनय की अपेक्षा शब्दनय का विषय कम है। क्योंकि शब्दनय काल आदि के भेद से वर्तमान पर्याय में भी भेद स्वीकार करता है। शब्दनय वर्तमान पर्याय के वाचक विविध पर्यायवाची शब्दों में से काल. लिंग. संख्या. परुष आदि व्याकरण सम्बन्धी विषमताओं का निराकरण करके केवल समान काल, लिंग आदि शब्दों को एकार्थवाची मानता है। जबकि ऋजुसूत्रनय में काल आदि का भेद नहीं होता। शब्दनय से भी समभिरूढ का विषय कम है। वह पर्याय और व्युत्पत्तिभेद से अर्थभेद मानता है। जबकि शब्दनय पर्यायवाची शब्दों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानता। समभिरूढ़नय इन्द्र, शक्र आदि एकार्थवाची शब्दों को भी व्युत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न अर्थवाची मानता है। वह किसी एक ही शब्द को वाचक रूप में रूढ़ करता है। पर वह सूक्ष्मता शब्दनय में नहीं है। एवंभूतनय का विषय समभिरूढ़नय से भी न्यून है। वह अर्थ को भी उस शब्द का वाच्य तभी मानता है, जब अर्थ अपनी व्युत्पत्ति मूलक्रिया में लगा हो। सारांश यह है, पूर्व-पूर्व नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर विषय वाला होता है; और उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही आधृत है, और प्रत्येक का विषयक्षेत्र उत्तरोत्तर न्यून होने से इनका परस्पर में पौर्वापर्य सम्बन्ध है। नयद्वार के विवेचन के साथ ही चारों प्रकार के अनुयोगद्वार का
७९. कालादिभेदेन ध्वनेरर्थभेदं प्रतिपद्यमानः शब्दः । कालकारकलिंगसंख्यापुरुषोपसर्गाः कालादयः ।
-जैनतर्कभाषा ८०. पर्यायशब्देषु नियुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन् समभिरूढः ।
—जैनतर्कभाषा ८१. येनात्मनाभूतस्तेनैवाध्यवसायतीति एवंभूतः ।
—सर्वार्थसिद्धि १/३३ [२७]