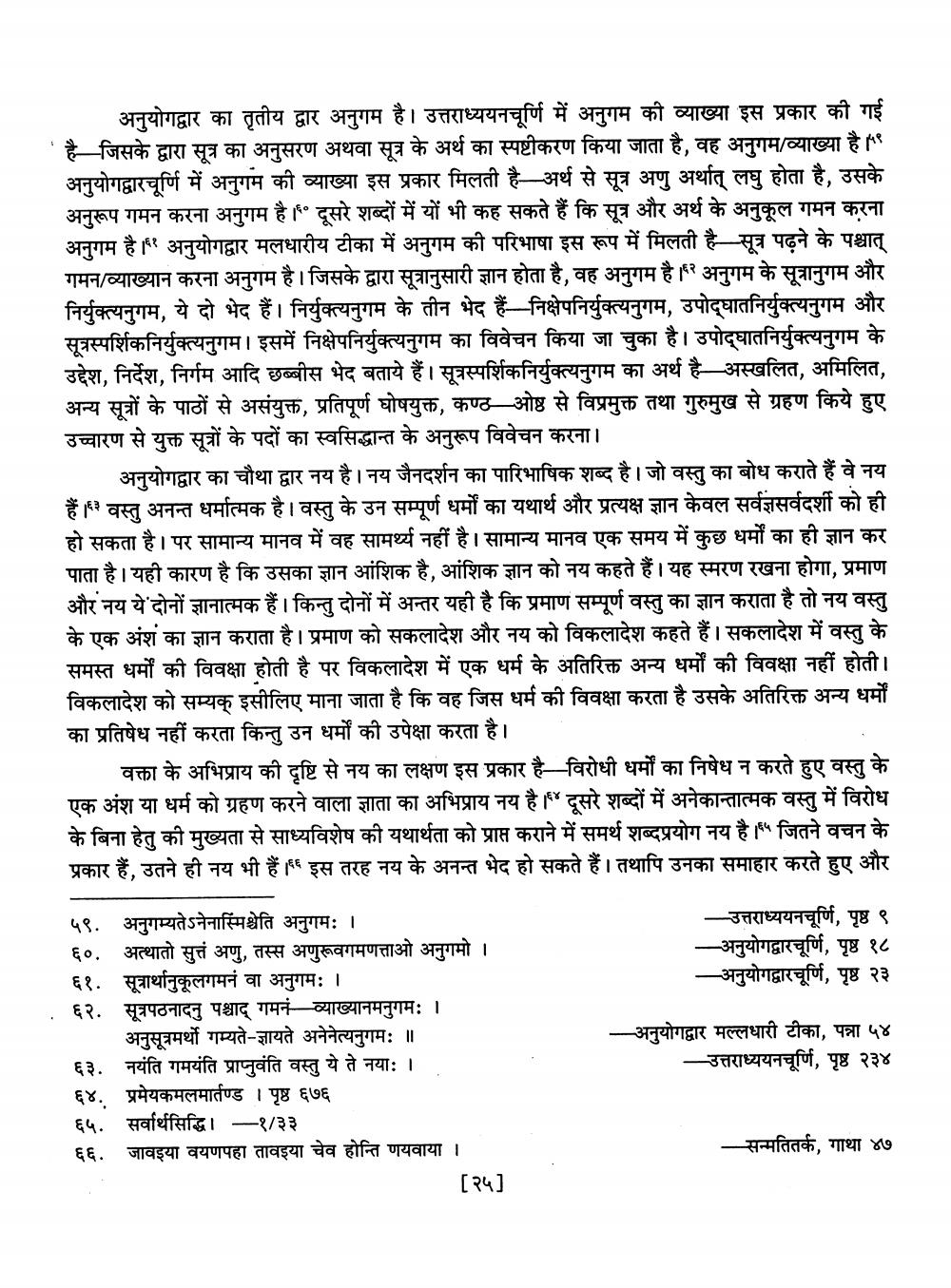________________
अनुयोगद्वार का तृतीय द्वार अनुगम है। उत्तराध्ययनचूर्णि में अनुगम की व्याख्या इस प्रकार की गई है जिसके द्वारा सूत्र का अनुसरण अथवा सूत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण किया जाता है, वह अनुगम/व्याख्या है। अनुयोगद्वारचूर्णि में अनुगम की व्याख्या इस प्रकार मिलती है—अर्थ से सूत्र अणु अर्थात् लघु होता है, उसके अनुरूप गमन करना अनुगम है। दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि सूत्र और अर्थ के अनुकूल गमन करना अनुगम है।६९ अनुयोगद्वार मलधारीय टीका में अनुगम की परिभाषा इस रूप में मिलती है सूत्र पढ़ने के पश्चात् गमन/व्याख्यान करना अनुगम है। जिसके द्वारा सूत्रानुसारी ज्ञान होता है, वह अनुगम है।६२ अनुगम के सूत्रानुगम और निर्युक्त्यनुगम, ये दो भेद हैं। निर्युक्त्यनुगम के तीन भेद हैं—निक्षेपनियुक्त्यनुगम, उपोद्घातनिर्युक्त्यनुगम और सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्त्यनुगम। इसमें निक्षेपनिर्युक्त्यनुगम का विवेचन किया जा चुका है। उपोद्घातनिर्युक्त्यनुगम के उद्देश, निर्देश, निर्गम आदि छब्बीस भेद बताये हैं। सूत्रस्पर्शिकनियुक्त्यनुगम का अर्थ है—अस्खलित, अमिलित, अन्य सूत्रों के पाठों से असंयुक्त, प्रतिपूर्ण घोषयुक्त, कण्ठ ओष्ठ से विप्रमुक्त तथा गुरुमुख से ग्रहण किये हुए उच्चारण से युक्त सूत्रों के पदों का स्वसिद्धान्त के अनुरूप विवेचन करना।
अनुयोगद्वार का चौथा द्वार नय है। नय जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है। जो वस्तु का बोध कराते हैं वे नय हैं।६३ वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। वस्तु के उन सम्पूर्ण धर्मों का यथार्थ और प्रत्यक्ष ज्ञान केवल सर्वज्ञसर्वदर्शी को ही हो सकता है। पर सामान्य मानव में वह सामर्थ्य नहीं है। सामान्य मानव एक समय में कुछ धर्मों का ही ज्ञान कर
है कि उसका ज्ञान आशिक है, आंशिक ज्ञान को नय कहते हैं। यह स्मरण रखना होगा, प्रमाण और नय ये दोनों ज्ञानात्मक हैं। किन्तु दोनों में अन्तर यही है कि प्रमाण सम्पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराता है तो नय वस्तु के एक अंशं का ज्ञान कराता है। प्रमाण को सकलादेश और नय को विकलादेश कहते हैं। सकलादेश में वस्तु के समस्त धर्मों की विवक्षा होती है पर विकलादेश में एक धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की विवक्षा नहीं होती। विकलादेश को सम्यक् इसीलिए माना जाता है कि वह जिस धर्म की विवक्षा करता है उसके अतिरिक्त अन्य धर्मों का प्रतिषेध नहीं करता किन्तु उन धर्मों की उपेक्षा करता है।
वक्ता के अभिप्राय की दृष्टि से नय का लक्षण इस प्रकार है—विरोधी धर्मों का निषेध न करते हुए वस्तु के एक अंश या धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है। दूसरे शब्दों में अनेकान्तात्मक वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुख्यता से साध्यविशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ शब्दप्रयोग नय है।५ जितने वचन के प्रकार हैं, उतने ही नय भी हैं। इस तरह नय के अनन्त भेद हो सकते हैं। तथापि उनका समाहार करते हुए और
-उत्तराध्ययनचूर्णि, पृष्ठ ९ -अनुयोगद्वारचूर्णि, पृष्ठ १८ —अनुयोगद्वारचूर्णि, पृष्ठ २३
५९. अनुगम्यतेऽनेनास्मिश्चेति अनुगमः । ६०. अत्थातो सुत्तं अणु, तस्स अणुरूवगमणत्ताओ अनुगमो । ६१. सूत्रार्थानुकूलगमनं वा अनुगमः ।
सूत्रपठनादनु पश्चाद् गमनं व्याख्यानमनुगमः ।
अनुसूत्रमर्थो गम्यते-ज्ञायते अनेनेत्यनुगमः ॥ ६३. नयंति गमयंति प्राप्नुवंति वस्तु ये ते नयाः । ६४. प्रमेयकमलमार्तण्ड । पृष्ठ ६७६ ६५. सर्वार्थसिद्धि। -१/३३ ६६. जावइया वयणपहा तावइया चेव होन्ति णयवाया ।
[२५]
-अनुयोगद्वार मल्लधारी टीका, पन्ना ५४
-उत्तराध्ययनचूर्णि, पृष्ठ २३४
-सन्मतितर्क, गाथा ४७