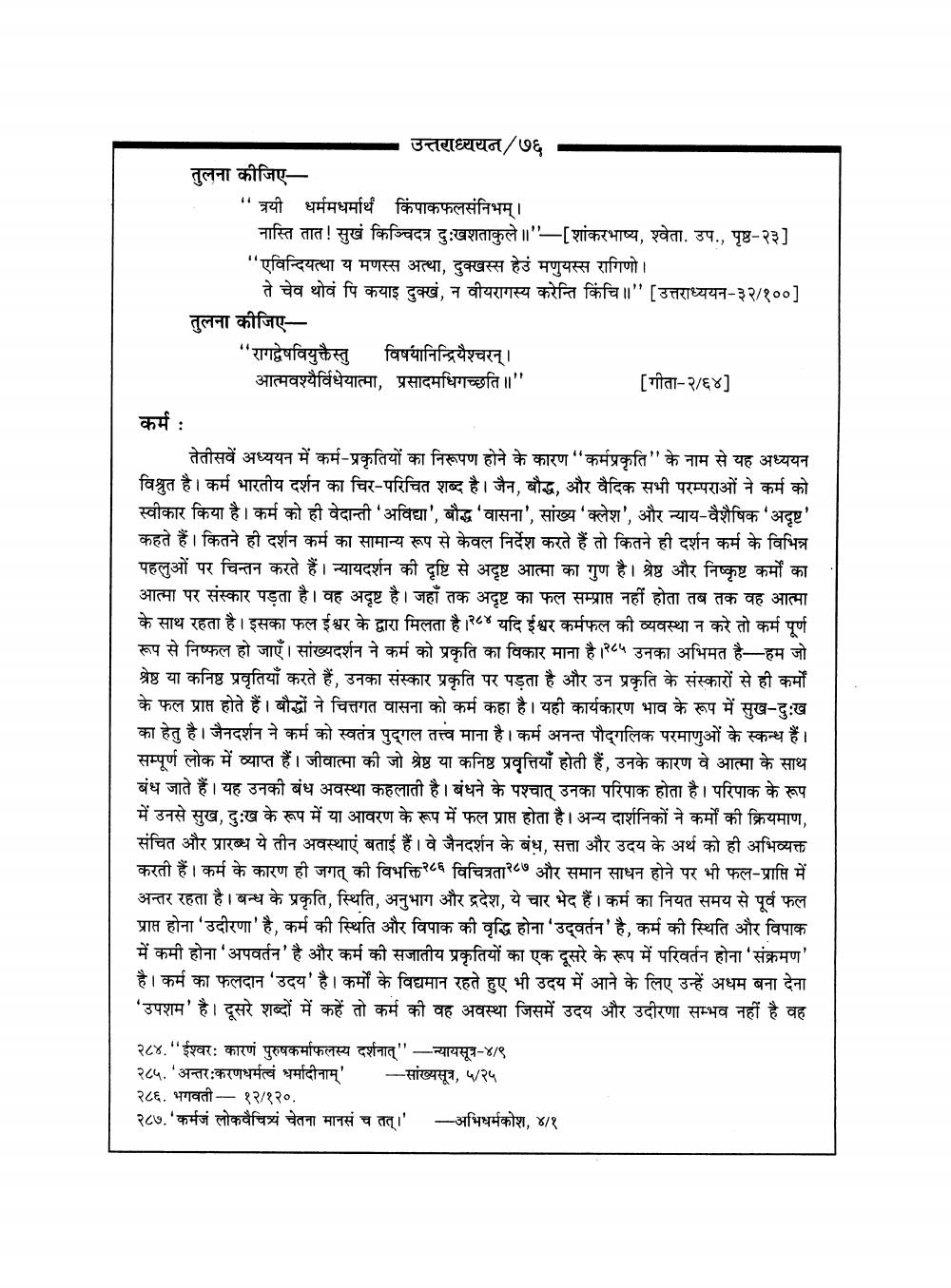________________
उत्तराध्ययन/७६ तुलना कीजिए
"त्रयी धर्ममधर्मार्थं किंपाकफलसंनिभम्।
नास्ति तात! सुखं किञ्चिदत्र दुःखशताकुले ॥"-[शांकरभाष्य, श्वेता. उप., पृष्ठ-२३] "एविन्दियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेडं मणुयस्स रागिणो।
ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं, न वीयरागस्य करेन्ति किंचि॥" [उत्तराध्ययन-३२/१००] तुलना कीजिए
"रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, प्रसादमधिगच्छति ॥"
[गीता-२/६४] कर्म :
तेतीसवें अध्ययन में कर्म-प्रकृतियों का निरूपण होने के कारण "कर्मप्रकृति" के नाम से यह अध्ययन विश्रुत है। कर्म भारतीय दर्शन का चिर-परिचित शब्द है। जैन, बौद्ध, और वैदिक सभी परम्पराओं ने कर्म को स्वीकार किया है। कर्म को ही वेदान्ती 'अविद्या', बौद्ध वासना', सांख्य 'क्लेश', और न्याय-वैशैषिक 'अदृष्ट' कहते हैं। कितने ही दर्शन कर्म का सामान्य रूप से केवल निर्देश करते हैं तो कितने ही दर्शन कर्म के विभिन्न पहलुओं पर चिन्तन करते हैं। न्यायदर्शन की दृष्टि से अदृष्ट आत्मा का गुण है। श्रेष्ठ और निष्कृष्ट कर्मों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है। वह अदृष्ट है। जहाँ तक अदृष्ट का फल सम्प्राप्त नहीं होता तब तक वह आत्मा के साथ रहता है। इसका फल ईश्वर के द्वारा मिलता है।२८४ यदि ईश्वर कर्मफल की व्यवस्था न करे तो कर्म पूर्ण रूप से निष्फल हो जाएँ। सांख्यदर्शन ने कर्म को प्रकृति का विकार माना है।२८५ उनका अभिमत है—हम जो श्रेष्ठ या कनिष्ठ प्रवृतियाँ करते हैं, उनका संस्कार प्रकृति पर पड़ता है और उन प्रकृति के संस्कारों से ही कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। बौद्धों ने चित्तगत वासना को कर्म कहा है। यही कार्यकारण भाव के रूप में सुख-दु:ख का हेतु है। जैनदर्शन ने कर्म को स्वतंत्र पुद्गल तत्त्व माना है। कर्म अनन्त पौद्गलिक परमाणुओं के स्कन्ध हैं। सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं। जीवात्मा की जो श्रेष्ठ या कनिष्ठ प्रवृत्तियाँ होती हैं, उनके कारण वे आत्मा के साथ बंध जाते हैं। यह उनकी बंध अवस्था कहलाती है। बंधने के पश्चात् उनका परिपाक होता है। परिपाक के रूप में उनसे सुख, दु:ख के रूप में या आवरण के रूप में फल प्राप्त होता है। अन्य दार्शनिकों ने कर्मों की क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध ये तीन अवस्थाएं बताई हैं। वे जैनदर्शन के बंध, सत्ता और उदय के अर्थ को ही अभिव्यक्त करती हैं। कर्म के कारण ही जगत् की विभक्ति२८६ विचित्रता२८७ और समान साधन होने पर भी फल-प्राप्ति में अन्तर रहता है। बन्ध के प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और द्रदेश, ये चार भेद हैं। कर्म का नियत समय से पूर्व फल प्राप्त होना 'उदीरणा' है, कर्म की स्थिति और विपाक की वृद्धि होना 'उद्वर्तन' है, कर्म की स्थिति और विपाक में कमी होना 'अपवर्तन' है और कर्म की सजातीय प्रकृतियों का एक दूसरे के रूप में परिवर्तन होना 'संक्रमण' है। कर्म का फलदान 'उदय' है। कर्मों के विद्यमान रहते हुए भी उदय में आने के लिए उन्हें अधम बना देना 'उपशम' है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर्म की वह अवस्था जिसमें उदय और उदीरणा सम्भव नहीं है वह २८४. "ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफलस्य दर्शनात्" -न्यायसूत्र-४/९ २८५. 'अन्तर:करणधर्मत्वं धर्मादीनाम्' -सांख्यसूत्र, ५/२५ २८६. भगवती- १२/१२०. २८७. 'कर्मजं लोकवैचित्र्यं चेतना मानसं च तत्।' -अभिधर्मकोश, ४/१