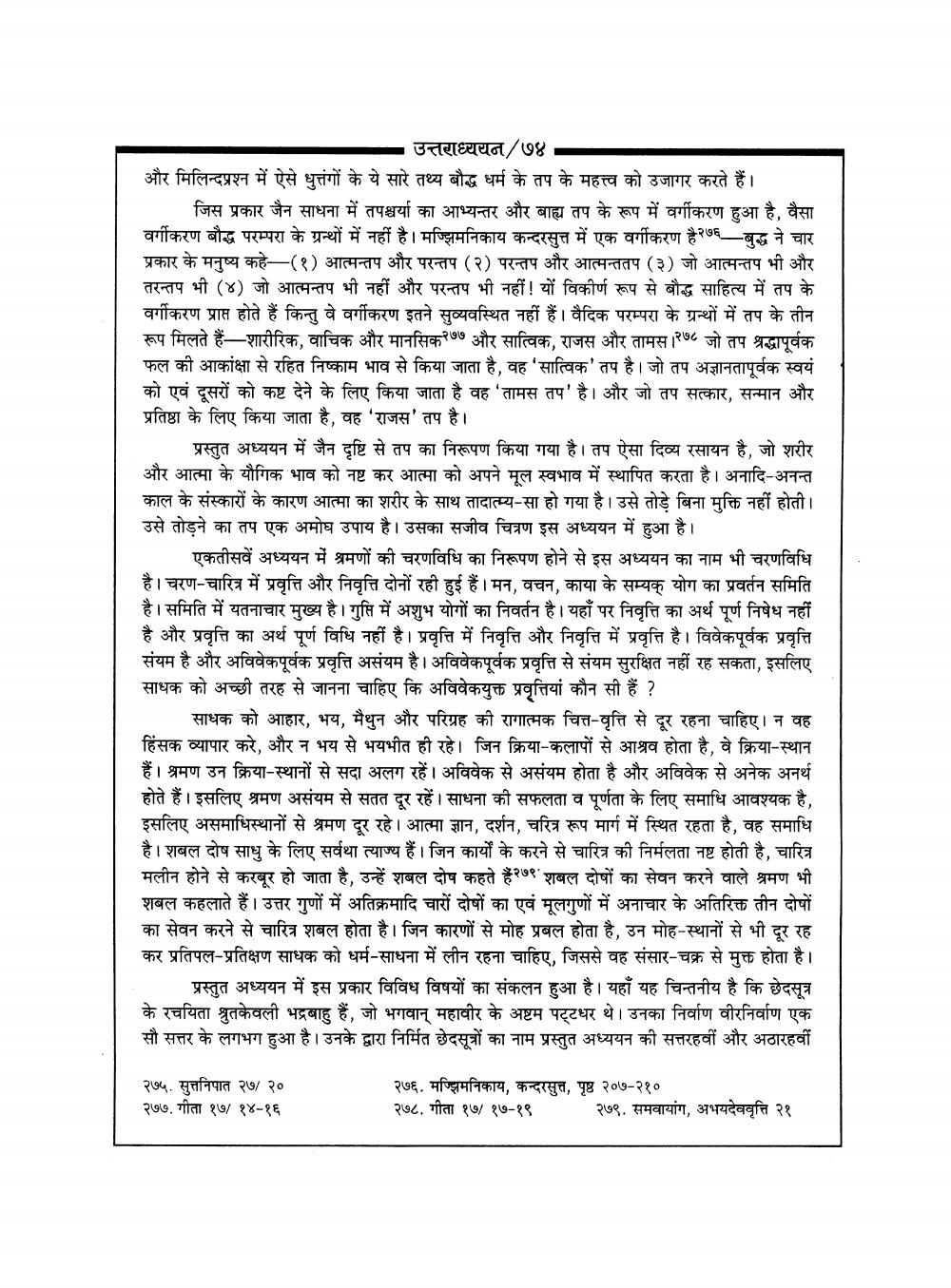________________
उत्तराध्ययन/७४ और मिलिन्दप्रश्न में ऐसे धुत्तंगों के ये सारे तथ्य बौद्ध धर्म के तप के महत्त्व को उजागर करते हैं।
जिस प्रकार जैन साधना में तपश्चर्या का आभ्यन्तर और बाह्य तप के रूप में वर्गीकरण हुआ है, वैसा वर्गीकरण बौद्ध परम्परा के ग्रन्थों में नहीं है। मज्झिमनिकाय कन्दरसुत्त में एक वर्गीकरण है२७६–बुद्ध ने चार प्रकार के मनुष्य कहे-(१) आत्मन्तप और परन्तप (२) परन्तप और आत्मन्ततप (३) जो आत्मन्तप भी और तरन्तप भी (४) जो आत्मन्तप भी नहीं और परन्तप भी नहीं! यों विकीर्ण रूप से बौद्ध साहित्य में तप के वर्गीकरण प्राप्त होते हैं किन्तु वे वर्गीकरण इतने सुव्यवस्थित नहीं हैं। वैदिक परम्परा के ग्रन्थों में तप के तीन रूप मिलते हैं—शारीरिक, वाचिक और मानसिक२७७ और सात्विक, राजस और तामस।२७८ जो तप श्रद्धापूर्वक फल की आकांक्षा से रहित निष्काम भाव से किया जाता है, वह 'सात्विक' तप है। जो तप अज्ञानतापूर्वक स्वयं को एवं दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है वह 'तामस तप' है। और जो तप सत्कार, सन्मान और प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, वह 'राजस' तप है।
प्रस्तुत अध्ययन में जैन दृष्टि से तप का निरूपण किया गया है। तप ऐसा दिव्य रसायन है, जो शरीर और आत्मा के यौगिक भाव को नष्ट कर आत्मा को अपने मूल स्वभाव में स्थापित करता है। अनादि-अनन्त काल के संस्कारों के कारण आत्मा का शरीर के साथ तादात्म्य-सा हो गया है। उसे तोड़े बिना मुक्ति नहीं होती। उसे तोड़ने का तप एक अमोघ उपाय है। उसका सजीव चित्रण इस अध्ययन में हुआ है।
एकतीसवें अध्ययन में श्रमणों की चरणविधि का निरूपण होने से इस अध्ययन का नाम भी चरणविधि है। चरण-चारित्र में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों रही हुई हैं। मन, वचन, काया के सम्यक् योग का प्रवर्तन समिति है। समिति में यतनाचार मुख्य है। गुप्ति में अशुभ योगों का निवर्तन है। यहाँ पर निवृत्ति का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है और प्रवृत्ति का अर्थ पूर्ण विधि नहीं है। प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति है। विवेकपूर्वक प्रवृत्ति संयम है और अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति असंयम है। अविवेकपूर्वक प्रवृत्ति से संयम सुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए साधक को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि अविवेकयुक्त प्रवृत्तियां कौन सी हैं ?
साधक को आहार, भय, मैथुन और परिग्रह की रागात्मक चित्त-वृत्ति से दूर रहना चाहिए। न वह हिंसक व्यापार करे, और न भय से भयभीत ही रहे। जिन क्रिया-कलापों से आश्रव होता है, वे क्रिया-स्थान हैं। श्रमण उन क्रिया-स्थानों से सदा अलग रहें। अविवेक से असंयम होता है और अविवेक से अनेक अनर्थ होते हैं। इसलिए श्रमण असंयम से सतत दूर रहें। साधना की सफलता व पूर्णता के लिए समाधि आवश्यक है, इसलिए असमाधिस्थानों से श्रमण दूर रहे। आत्मा ज्ञान, दर्शन, चरित्र रूप मार्ग में स्थित रहता है, वह समाधि है। शबल दोष साध के लिए सर्वथा त्याज्य हैं। जिन कार्यों के करने से चारित्र की निर्मलता नष्ट होती है, चारित्र मलीन होने से करबूर हो जाता है, उन्हें शबल दोष कहते हैं२७९ शबल दोषों का सेवन करने वाले श्रमण भी शबल कहलाते हैं। उत्तर गुणों में अतिक्रमादि चारों दोषों का एवं मूलगुणों में अनाचार के अतिरिक्त तीन दोषों का सेवन करने से चारित्र शबल होता है। जिन कारणों से मोह प्रबल होता है, उन मोह-स्थानों से भी दूर रह कर प्रतिपल-प्रतिक्षण साधक को धर्म-साधना में लीन रहना चाहिए, जिससे वह संसार-चक्र से मुक्त होता है।
__ प्रस्तुत अध्ययन में इस प्रकार विविध विषयों का संकलन हुआ है। यहाँ यह चिन्तनीय है कि छेदसूत्र के रचयिता श्रुतकेवली भद्रबाहु हैं, जो भगवान् महावीर के अष्टम पट्टधर थे। उनका निर्वाण वीरनिर्वाण एक सौ सत्तर के लगभग हुआ है। उनके द्वारा निर्मित छेदसूत्रों का नाम प्रस्तुत अध्ययन की सत्तरहवीं और अठारहवीं
२७५. सुत्तनिपात २७/ २० २७७. गीता १७/ १४-१६
२७६. मज्झिमनिकाय, कन्दरसुत्त, पृष्ठ २०७-२१० २७८, गीता १७/ १७-१९ २ ७९. समवायांग, अभयदेववृत्ति २१