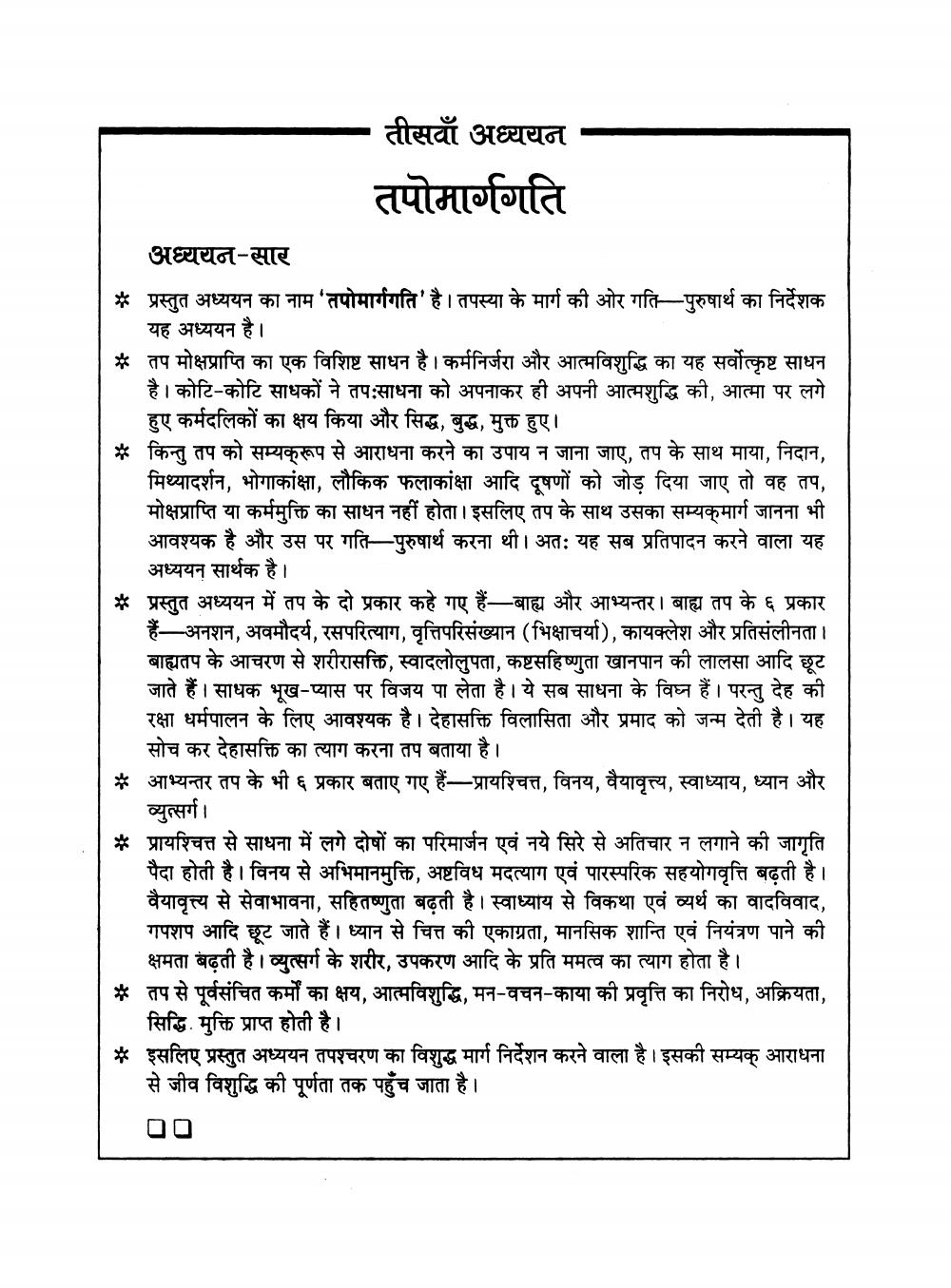________________
तीसवाँ अध्ययन तपोमार्गगति
अध्ययन-सार * प्रस्तुत अध्ययन का नाम 'तपोमार्गगति' है। तपस्या के मार्ग की ओर गति—पुरुषार्थ का निर्देशक
यह अध्ययन है। * तप मोक्षप्राप्ति का एक विशिष्ट साधन है। कर्मनिर्जरा और आत्मविशुद्धि का यह सर्वोत्कृष्ट साधन
है। कोटि-कोटि साधकों ने तप:साधना को अपनाकर ही अपनी आत्मशुद्धि की, आत्मा पर लगे
हुए कर्मदलिकों का क्षय किया और सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हुए। * किन्तु तप को सम्यक्रूप से आराधना करने का उपाय न जाना जाए, तप के साथ माया, निदान,
मिथ्यादर्शन, भोगाकांक्षा, लौकिक फलाकांक्षा आदि दूषणों को जोड़ दिया जाए तो वह तप, मोक्षप्राप्ति या कर्ममुक्ति का साधन नहीं होता। इसलिए तप के साथ उसका सम्यक्मार्ग जानना भी आवश्यक है और उस पर गति-पुरुषार्थ करना थी। अतः यह सब प्रतिपादन करने वाला यह
अध्ययन सार्थक है। * प्रस्तुत अध्ययन में तप के दो प्रकार कहे गए हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। बाह्य तप के ६ प्रकार
हैं—अनशन, अवमौदर्य, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान (भिक्षाचर्या), कायक्लेश और प्रतिसंलीनता। बाह्यतप के आचरण से शरीरासक्ति, स्वादलोलुपता, कष्टसहिष्णुता खानपान की लालसा आदि छूट जाते हैं। साधक भूख-प्यास पर विजय पा लेता है। ये सब साधना के विघ्न हैं। परन्तु देह की रक्षा धर्मपालन के लिए आवश्यक है। देहासक्ति विलासिता और प्रमाद को जन्म देती है। यह
सोच कर देहासक्ति का त्याग करना तप बताया है। * आभ्यन्तर तप के भी ६ प्रकार बताए गए हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, ध्यान और
व्युत्सर्ग। * प्रायश्चित्त से साधना में लगे दोषों का परिमार्जन एवं नये सिरे से अतिचार न लगाने की जागृति
पैदा होती है। विनय से अभिमानमुक्ति, अष्टविध मदत्याग एवं पारस्परिक सहयोगवृत्ति बढ़ती है। वैयावृत्त्य से सेवाभावना, सहितष्णुता बढ़ती है। स्वाध्याय से विकथा एवं व्यर्थ का वादविवाद, गपशप आदि छूट जाते हैं। ध्यान से चित्त की एकाग्रता, मानसिक शान्ति एवं नियंत्रण पाने की
क्षमता बढ़ती है। व्युत्सर्ग के शरीर, उपकरण आदि के प्रति ममत्व का त्याग होता है। * तप से पूर्वसंचित कर्मों का क्षय, आत्मविशुद्धि, मन-वचन-काया की प्रवृत्ति का निरोध, अक्रियता,
सिद्धि. मुक्ति प्राप्त होती है। * इसलिए प्रस्तुत अध्ययन तपश्चरण का विशुद्ध मार्ग निर्देशन करने वाला है। इसकी सम्यक् आराधना
से जीव विशुद्धि की पूर्णता तक पहुँच जाता है। 00