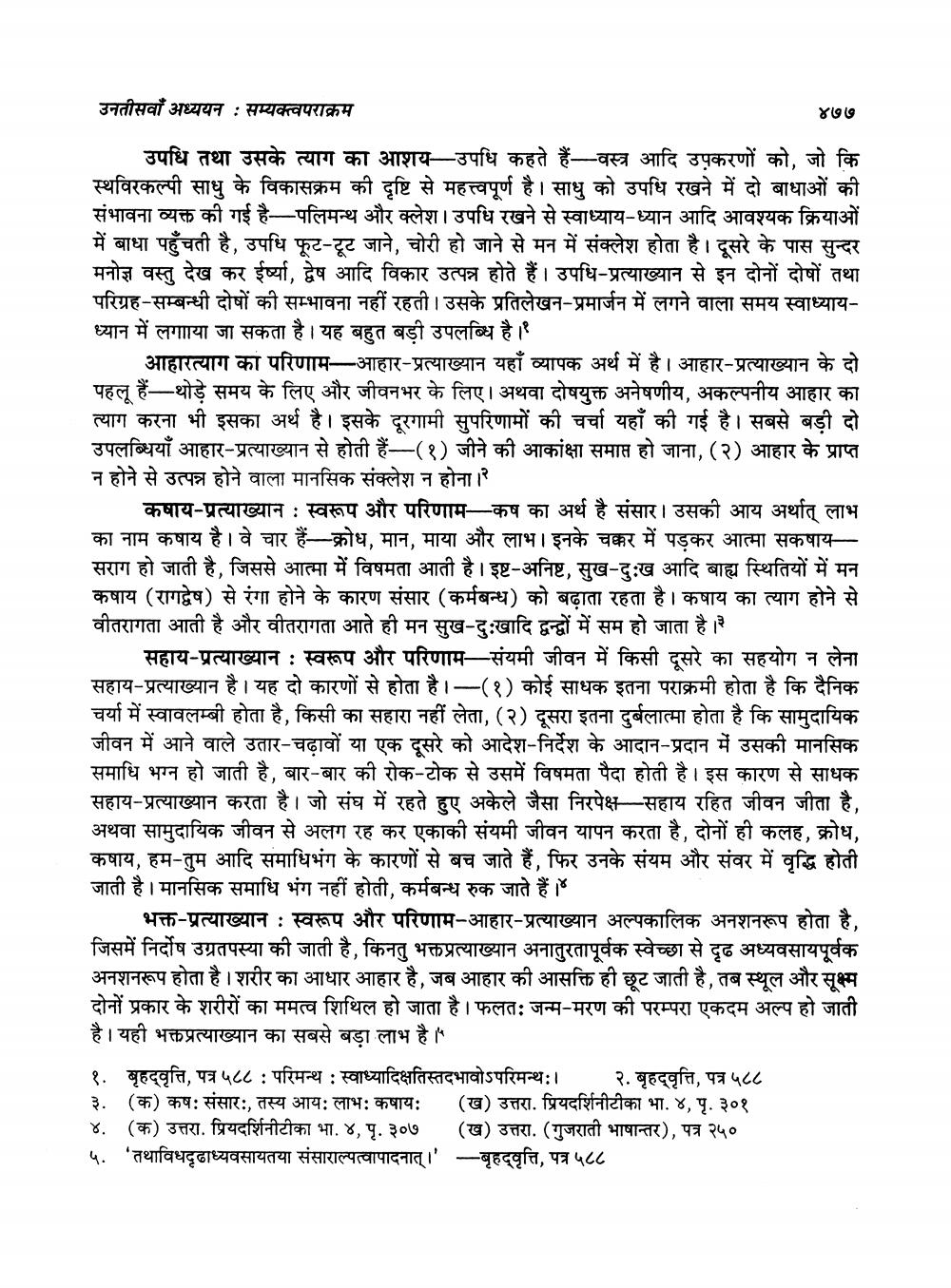________________
उनतीसवाँ अध्ययन : सम्यक्त्वपराक्रम
४७७
उपधि तथा उसके त्याग का आशय-उपधि कहते हैं-वस्त्र आदि उपकरणों को, जो कि स्थविरकल्पी साधु के विकासक्रम की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। साधु को उपधि रखने में दो बाधाओं की संभावना व्यक्त की गई है—पलिमन्थ और क्लेश। उपधि रखने से स्वाध्याय-ध्यान आदि आवश्यक क्रियाओं में बाधा पहुँचती है, उपधि फूट-टूट जाने, चोरी हो जाने से मन में संक्लेश होता है। दूसरे के पास सुन्दर मनोज्ञ वस्तु देख कर ईर्ष्या, द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं। उपधि-प्रत्याख्यान से इन दोनों दोषों तथा परिग्रह-सम्बन्धी दोषों की सम्भावना नहीं रहती। उसके प्रतिलेखन-प्रमार्जन में लगने वाला समय स्वाध्यायध्यान में लगाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
आहारत्याग का परिणाम-आहार-प्रत्याख्यान यहाँ व्यापक अर्थ में है। आहार-प्रत्याख्यान के दो पहलू हैं-थोड़े समय के लिए और जीवनभर के लिए। अथवा दोषयुक्त अनेषणीय, अकल्पनीय आहार का त्याग करना भी इसका अर्थ है। इसके दूरगामी सुपरिणामों की चर्चा यहाँ की गई है। सबसे बड़ी दो उपलब्धियाँ आहार-प्रत्याख्यान से होती हैं—(१) जीने की आकांक्षा समाप्त हो जाना, (२) आहार के प्राप्त न होने से उत्पन्न होने वाला मानसिक संक्लेशन होना।२
कषाय-प्रत्याख्यान : स्वरूप और परिणाम–कष का अर्थ है संसार। उसकी आय अर्थात् लाभ का नाम कषाय है। वे चार हैं-क्रोध, मान, माया और लाभ। इनके चक्कर में पडकर आत्मा सकषायसराग हो जाती है. जिससे आत्मा में विषमता आती है। इष्ट-अनिष्ट सख-द:ख आदि बाह्य स्थितियों में मन कषाय (रागद्वेष) से रंगा होने के कारण संसार (कर्मबन्ध) को बढ़ाता रहता है। कषाय का त्याग होने से वीतरागता आती है और वीतरागता आते ही मन सुख-दुःखादि द्वन्द्वों में सम हो जाता है।
सहाय-प्रत्याख्यान : स्वरूप और परिणाम–संयमी जीवन में किसी दूसरे का सहयोग न लेना सहाय-प्रत्याख्यान है। यह दो कारणों से होता है। -(१) कोई साधक इतना पराक्रमी होता है कि दैनिक चर्या में स्वावलम्बी होता है, किसी का सहारा नहीं लेता, (२) दूसरा इतना दुर्बलात्मा होता है कि सामुदायिक जीवन में आने वाले उतार-चढ़ावों या एक दूसरे को आदेश-निर्देश के आदान-प्रदान में उसकी मानसिक समाधि भग्न हो जाती है, बार-बार की रोक-टोक से उसमें विषमता पैदा होती है। इस कारण से साधक सहाय-प्रत्याख्यान करता है। जो संघ में रहते हुए अकेले जैसा निरपेक्ष-सहाय रहित जीवन जीता है, अथवा सामुदायिक जीवन से अलग रह कर एकाकी संयमी जीवन यापन करता है, दोनों ही कलह, क्रोध, कषाय, हम-तुम आदि समाधिभंग के कारणों से बच जाते हैं, फिर उनके संयम और संवर में वृद्धि होती जाती है। मानसिक समाधि भंग नहीं होती, कर्मबन्ध रुक जाते हैं।
भक्त-प्रत्याख्यान : स्वरूप और परिणाम-आहार-प्रत्याख्यान अल्पकालिक अनशनरूप होता है, जिसमें निर्दोष उग्रतपस्या की जाती है, किनतु भक्तप्रत्याख्यान अनातुरतापूर्वक स्वेच्छा से दृढ अध्यवसायपूर्वक अनशनरूप होता है। शरीर का आधार आहार है, जब आहार की आसक्ति ही छूट जाती है, तब स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों का ममत्व शिथिल हो जाता है । फलतः जन्म-मरण की परम्परा एकदम अल्प हो जाती है। यही भक्तप्रत्याख्यान का सबसे बड़ा लाभ है।
१. बृहद्वत्ति, पत्र ५८८ : परिमन्थ : स्वाध्यादिक्षतिस्तदभावोऽपरिमन्थः। २. बृहद्वत्ति, पत्र ५८८ ३. (क) कष: संसारः, तस्य आयः लाभ: कषायः (ख) उत्तरा. प्रियदर्शिनीटीका भा. ४, पृ. ३०१ ४. (क) उत्तरा. प्रियदर्शिनीटीका भा. ४, पृ. ३०७ (ख) उत्तरा. (गुजराती भाषान्तर), पत्र २५० ५. 'तथाविधदृढाध्यवसायतया संसाराल्पत्वापादनात्।' -बृहद्वृत्ति, पत्र ५८८