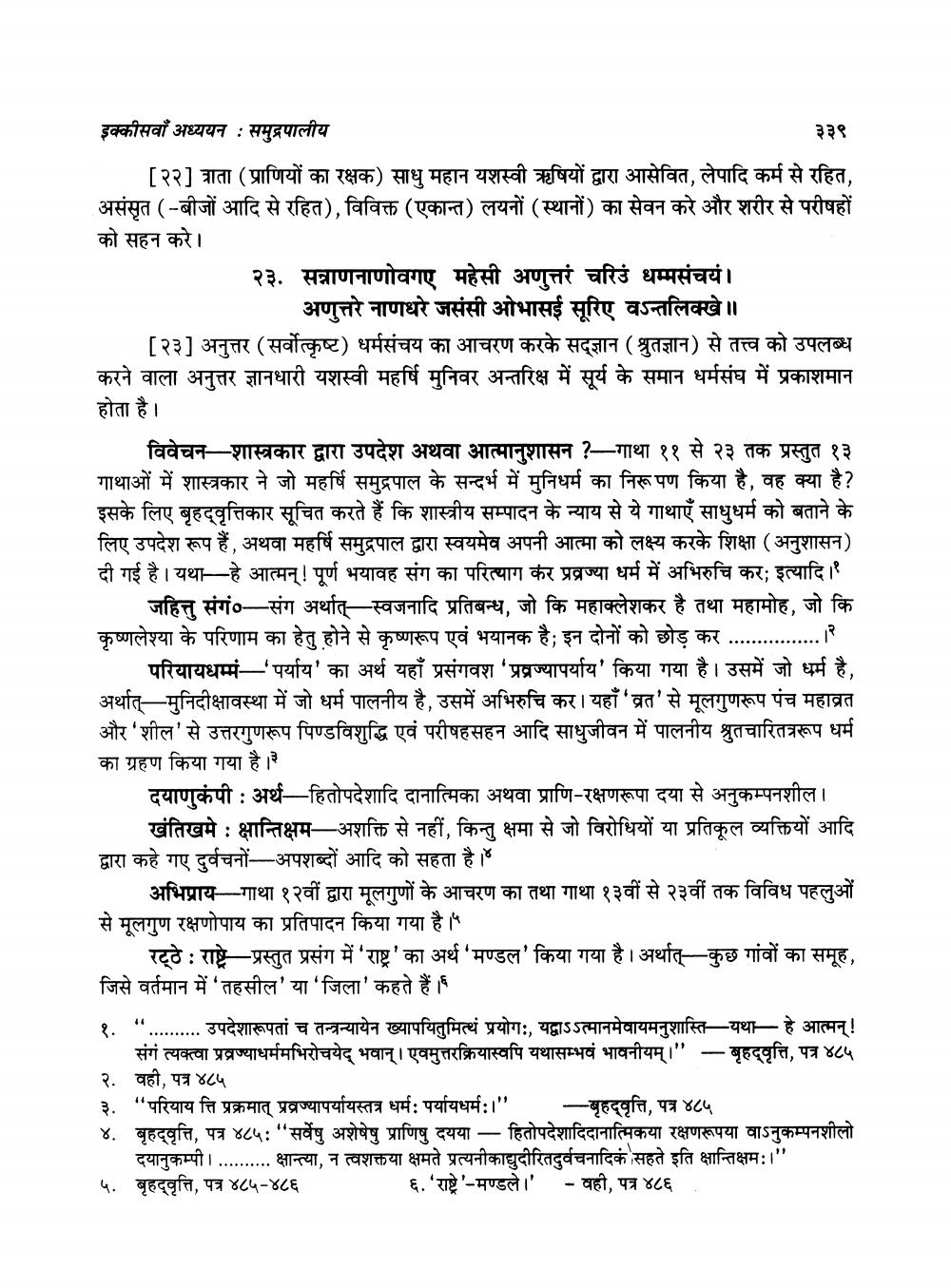________________
इक्कीसवाँ अध्ययन : समुद्रपालीय
[२२] त्राता (प्राणियों का रक्षक) साधु महान यशस्वी ऋषियों द्वारा आसेवित, लेपादि कर्म से रहित, असंसृत (-बीजों आदि से रहित), विविक्त (एकान्त) लयनों (स्थानों) का सेवन करे और शरीर से परीषहों को सहन करे।
२३. सन्नाणनाणोवगए महेसी अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचयं।
___ अणुत्तरे नाणधरे जसंसी ओभासई सूरिए वऽन्तलिक्खे॥ [२३] अनुत्तर (सर्वोत्कृष्ट) धर्मसंचय का आचरण करके सद्ज्ञान (श्रुतज्ञान) से तत्त्व को उपलब्ध करने वाला अनुत्तर ज्ञानधारी यशस्वी महर्षि मुनिवर अन्तरिक्ष में सूर्य के समान धर्मसंघ में प्रकाशमान होता है।
विवेचन–शास्त्रकार द्वारा उपदेश अथवा आत्मानुशासन ?-गाथा ११ से २३ तक प्रस्तुत १३ गाथाओं में शास्त्रकार ने जो महर्षि समुद्रपाल के सन्दर्भ में मुनिधर्म का निरूपण किया है, वह क्या है? इसके लिए बृहद्वृत्तिकार सूचित करते हैं कि शास्त्रीय सम्पादन के न्याय से ये गाथाएँ साधुधर्म को बताने के लिए उपदेश रूप हैं, अथवा महर्षि समुद्रपाल द्वारा स्वयमेव अपनी आत्मा को लक्ष्य करके शिक्षा (अनुशासन) दी गई है। यथा-हे आत्मन् ! पूर्ण भयावह संग का परित्याग कर प्रव्रज्या धर्म में अभिरुचि कर; इत्यादि।
जहित्तु संगं०–संग अर्थात् स्वजनादि प्रतिबन्ध, जो कि महाक्लेशकर है तथा महामोह, जो कि कृष्णलेश्या के परिणाम का हेतु होने से कृष्णरूप एवं भयानक है; इन दोनों को छोड़ कर ...............२
परियायधम्मं—'पर्याय' का अर्थ यहाँ प्रसंगवश 'प्रव्रज्यापर्याय' किया गया है। उसमें जो धर्म है, अर्थात्-मुनिदीक्षावस्था में जो धर्म पालनीय है, उसमें अभिरुचि कर । यहाँ 'व्रत' से मूलगुणरूप पंच महाव्रत
और 'शील' से उत्तरगुणरूप पिण्डविशुद्धि एवं परीषहसहन आदि साधुजीवन में पालनीय श्रुतचारितत्ररूप धर्म का ग्रहण किया गया है।
दयाणुकंपी : अर्थ—हितोपदेशादि दानात्मिका अथवा प्राणि-रक्षणरूपा दया से अनुकम्पनशील ।
खंतिखमे : क्षान्तिक्षम-अशक्ति से नहीं, किन्तु क्षमा से जो विरोधियों या प्रतिकूल व्यक्तियों आदि द्वारा कहे गए दुर्वचनों-अपशब्दों आदि को सहता है।
अभिप्राय—गाथा १२वीं द्वारा मूलगुणों के आचरण का तथा गाथा १३वीं से २३वीं तक विविध पहलुओं से मूलगुण रक्षणोपाय का प्रतिपादन किया गया है।
रट्टे : राष्ट्र प्रस्तुत प्रसंग में 'राष्ट्र' का अर्थ 'मण्डल' किया गया है। अर्थात् —कुछ गांवों का समूह, जिसे वर्तमान में 'तहसील' या 'जिला' कहते हैं। १. "......... उपदेशारूपतां च तन्त्रन्यायेन ख्यापयितुमित्थं प्रयोगः, यद्वाऽऽत्मानमेवायमनुशास्ति—यथा— हे आत्मन् !
संगं त्यक्त्वा प्रव्रज्याधर्ममभिरोचयेद् भवान् । एवमुत्तरक्रियास्वपि यथासम्भवं भावनीयम्।" -बृहवृत्ति, पत्र ४८५ २. वही, पत्र ४८५ ३. "परियाय त्ति प्रक्रमात् प्रव्रज्यापर्यायस्तत्र धर्म: पर्यायधर्मः।" -बृहवृत्ति, पत्र ४८५ ४. बहदवत्ति. पत्र ४८५: "सर्वेष अशेषेष प्राणिष दयया - हितोपदेशादिदानात्मिकया रक्षणरूपया वाऽनकम्पनशीलो
दयानुकम्पी। .......... क्षान्त्या, न त्वशक्तया क्षमते प्रत्यनीकाधुदीरितदुर्वचनादिकं सहते इति क्षान्तिक्षमः।" ५. बृहद्वृत्ति, पत्र ४८५-४८६
६. 'राष्ट्र'-मण्डले।' - वही, पत्र ४८६ .