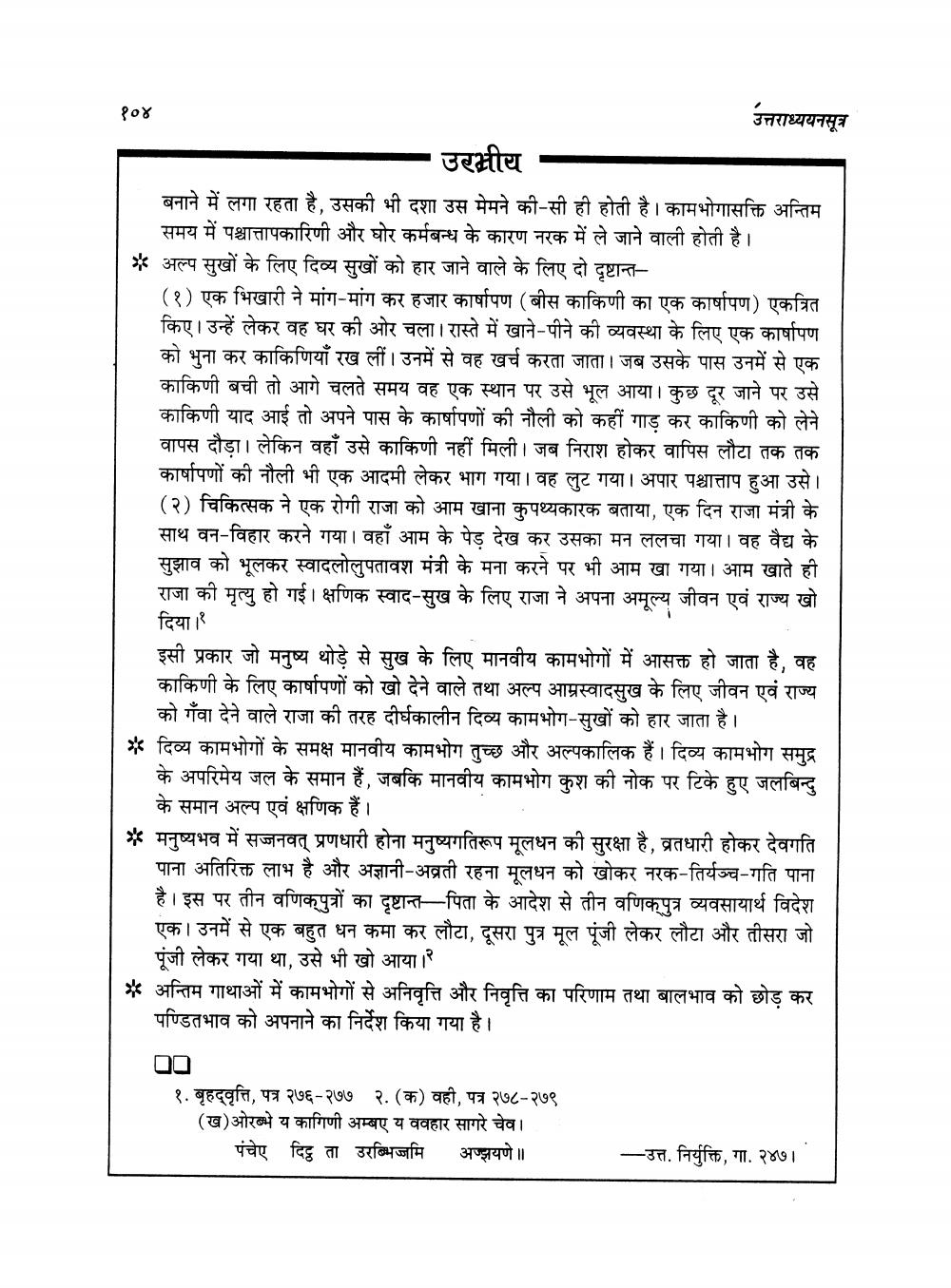________________
१०४
उत्तराध्
उरभीय
बनाने में लगा रहता है, उसकी भी दशा उस मेमने की-सी ही होती है। कामभोगासक्ति अन्तिम समय में पश्चात्तापकारिणी और घोर कर्मबन्ध के कारण नरक में ले जाने वाली होती है। * अल्प सुखों के लिए दिव्य सुखों को हार जाने वाले के लिए दो दृष्टान्त
(१) एक भिखारी ने मांग-मांग कर हजार कार्षापण (बीस काकिणी का एक कार्षापण) एकत्रित किए। उन्हें लेकर वह घर की ओर चला। रास्ते में खाने-पीने की व्यवस्था के लिए एक कार्षापण को भुना कर काकिणियाँ रख लीं। उनमें से वह खर्च करता जाता। जब उसके पास उनमें से एक काकिणी बची तो आगे चलते समय वह एक स्थान पर उसे भूल आया। कुछ दूर जाने पर उसे काकिणी याद आई तो अपने पास के कार्षापणों की नौली को कहीं गाड़ कर काकिणी को लेने वापस दौड़ा। लेकिन वहाँ उसे काकिणी नहीं मिली। जब निराश होकर वापिस लौटा तक तक कार्षापणों की नौली भी एक आदमी लेकर भाग गया। वह लुट गया। अपार पश्चात्ताप हुआ उसे (२) चिकित्सक ने एक रोगी राजा को आम खाना कुपथ्यकारक बताया, एक दिन राजा मंत्री के साथ वन विहार करने गया। वहाँ आम के पेड़ देख कर उसका मन ललचा गया। वह वैद्य के सुझाव को भूलकर स्वादलोलुपतावश मंत्री के मना करने पर भी आम खा गया। आम खाते ही राजा की मृत्यु हो गई। क्षणिक स्वाद-सुख के लिए राजा ने अपना अमूल्य जीवन एवं राज्य खो दिया । १
इसी प्रकार जो मनुष्य थोड़े से सुख के लिए मानवीय कामभोगों में आसक्त हो जाता है, वह काकिणी के लिए कार्षापणों को खो देने वाले तथा अल्प आम्रस्वादसुख के लिए जीवन एवं राज्य को गँवा देने वाले राजा की तरह दीर्घकालीन दिव्य कामभोग-सुखों को हार जाता 1
* दिव्य कामभोगों के समक्ष मानवीय कामभोग तुच्छ और अल्पकालिक हैं। दिव्य कामभोग समुद्र के अपरिमेय जल के समान हैं, जबकि मानवीय कामभोग कुश की नोक पर टिके हुए जलबिन्दु के समान अल्प एवं क्षणिक हैं ।
* मनुष्यभव में सज्जनवत् प्रणधारी होना मनुष्यगतिरूप मूलधन की सुरक्षा है, व्रतधारी होकर देवगति पाना अतिरिक्त लाभ है और अज्ञानी - अव्रती रहना मूलधन को खोकर नरक - तिर्यञ्च-गति पाना है। इस पर तीन वणिक्पुत्रों का दृष्टान्त —-पिता के आदेश से तीन वणिक्पुत्र व्यवसायार्थ विदेश एक। उनमें से एक बहुत धन कमा कर लौटा, दूसरा पुत्र मूल पूंजी लेकर लौटा और तीसरा जो पूंजी लेकर गया था, उसे भी खो आया । २
* अन्तिम गाथाओं में कामभोगों से अनिवृत्ति और निवृत्ति का परिणाम तथा बालभाव को छोड़ कर पण्डितभाव को अपनाने का निर्देश किया गया है।
1
१. बृहद्वृत्ति, पत्र २७६ - २७७ २. (क) वही, पत्र २७८ - २७९
(ख) ओरब्भे य कागिणी अम्बए य ववहार सागरे चेव । पंचेए दिट्ठ ता उरब्भिज्जमि
अज्झयणे ॥
- उत्त. नियुक्ति, गा. २४७ ।