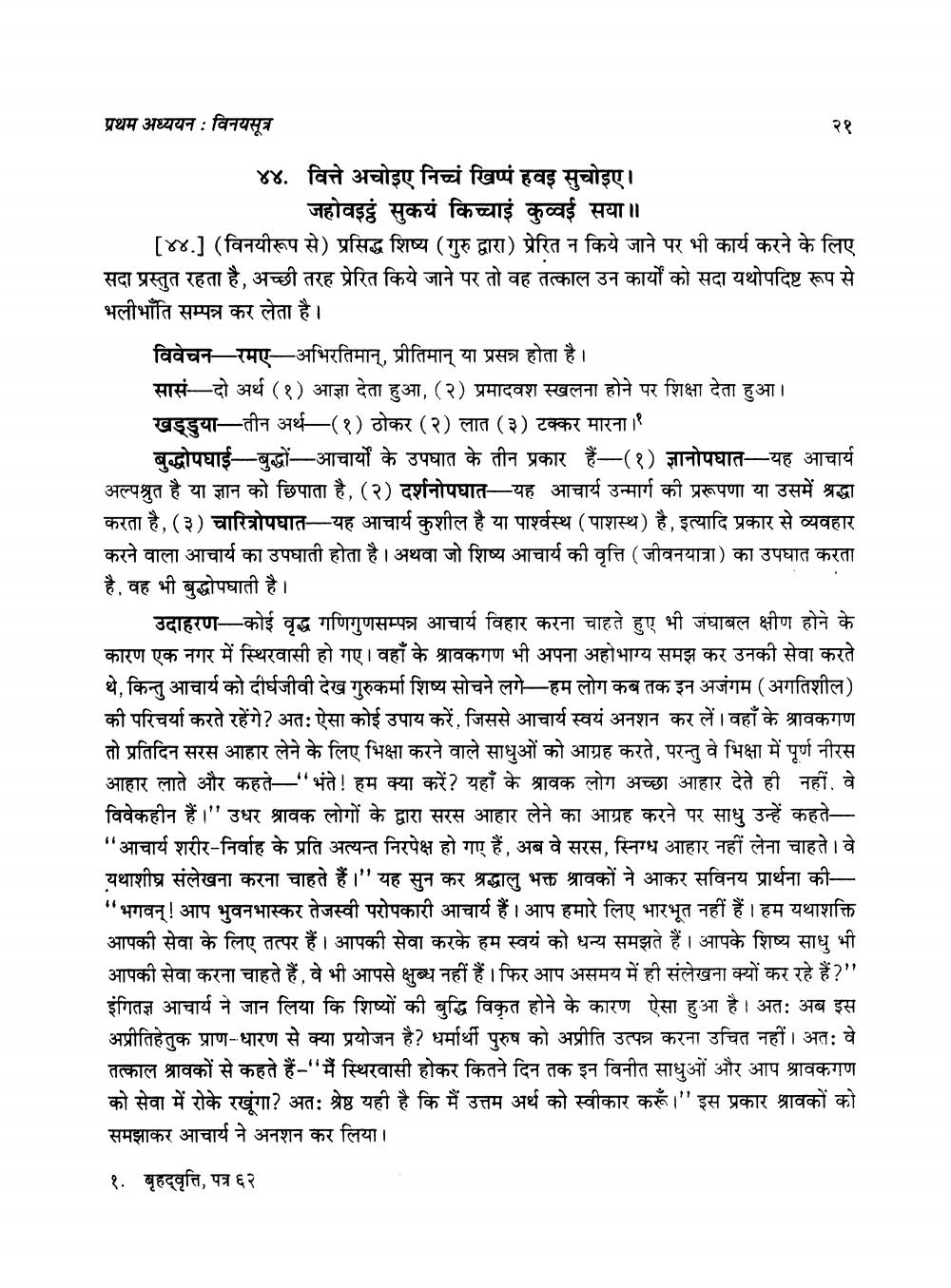________________
प्रथम अध्ययन : विनयसूत्र
४४. वित्ते अचोइए निच्चं खिप्पं हवइ सुचोइए । जहोवइट्ठ सुकयं किच्चाई कुव्वई सया ॥
२१
[४४.] (विनयीरूप से) प्रसिद्ध शिष्य (गुरु द्वारा ) प्रेरित न किये जाने पर भी कार्य करने के लिए सदा प्रस्तुत रहता है, अच्छी तरह प्रेरित किये जाने पर तो वह तत्काल उन कार्यों को सदा यथोपदिष्ट रूप से भलीभाँति सम्पन्न कर लेता है ।
विवेचन— रमए— अभिरतिमान्, प्रीतिमान् या प्रसन्न होता है ।
सासं—दो अर्थ (१) आज्ञा देता हुआ, (२) प्रमादवश स्खलना होने पर शिक्षा देता हुआ ।
खड्डुया - तीन अर्थ — (१) ठोकर (२) लात (३) टक्कर मारना । १
बुद्धोपघाई— बुद्धों— आचार्यों के उपघात के तीन प्रकार हैं- ( १ ) ज्ञानोपघात—यह आचार्य अल्पश्रुत है या ज्ञान को छिपाता है, (२) दर्शनोपघात — यह आचार्य उन्मार्ग की प्ररूपणा या उसमें श्रद्धा करता है, (३) चारित्रोपघात — यह आचार्य कुशील है या पार्श्वस्थ (पाशस्थ ) है, इत्यादि प्रकार से व्यवहार करने वाला आचार्य का उपघाती होता है। अथवा जो शिष्य आचार्य की वृत्ति (जीवनयात्रा) का उपघात करता है, वह भी बुद्धोपघाती है।
·
उदाहरण—कोई वृद्ध गणिगुणसम्पन्न आचार्य विहार करना चाहते हुए भी जंघाबल क्षीण होने के कारण एक नगर में स्थिरवासी हो गए। वहाँ के श्रावकगण भी अपना अहोभाग्य समझ कर उनकी सेवा करते थे, किन्तु आचार्य को दीर्घजीवी देख गुरुकर्मा शिष्य सोचने लगे—हम लोग कब तक इन अजंगम (अगतिशील) की परिचर्या करते रहेंगे? अतः ऐसा कोई उपाय करें, जिससे आचार्य स्वयं अनशन कर लें। वहाँ के श्रावकगण तो प्रतिदिन सरस आहार लेने के लिए भिक्षा करने वाले साधुओं को आग्रह करते, परन्तु वे भिक्षा में पूर्ण नीरस आहार लाते और कहते — "भंते! हम क्या करें? यहाँ के श्रावक लोग अच्छा आहार देते ही नहीं, वे विवेकहीन हैं। " उधर श्रावक लोगों के द्वारा सरस आहार लेने का आग्रह करने पर साधु उन्हें कहते" आचार्य शरीर - निर्वाह के प्रति अत्यन्त निरपेक्ष हो गए हैं, अब वे सरस, स्निग्ध आहार नहीं लेना चाहते। वे यथाशीघ्र संलेखना करना चाहते हैं।" यह सुन कर श्रद्धालु भक्त श्रावकों ने आकर सविनय प्रार्थना की— "भगवन्! आप भुवनभास्कर तेजस्वी परोपकारी आचार्य हैं। आप हमारे लिए भारभूत नहीं हैं। हम यथाशक्ति आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आपकी सेवा करके हम स्वयं को धन्य समझते हैं। आपके शिष्य साधु भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, वे भी आपसे क्षुब्ध नहीं हैं। फिर आप असमय में ही संलेखना क्यों कर रहे हैं?" इंगितज्ञ आचार्य ने जान लिया कि शिष्यों की बुद्धि विकृत होने के कारण ऐसा हुआ है। अतः अब इस अप्रीतिहेतुक प्राण-धारण से क्या प्रयोजन है? धर्मार्थी पुरुष को अप्रीति उत्पन्न करना उचित नहीं । अतः वे तत्काल श्रावकों से कहते हैं-"मैं स्थिरवासी होकर कितने दिन तक इन विनीत साधुओं और आप श्रावकगण को सेवा में रोके रखूंगा? अतः श्रेष्ठ यही है कि मैं उत्तम अर्थ को स्वीकार करूँ।" इस प्रकार श्रावकों को समझाकर आचार्य ने अनशन कर लिया।
१. बृहद्वृत्ति, पत्र ६२