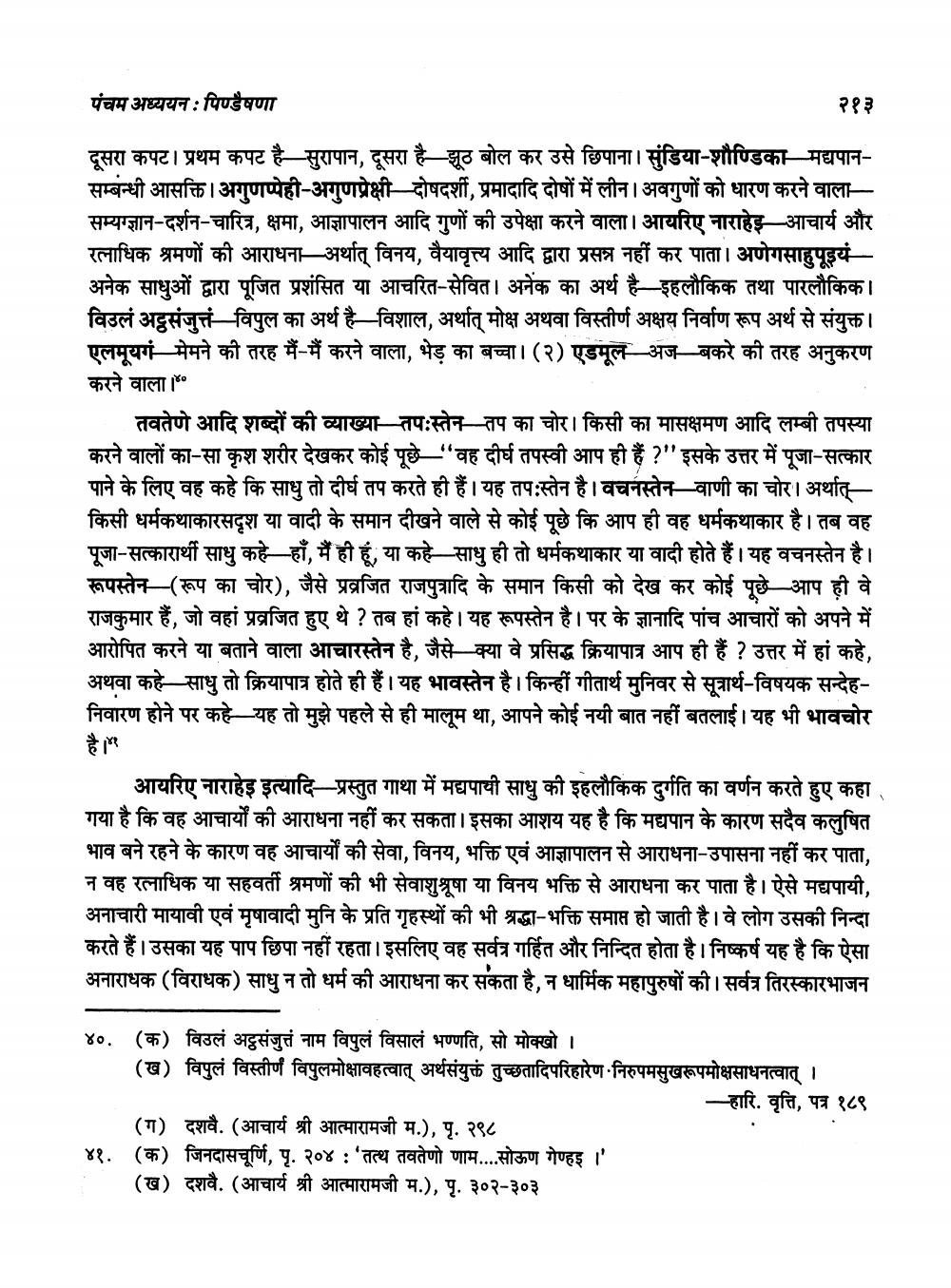________________
पंचम अध्ययन : पिण्डैषणा
२१३
दूसरा कपट । प्रथम कपट है— सुरापान, दूसरा है—झूठ बोल कर उसे छिपाना। सुंडिया - शौण्डिका मद्यपानसम्बंन्धी आसक्ति। अगुणप्पेही - अगुणप्रेक्षी —— दोषदर्शी, प्रमादादि दोषों में लीन । अवगुणों को धारण करने वाला— सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र, क्षमा, आज्ञापालन आदि गुणों की उपेक्षा करने वाला। आयरिए नाराहेइ – आचार्य और रत्नाधिक श्रमणों की आराधना —— अर्थात् विनय, वैयावृत्त्य आदि द्वारा प्रसन्न नहीं कर पाता । अणेगसाहुइयं— अनेक साधुओं द्वारा पूजित प्रशंसित या आचरित - सेवित । अनेक का अर्थ है— इहलौकिक तथा पारलौकिक । विडलं अट्ठसंजुत्तं विपुल का अर्थ है- विशाल, अर्थात् मोक्ष अथवा विस्तीर्ण अक्षय निर्वाण रूप अर्थ से संयुक्त । एलमूगं— मेमने की तरह मैं-मैं करने वाला, भेड़ का बच्चा । (२) एडमूल – अज—– बकरे की तरह अनुकरण करने वाला ।
तव आदि शब्दों की व्याख्या— तपः स्तेन — तप का चोर। किसी का मासक्षमण आदि लम्बी तपस्या करने वालों का-सा कृश शरीर देखकर कोई पूछे" वह दीर्घ तपस्वी आप ही हैं ?" इसके उत्तर में पूजा-सत्कार पाने के लिए वह कहे कि साधु तो दीर्घ तप करते ही हैं। यह तप:स्तेन है। वचनस्तेन वाणी का चोर । अर्थात् किसी धर्मकथाकारसदृश या वादी के समान दीखने वाले से कोई पूछे कि आप ही वह धर्मकथाकार है । तब वह पूजा - सत्कारार्थी साधु कहे — हाँ, मैं ही हूँ, या कहे—साधु ही तो धर्मकथाकार या वादी होते हैं। यह वचनस्तेन है। रूपस्तेन—(रूप का चोर), जैसे प्रव्रजित राजपुत्रादि के समान किसी को देख कर कोई पूछे आप ही वे राजकुमार हैं, जो वहां प्रव्रजित हुए थे ? तब हां कहे। यह रूपस्तेन है । पर के ज्ञानादि पांच आचारों को अपने में आरोपित करने या बताने वाला आचारस्तेन है, जैसे- क्या वे प्रसिद्ध क्रियापात्र आप ही हैं ? उत्तर में हां कहे, अथवा कहे ——साधु तो क्रियापात्र होते ही हैं। यह भावस्तेन है। किन्हीं गीतार्थ मुनिवर से सूत्रार्थ - विषयक सन्देहनिवारण होने पर कहे—यह तो मुझे पहले से ही मालूम था, आपने कोई नयी बात नहीं बतलाई । यह भी भावचोर है।
आयरिए नाराहे इत्यादि - प्रस्तुत गाथा में मद्यपायी साधु की इहलौकिक दुर्गति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह आचार्यों की आराधना नहीं कर सकता। इसका आशय यह है कि मद्यपान के कारण सदैव कलुषित भाव बने रहने के कारण वह आचार्यों की सेवा, विनय, भक्ति एवं आज्ञापालन से आराधना-उपासना नहीं कर पाता, न वह रत्नाधिक या सहवर्ती श्रमणों की भी सेवाशुश्रूषा या विनय भक्ति से आराधना कर पाता है। ऐसे मद्यपायी, अनाचारी मायावी एवं मृषावादी मुनि के प्रति गृहस्थों की भी श्रद्धा-भक्ति समाप्त हो जाती है। वे लोग उसकी निन्दा करते हैं। उसका यह पाप छिपा नहीं रहता। इसलिए वह सर्वत्र गर्हित और निन्दित होता है। निष्कर्ष यह है कि ऐसा अनाराधक (विराधक) साधु न तो धर्म की आराधना कर सकता है, न धार्मिक महापुरुषों की । सर्वत्र तिरस्कारभाजन
४०.
४१.
(क) विउलं अट्ठसंजुत्तं नाम विपुलं विसालं भण्णति, सो मोक्खो ।
(ख) विपुलं विस्तीर्णं विपुलमोक्षावहत्वात् अर्थसंयुक्तं तुच्छतादिपरिहारेण निरुपमसुखरूपमोक्षसाधनत्वात् ।
-हारि वृत्ति, पत्र १८९
(ग) दशवै. ( आचार्य श्री आत्मारामजी म.), पृ. २९८
(क) जिनदासचूर्णि, पृ. २०४ : 'तत्थ तवतेणो णाम.... सोऊण गेण्हइ ।' (ख) दशवै. ( आचार्य श्री आत्मारामजी म.), पृ. ३०२ - ३०३