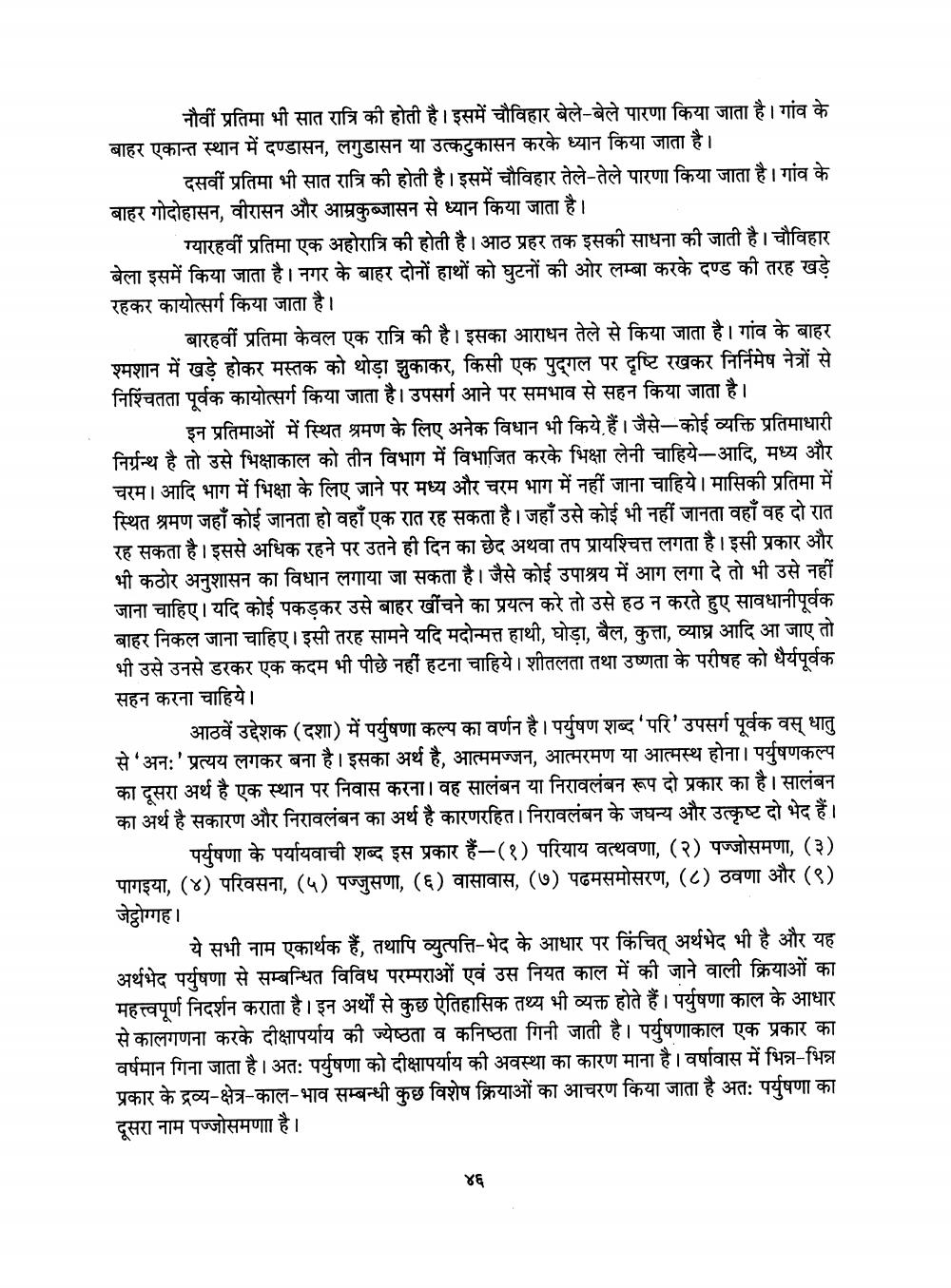________________
नौवीं प्रतिमा भी सात रात्रि की होती है। इसमें चौविहार बेले-बेले पारणा किया जाता है। गांव के बाहर एकान्त स्थान में दण्डासन, लगुडासन या उत्कटुकासन करके ध्यान किया जाता है।
दसवीं प्रतिमा भी सात रात्रि की होती है। इसमें चौविहार तेले-तेले पारणा किया जाता है। गांव के बाहर गोदोहासन, वीरासन और आम्रकुब्जासन से ध्यान किया जाता है।
ग्यारहवीं प्रतिमा एक अहोरात्रि की होती है। आठ प्रहर तक इसकी साधना की जाती है। चौविहार बेला इसमें किया जाता है। नगर के बाहर दोनों हाथों को घुटनों की ओर लम्बा करके दण्ड की तरह खड़े रहकर कायोत्सर्ग किया जाता है।
___ बारहवीं प्रतिमा केवल एक रात्रि की है। इसका आराधन तेले से किया जाता है। गांव के बाहर श्मशान में खड़े होकर मस्तक को थोड़ा झुकाकर, किसी एक पुद्गल पर दृष्टि रखकर निर्निमेष नेत्रों से निश्चितता पूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता है। उपसर्ग आने पर समभाव से सहन किया जाता है।
इन प्रतिमाओं में स्थित श्रमण के लिए अनेक विधान भी किये हैं। जैसे-कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी निर्ग्रन्थ है तो उसे भिक्षाकाल को तीन विभाग में विभाजित करके भिक्षा लेनी चाहिये-आदि, मध्य और चरम। आदि भाग में भिक्षा के लिए जाने पर मध्य और चरम भाग में नहीं जाना चाहिये। मासिकी प्रतिमा में स्थित श्रमण जहाँ कोई जानता हो वहाँ एक रात रह सकता है। जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता वहाँ वह दो रात रह सकता है। इससे अधिक रहने पर उतने ही दिन का छेद अथवा तप प्रायश्चित्त लगता है। इसी प्रकार और भी कठोर अनुशासन का विधान लगाया जा सकता है। जैसे कोई उपाश्रय में आग लगा दे तो भी उसे नहीं जाना चाहिए। यदि कोई पकड़कर उसे बाहर खींचने का प्रयत्न करे तो उसे हठ न करते हुए सावधानीपूर्वक बाहर निकल जाना चाहिए। इसी तरह सामने यदि मदोन्मत्त हाथी, घोड़ा, बैल, कुत्ता, व्याघ्र आदि आ जाए तो भी उसे उनसे डरकर एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिये। शीतलता तथा उष्णता के परीषह को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिये।
आठवें उद्देशक (दशा) में पर्युषणा कल्प का वर्णन है। पर्युषण शब्द 'परि' उपसर्ग पूर्वक वस् धातु से 'अनः' प्रत्यय लगकर बना है। इसका अर्थ है, आत्ममज्जन, आत्मरमण या आत्मस्थ होना। पर्युषणकल्प का दूसरा अर्थ है एक स्थान पर निवास करना। वह सालंबन या निरावलंबन रूप दो प्रकार का है। सालंबन का अर्थ है सकारण और निरावलंबन का अर्थ है कारणरहित। निरावलंबन के जघन्य और उत्कृष्ट दो भेद हैं।
पर्युषणा के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं-(१) परियाय वत्थवणा, (२) पज्जोसमणा, (३) पागइया, (४) परिवसना, (५) पज्जुसणा, (६) वासावास, (७) पढमसमोसरण, (८) ठवणा और (९) जेट्ठोग्गह।
ये सभी नाम एकार्थक हैं, तथापि व्युत्पत्ति-भेद के आधार पर किंचित् अर्थभेद भी है और यह अर्थभेद पर्युषणा से सम्बन्धित विविध परम्पराओं एवं उस नियत काल में की जाने वाली क्रियाओं का महत्त्वपूर्ण निदर्शन कराता है। इन अर्थों से कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी व्यक्त होते हैं। पर्युषणा काल के आधार से कालगणना करके दीक्षापर्याय की ज्येष्ठता व कनिष्ठता गिनी जाती है। पर्युषणाकाल एक प्रकार का वर्षमान गिना जाता है। अतः पर्युषणा को दीक्षापर्याय की अवस्था का कारण माना है। वर्षावास में भिन्न-भिन्न प्रकार के द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव सम्बन्धी कुछ विशेष क्रियाओं का आचरण किया जाता है अतः पर्युषणा का दूसरा नाम पज्जोसमणा है।