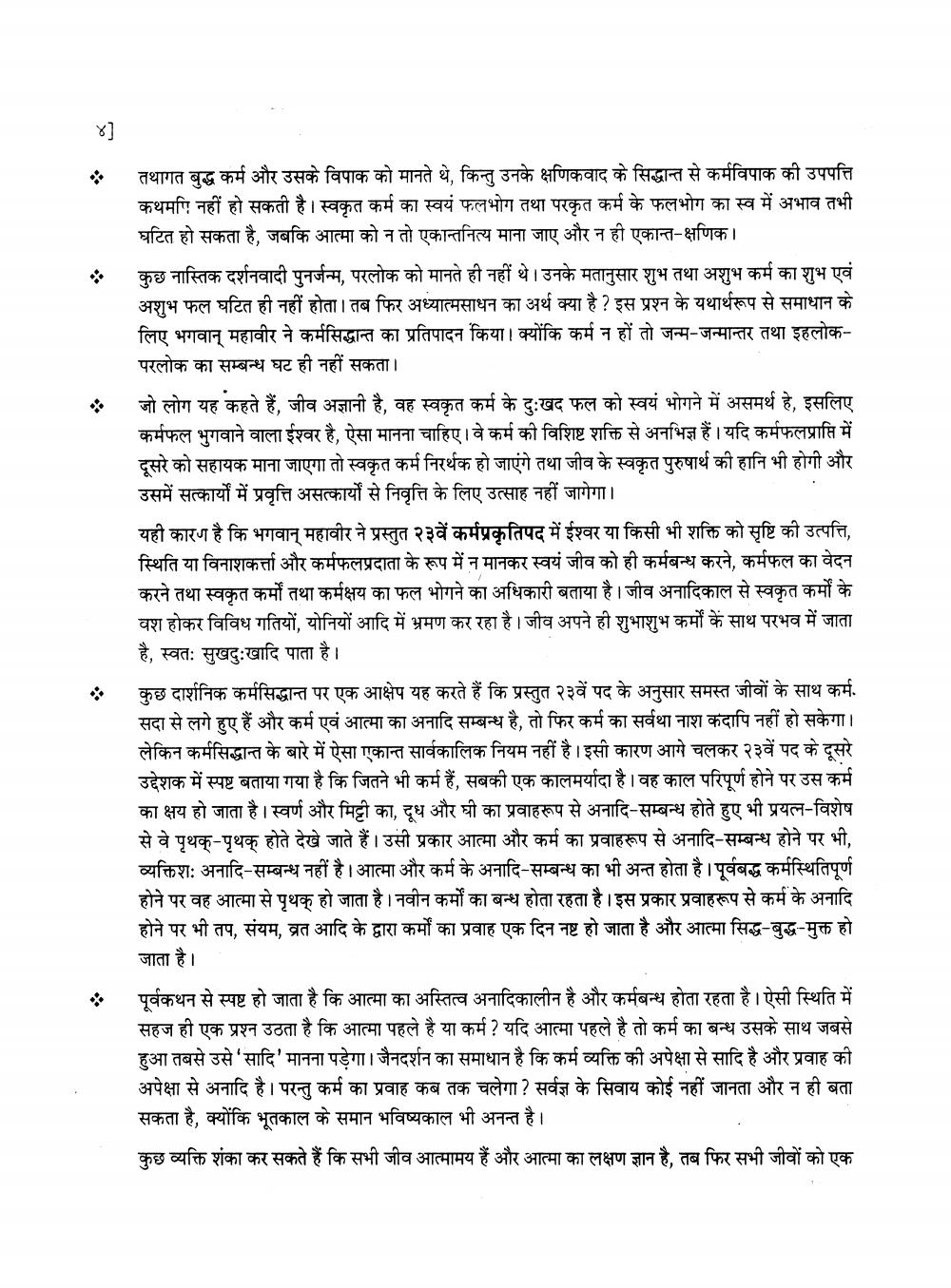________________
*
तथागत बुद्ध कर्म और उसके विपाक को मानते थे, किन्तु उनके क्षणिकवाद के सिद्धान्त से कर्मविपाक की उपपत्ति कथमपि नहीं हो सकती है। स्वकत कर्म का स्वयं फलभोग तथा परकत कर्म के फलभोग का स्व में अभाव तभी घटित हो सकता है, जबकि आत्मा को न तो एकान्तनित्य माना जाए और न ही एकान्त-क्षणिक। कुछ नास्तिक दर्शनवादी पुनर्जन्म, परलोक को मानते ही नहीं थे। उनके मतानुसार शुभ तथा अशुभ कर्म का शुभ एवं अशुभ फल घटित ही नहीं होता। तब फिर अध्यात्मसाधन का अर्थ क्या है ? इस प्रश्न के यथार्थरूप से समाधान के लिए भगवान् महावीर ने कर्मसिद्धान्त का प्रतिपादन किया। क्योंकि कर्म न हों तो जन्म-जन्मान्तर तथा इहलोकपरलोक का सम्बन्ध घट ही नहीं सकता। जो लोग यह कहते हैं, जीव अज्ञानी है, वह स्वकृत कर्म के दुःखद फल को स्वयं भोगने में असमर्थ हे, इसलिए कर्मफल भुगवाने वाला ईश्वर है, ऐसा मानना चाहिए। वे कर्म की विशिष्ट शक्ति से अनभिज्ञ हैं। यदि कर्मफलप्राप्ति में दूसरे को सहायक माना जाएगा तो स्वकृत कर्म निरर्थक हो जाएंगे तथा जीव के स्वकृत पुरुषार्थ की हानि भी होगी और उसमें सत्कार्यों में प्रवृत्ति असत्कार्यों से निवृत्ति के लिए उत्साह नहीं जागेगा। यही कारण है कि भगवान् महावीर ने प्रस्तुत २३वें कर्मप्रकृतिपद में ईश्वर या किसी भी शक्ति को सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति या विनाशकर्ता और कर्मफलप्रदाता के रूप में न मानकर स्वयं जीव को ही कर्मबन्ध करने, कर्मफल का वेदन करने तथा स्वकृत कर्मों तथा कर्मक्षय का फल भोगने का अधिकारी बताया है। जीव अनादिकाल से स्वकृत कर्मों के वश होकर विविध गतियों, योनियों आदि में भ्रमण कर रहा है। जीव अपने ही शुभाशुभ कर्मों के साथ परभव में जाता है, स्वतः सुखदुःखादि पाता है। कुछ दार्शनिक कर्मसिद्धान्त पर एक आक्षेप यह करते हैं कि प्रस्तुत २३वें पद के अनुसार समस्त जीवों के साथ कर्म. सदा से लगे हुए हैं और कर्म एवं आत्मा का अनादि सम्बन्ध है, तो फिर कर्म का सर्वथा नाश कदापि नहीं हो सकेगा। लेकिन कर्मसिद्धान्त के बारे में ऐसा एकान्त सार्वकालिक नियम नहीं है। इसी कारण आगे चलकर २३वें पद के दूसरे उद्देशक में स्पष्ट बताया गया है कि जितने भी कर्म हैं, सबकी एक कालमर्यादा है। वह काल परिपूर्ण होने पर उस कर्म का क्षय हो जाता है। स्वर्ण और मिट्टी का, दूध और घी का प्रवाहरूप से अनादि-सम्बन्ध होते हुए भी प्रयत्न-विशेष से वे पृथक्-पृथक् होते देखे जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा और कर्म का प्रवाहरूप से अनादि-सम्बन्ध होने पर भी, व्यक्तिशः अनादि-सम्बन्ध नहीं है। आत्मा और कर्म के अनादि-सम्बन्ध का भी अन्त होता है। पूर्वबद्ध कर्मस्थितिपूर्ण होने पर वह आत्मा से पृथक् हो जाता है। नवीन कर्मों का बन्ध होता रहता है। इस प्रकार प्रवाहरूप से कर्म के अनादि होने पर भी तप, संयम, व्रत आदि के द्वारा कर्मों का प्रवाह एक दिन नष्ट हो जाता है और आत्मा सिद्ध-बुद्ध-मुक्त हो जाता है। पूर्वकथन से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा का अस्तित्व अनादिकालीन है और कर्मबन्ध होता रहता है। ऐसी स्थिति में सहज ही एक प्रश्न उठता है कि आत्मा पहले है या कर्म? यदि आत्मा पहले है तो कर्म का बन्ध उसके साथ जबसे हुआ तबसे उसे 'सादि' मानना पड़ेगा। जैनदर्शन का समाधान है कि कर्म व्यक्ति की अपेक्षा से सादि है और प्रवाह की अपेक्षा से अनादि है। परन्तु कर्म का प्रवाह कब तक चलेगा? सर्वज्ञ के सिवाय कोई नहीं जानता और न ही बता सकता है, क्योंकि भूतकाल के समान भविष्यकाल भी अनन्त है। कुछ व्यक्ति शंका कर सकते हैं कि सभी जीव आत्मामय हैं और आत्मा का लक्षण ज्ञान है, तब फिर सभी जीवों को एक