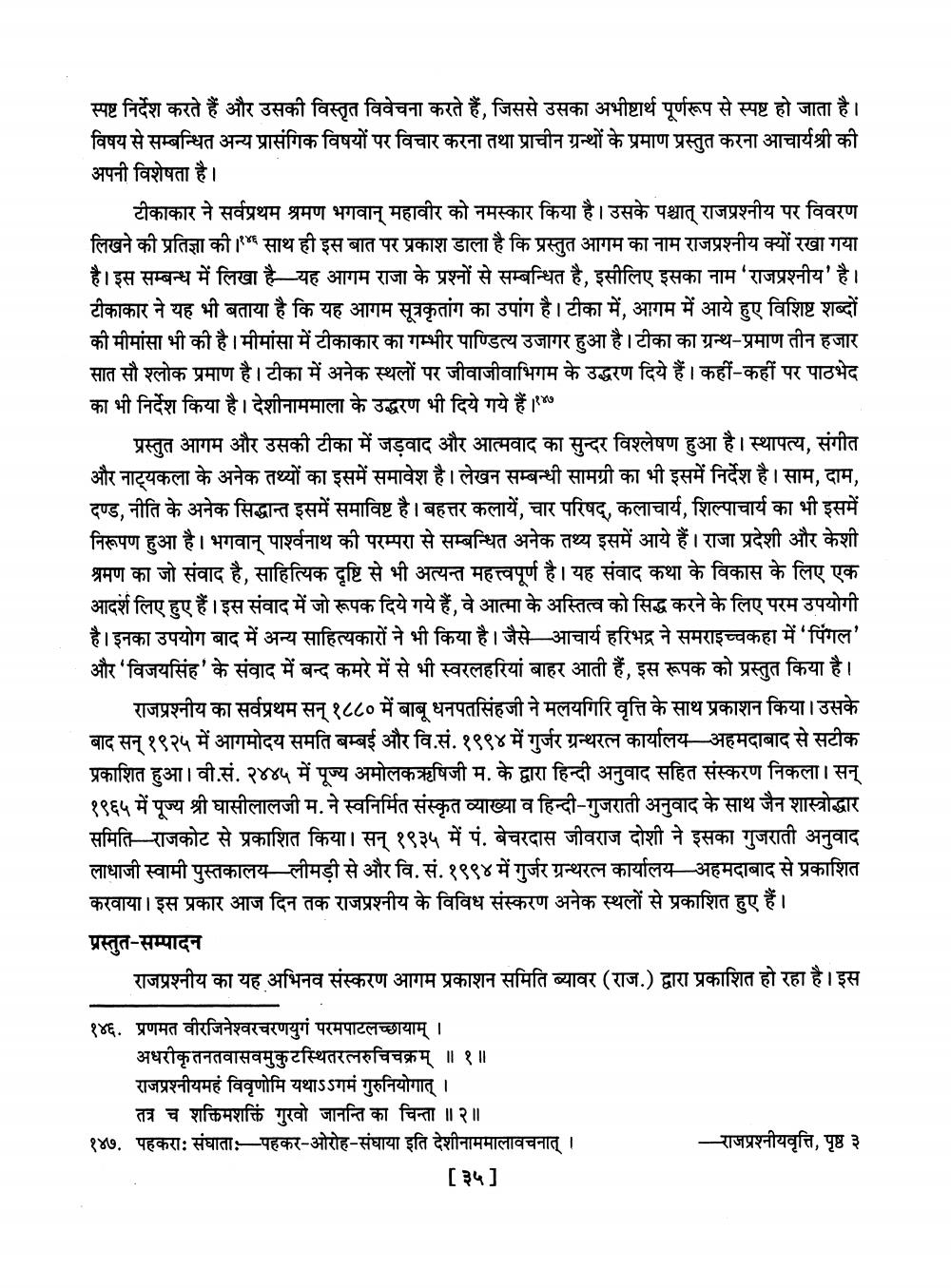________________
स्पष्ट निर्देश करते हैं और उसकी विस्तृत विवेचना करते हैं, जिससे उसका अभीष्टार्थ पूर्णरूप से स्पष्ट हो जाता है। विषय से सम्बन्धित अन्य प्रासंगिक विषयों पर विचार करना तथा प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण प्रस्तुत करना आचार्यश्री की अपनी विशेषता है। ___टीकाकार ने सर्वप्रथम श्रमण भगवान् महावीर को नमस्कार किया है। उसके पश्चात् राजप्रश्नीय पर विवरण लिखने की प्रतिज्ञा की।४६ साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला है कि प्रस्तुत आगम का नाम राजप्रश्नीय क्यों रखा गया है। इस सम्बन्ध में लिखा है—यह आगम राजा के प्रश्नों से सम्बन्धित है, इसीलिए इसका नाम 'राजप्रश्नीय' है। टीकाकार ने यह भी बताया है कि यह आगम सूत्रकृतांग का उपांग है। टीका में, आगम में आये हुए विशिष्ट शब्दों की मीमांसा भी की है। मीमांसा में टीकाकार का गम्भीर पाण्डित्य उजागर हुआ है। टीका का ग्रन्थ-प्रमाण तीन हजार सात सौ श्लोक प्रमाण है। टीका में अनेक स्थलों पर जीवाजीवाभिगम के उद्धरण दिये हैं। कहीं-कहीं पर पाठभेद का भी निर्देश किया है। देशीनाममाला के उद्धरण भी दिये गये हैं।१४७
प्रस्तुत आगम और उसकी टीका में जड़वाद और आत्मवाद का सुन्दर विश्लेषण हुआ है। स्थापत्य, संगीत और नाट्यकला के अनेक तथ्यों का इसमें समावेश है। लेखन सम्बन्धी सामग्री का भी इसमें निर्देश है। साम, दाम, दण्ड, नीति के अनेक सिद्धान्त इसमें समाविष्ट है। बहत्तर कलायें, चार परिषद्, कलाचार्य, शिल्पाचार्य का भी इसमें निरूपण हुआ है। भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा से सम्बन्धित अनेक तथ्य इसमें आये हैं। राजा प्रदेशी और केशी श्रमण का जो संवाद है, साहित्यिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह संवाद कथा के विकास के लिए एक आदर्श लिए हुए हैं। इस संवाद में जो रूपक दिये गये हैं, वे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए परम उपयोगी है। इनका उपयोग बाद में अन्य साहित्यकारों ने भी किया है। जैसे—आचार्य हरिभद्र ने समराइच्चकहा में 'पिंगल' और 'विजयसिंह' के संवाद में बन्द कमरे में से भी स्वरलहरियां बाहर आती हैं, इस रूपक को प्रस्तुत किया है। ___ राजप्रश्नीय का सर्वप्रथम सन् १८८० में बाबू धनपतसिंहजी ने मलयगिरि वृत्ति के साथ प्रकाशन किया। उसके बाद सन् १९२५ में आगमोदय समति बम्बई और वि.सं. १९९४ में गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय—अहमदाबाद से सटीक प्रकाशित हुआ। वी.सं. २४४५ में पूज्य अमोलकऋषिजी म. के द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित संस्करण निकला। सन् १९६५ में पूज्य श्री घासीलालजी म. ने स्वनिर्मित संस्कृत व्याख्या व हिन्दी-गुजराती अनुवाद के साथ जैन शास्त्रोद्धार समिति–राजकोट से प्रकाशित किया। सन् १९३५ में पं. बेचरदास जीवराज दोशी ने इसका गुजराती अनुवाद लाधाजी स्वामी पुस्तकालय—लीमड़ी से और वि.सं. १९९४ में गुर्जर ग्रन्थरत्न कार्यालय अहमदाबाद से प्रकाशित करवाया। इस प्रकार आज दिन तक राजप्रश्नीय के विविध संस्करण अनेक स्थलों से प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत-सम्पादन
राजप्रश्नीय का यह अभिनव संस्करण आगम प्रकाशन समिति ब्यावर (राज.) द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इस
१४६. प्रणमत वीरजिनेश्वरचरणयुगं परमपाटलच्छायाम् ।
अधरीकृतनतवासवमुकुटस्थितरत्नरुचिचक्रम् ॥ १॥ राजप्रश्नीयमहं विवृणोमि यथाऽऽगमं गुरुनियोगात् ।
तत्र च शक्तिमशक्तिं गुरवो जानन्ति का चिन्ता ॥ २॥ १४७. पहकराः संघाता:-पहकर-ओरोह-संघाया इति देशीनाममालावचनात् ।
[३५]
राजप्रश्नीयवृत्ति, पृष्ठ ३