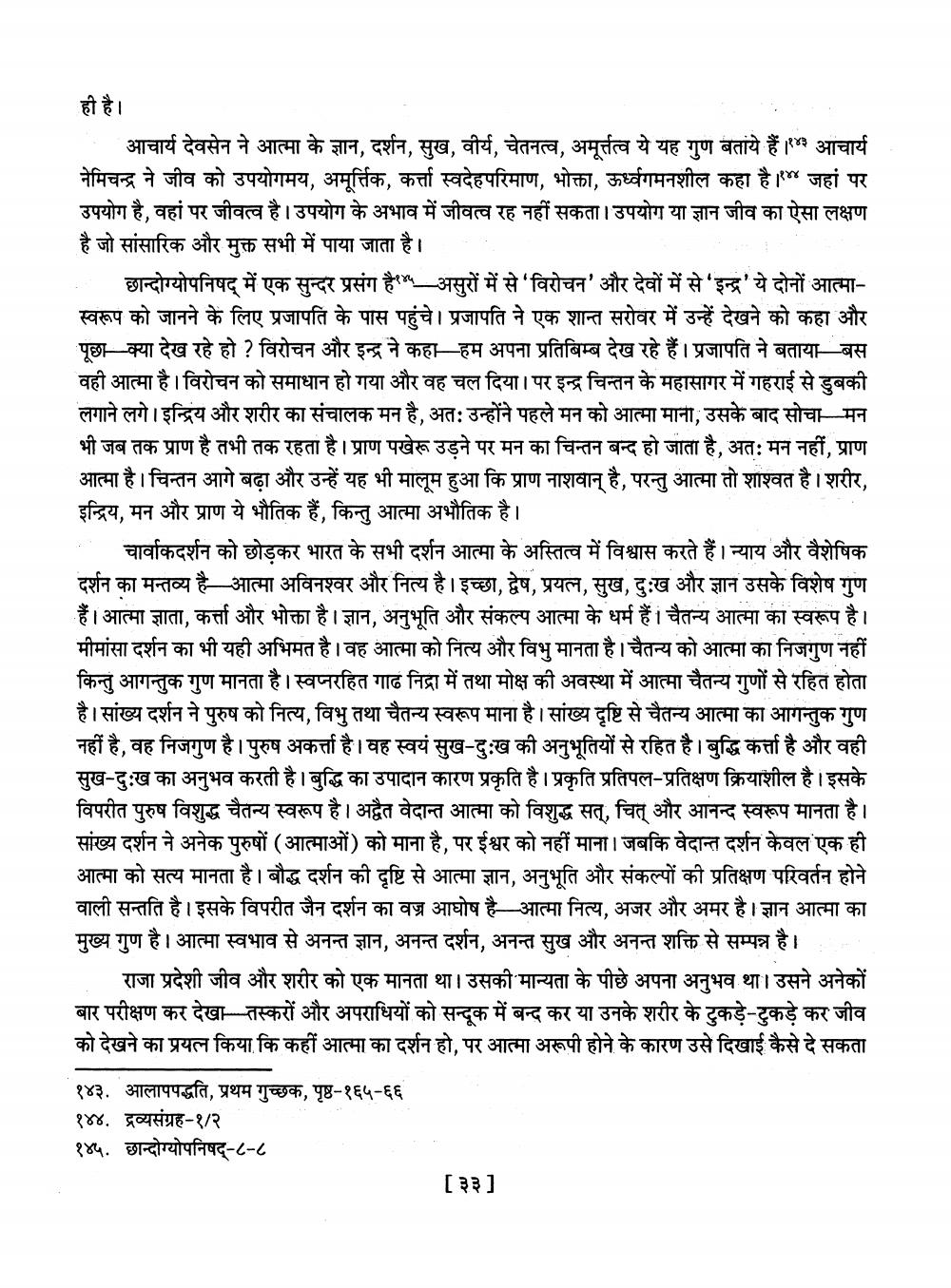________________
ही है।
आचार्य देवसेन ने आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चेतनत्व, अमूर्त्तत्व ये यह गुण बताये हैं । १४३ आचार्य नेमिचन्द्र ने जीव को उपयोगमय, अमूर्त्तिक, कर्त्ता स्वदेहपरिमाण, भोक्ता, ऊर्ध्वगमनशील कहा है ।१४४ जहां पर उपयोग है, वहां पर जीवत्व है। उपयोग के अभाव में जीवत्व रह नहीं सकता। उपयोग या ज्ञान जीव का ऐसा लक्षण है जो सांसारिक और मुक्त सभी में पाया जाता है।
छान्दोग्योपनिषद् में एक सुन्दर प्रसंग है ९४५ असुरों में से 'विरोचन' और देवों में से 'इन्द्र' ये दोनों आत्मास्वरूप को जानने के लिए प्रजापति के पास पहुंचे । प्रजापति ने एक शान्त सरोवर में उन्हें देखने को कहा और पूछा- क्या देख रहे हो ? विरोचन और इन्द्र ने कहा- हम अपना प्रतिबिम्ब देख रहे हैं। प्रजापति ने बताया- बस वही आत्मा है। विरोचन को समाधान हो गया और वह चल दिया। पर इन्द्र चिन्तन के महासागर में गहराई से डुबकी लगाने लगे। इन्द्रिय और शरीर का संचालक मन है, अतः उन्होंने पहले मन को आत्मा माना, उसके बाद सोचा न भी जब तक प्राण है तभी तक रहता है। प्राण पखेरू उड़ने पर मन का चिन्तन बन्द हो जाता है, अतः मन नहीं, प्राण आत्मा है। चिन्तन आगे बढ़ा और उन्हें यह भी मालूम हुआ कि प्राण नाशवान् है, परन्तु आत्मा तो शाश्वत है। शरीर, इन्द्रिय, मन और प्राण ये भौतिक हैं, किन्तु आत्मा अभौतिक है।
चार्वाकदर्शन को छोड़कर भारत के सभी दर्शन आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन का मन्तव्य है — आत्मा अविनश्वर और नित्य है। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान उसके विशेष गुण हैं। आत्मा ज्ञाता, कर्त्ता और भोक्ता है। ज्ञान, अनुभूति और संकल्प आत्मा के धर्म हैं। चैतन्य आत्मा का स्वरूप है। मीमांसा दर्शन का भी यही अभिमत है। वह आत्मा को नित्य और विभु मानता है। चैतन्य को आत्मा का निजगुण नहीं किन्तु आगन्तुक गुण मानता है। स्वप्नरहित गाढ निद्रा में तथा मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य गुणों से रहित होता है। सांख्य दर्शन ने पुरुष को नित्य, विभु तथा चैतन्य स्वरूप माना है। सांख्य दृष्टि से चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण नहीं है, वह निजगुण है। पुरुष अकर्त्ता है। वह स्वयं सुख-दुःख की अनुभूतियों से रहित है। बुद्धि कर्त्ता है और वही सुख-दुःख का अनुभव करती है। बुद्धि का उपादान कारण प्रकृति है। प्रकृति प्रतिपल-प्रतिक्षण क्रियाशील है। इसके विपरीत पुरुष विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है। अद्वैत वेदान्त आत्मा को विशुद्ध सत्, चित् और आनन्द स्वरूप मानता है। सांख्य दर्शन ने अनेक पुरुषों (आत्माओं) को माना है, पर ईश्वर को नहीं माना। जबकि वेदान्त दर्शन केवल एक ही आत्मा को सत्य मानता है। बौद्ध दर्शन की दृष्टि से आत्मा ज्ञान, अनुभूति और संकल्पों की प्रतिक्षण परिवर्तन होने वाली सन्तति है । इसके विपरीत जैन दर्शन का वज्र आघोष है— आत्मा नित्य, अजर और अमर है। ज्ञान आत्मा का मुख्य गुण है। आत्मा स्वभाव से अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त शक्ति से सम्पन्न है।
राजा प्रदेशी जीव और शरीर को एक मानता था । उसकी मान्यता के पीछे अपना अनुभव था । उसने अनेकों बार परीक्षण कर देखा तस्करों और अपराधियों को सन्दूक में बन्द कर या उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर जीव को देखने का प्रयत्न किया कि कहीं आत्मा का दर्शन हो, पर आत्मा अरूपी होने के कारण उसे दिखाई कैसे दे सकता
१४३. आलापपद्धति, प्रथम गुच्छक, पृष्ठ- १६५-६६
१४४. द्रव्यसंग्रह - १/२
१४५. छान्दोग्योपनिषद् - ८-८
[३३]