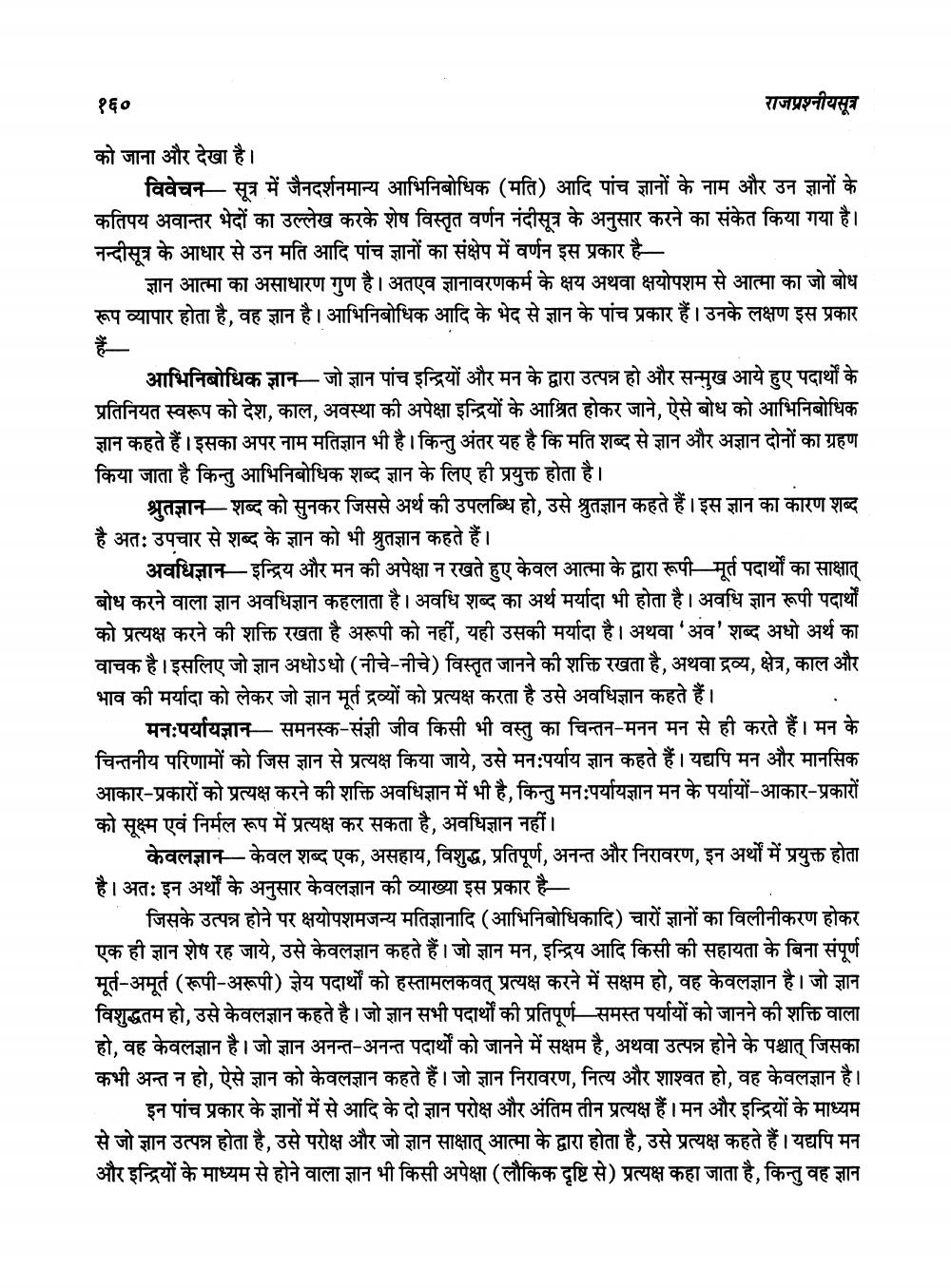________________
१६०
राजप्रश्नीयसूत्र
को जाना और देखा है।
विवेचन- सूत्र में जैनदर्शनमान्य आभिनिबोधिक (मति) आदि पांच ज्ञानों के नाम और उन ज्ञानों के कतिपय अवान्तर भेदों का उल्लेख करके शेष विस्तृत वर्णन नंदीसूत्र के अनुसार करने का संकेत किया गया है। नन्दीसूत्र के आधार से उन मति आदि पांच ज्ञानों का संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है
ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। अतएव ज्ञानावरणकर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम से आत्मा का जो बोध रूप व्यापार होता है, वह ज्ञान है। आभिनिबोधिक आदि के भेद से ज्ञान के पांच प्रकार हैं। उनके लक्षण इस प्रकार
___आभिनिबोधिक ज्ञान- जो ज्ञान पांच इन्द्रियों और मन के द्वारा उत्पन्न हो और सन्मुख आये हुए पदार्थों के प्रतिनियत स्वरूप को देश, काल, अवस्था की अपेक्षा इन्द्रियों के आश्रित होकर जाने, ऐसे बोध को आभिनिबोधिक ज्ञान कहते हैं। इसका अपर नाम मतिज्ञान भी है। किन्तु अंतर यह है कि मति शब्द से ज्ञान और अज्ञान दोनों का ग्रहण किया जाता है किन्तु आभिनिबोधिक शब्द ज्ञान के लिए ही प्रयुक्त होता है।
श्रुतज्ञान- शब्द को सुनकर जिससे अर्थ की उपलब्धि हो, उसे श्रुतज्ञान कहते हैं । इस ज्ञान का कारण शब्द है अतः उपचार से शब्द के ज्ञान को भी श्रुतज्ञान कहते हैं।
अवधिज्ञान- इन्द्रिय और मन की अपेक्षा न रखते हुए केवल आत्मा के द्वारा रूपी मूर्त पदार्थों का साक्षात् बोध करने वाला ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है। अवधि शब्द का अर्थ मर्यादा भी होता है। अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति रखता है अरूपी को नहीं, यही उसकी मर्यादा है। अथवा 'अव' शब्द अ वाचक है। इसलिए जो ज्ञान अधोऽधो (नीचे-नीचे) विस्तृत जानने की शक्ति रखता है, अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा को लेकर जो ज्ञान मूर्त द्रव्यों को प्रत्यक्ष करता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं।
____ मनःपर्यायज्ञान- समनस्क-संज्ञी जीव किसी भी वस्तु का चिन्तन-मनन मन से ही करते हैं। मन के चिन्तनीय परिणामों को जिस ज्ञान से प्रत्यक्ष किया जाये, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं। यद्यपि मन और मानसिक आकार-प्रकारों को प्रत्यक्ष करने की शक्ति अवधिज्ञान में भी है, किन्तु मनःपर्यायज्ञान मन के पर्यायों-आकार-प्रकारों को सूक्ष्म एवं निर्मल रूप में प्रत्यक्ष कर सकता है, अवधिज्ञान नहीं।
केवलज्ञान- केवल शब्द एक, असहाय, विशुद्ध, प्रतिपूर्ण, अनन्त और निरावरण, इन अर्थों में प्रयुक्त होता है। अतः इन अर्थों के अनुसार केवलज्ञान की व्याख्या इस प्रकार है
_ जिसके उत्पन्न होने पर क्षयोपशमजन्य मतिज्ञानादि (आभिनिबोधिकादि) चारों ज्ञानों का विलीनीकरण होकर एक ही ज्ञान शेष रह जाये, उसे केवलज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान मन, इन्द्रिय आदि किसी की सहायता के बिना संपूर्ण मूर्त-अमूर्त (रूपी-अरूपी) ज्ञेय पदार्थों को हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष करने में सक्षम हो, वह केवलज्ञान है। जो ज्ञान विशुद्धतम हो, उसे केवलज्ञान कहते है। जो ज्ञान सभी पदार्थों की प्रतिपूर्ण समस्त पर्यायों को जानने की शक्ति वाला हो, वह केवलज्ञान है। जो ज्ञान अनन्त-अनन्त पदार्थों को जानने में सक्षम है, अथवा उत्पन्न होने के पश्चात् जिसका कभी अन्त न हो, ऐसे ज्ञान को केवलज्ञान कहते हैं। जो ज्ञान निरावरण, नित्य और शाश्वत हो, वह केवलज्ञान है।
इन पांच प्रकार के ज्ञानों में से आदि के दो ज्ञान परोक्ष और अंतिम तीन प्रत्यक्ष हैं। मन और इन्द्रियों के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे परोक्ष और जो ज्ञान साक्षात् आत्मा के द्वारा होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । यद्यपि मन और इन्द्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान भी किसी अपेक्षा (लौकिक दृष्टि से) प्रत्यक्ष कहा जाता है, किन्तु वह ज्ञान