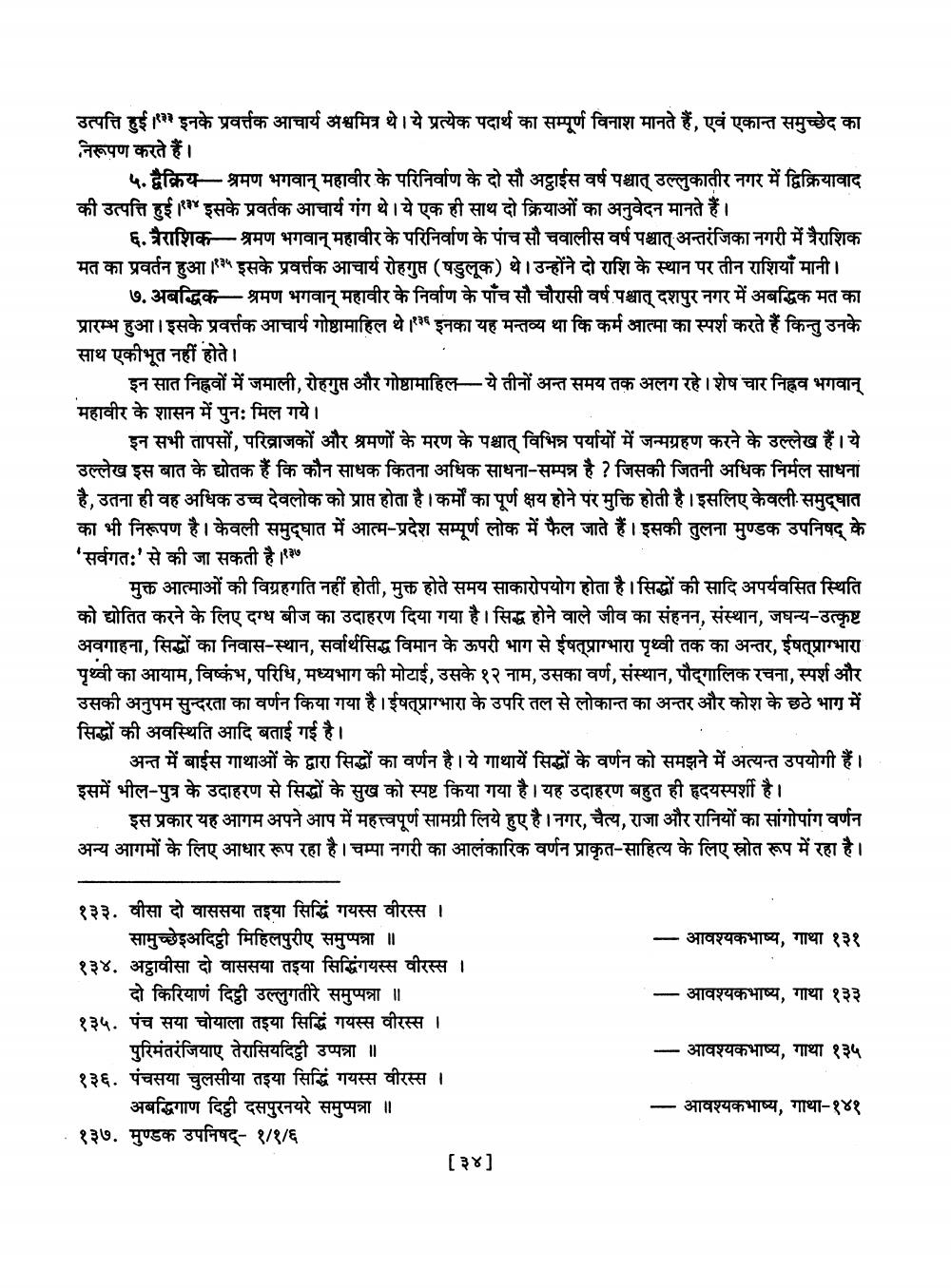________________
उत्पत्ति हुई। इनके प्रवर्तक आचार्य अश्वमित्र थे। ये प्रत्येक पदार्थ का सम्पूर्ण विनाश मानते हैं, एवं एकान्त समुच्छेद का निरूपण करते हैं।
५.द्वैक्रिय-श्रमण भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के दो सौ अट्ठाईस वर्ष पश्चात् उल्लुकातीर नगर में द्विक्रियावाद की उत्पत्ति हुई। इसके प्रवर्तक आचार्य गंग थे। ये एक ही साथ दो क्रियाओं का अनुवेदन मानते हैं।
६.त्रैराशिक-श्रमण भगवान् महावीर के परिनिर्वाण के पांच सौ चवालीस वर्ष पश्चात् अन्तरंजिका नगरी में त्रैराशिक मत का प्रवर्तन हुआ।१३५ इसके प्रवर्तक आचार्य रोहगुप्त (षडुलूक) थे। उन्होंने दो राशि के स्थान पर तीन राशियाँ मानी।
-श्रमण भगवान महावीर के निर्वाण के पाँच सौ चौरासी वर्ष पश्चात् दशपुर नगर में अबद्धिक मत का प्रारम्भ हुआ। इसके प्रवर्तक आचार्य गोष्ठामाहिल थे।३६ इनका यह मन्तव्य था कि कर्म आत्मा का स्पर्श करते हैं किन्तु उनके साथ एकीभूत नहीं होते।
इन सात निह्नवों में जमाली,रोहगुप्त और गोष्ठामाहिल-ये तीनों अन्त समय तक अलग रहे। शेष चार निहव भगवान् महावीर के शासन में पुनः मिल गये।
इन सभी तापसों, परिव्राजकों और श्रमणों के मरण के पश्चात् विभिन्न पर्यायों में जन्मग्रहण करने के उल्लेख हैं। ये उल्लेख इस बात के द्योतक हैं कि कौन साधक कितना अधिक साधना-सम्पन्न है ? जिसकी जितनी अधिक निर्मल साधना है, उतना ही वह अधिक उच्च देवलोक को प्राप्त होता है। कर्मों का पूर्ण क्षय होने पर मुक्ति होती है। इसलिए केवली. समुद्घात
का भी निरूपण है। केवली समुद्घात में आत्म-प्रदेश सम्पूर्ण लोक में फैल जाते हैं। इसकी तुलना मुण्डक उपनिषद् के 'सर्वगतः' से की जा सकती है ।१३७
मुक्त आत्माओं की विग्रहगति नहीं होती, मुक्त होते समय साकारोपयोग होता है। सिद्धों की सादि अपर्यवसित स्थिति को द्योतित करने के लिए दग्ध बीज का उदाहरण दिया गया है। सिद्ध होने वाले जीव का संहनन, संस्थान, जघन्य-उत्कृष्ट अवगाहना, सिद्धों का निवास स्थान, सर्वार्थसिद्ध विमान के ऊपरी भाग से ईषतप्रारभारा पृथ्वी तक का अन्तर, ईषतप्रारभारा पृथ्वी का आयाम, विष्कंभ, परिधि, मध्यभाग की मोटाई, उसके १२ नाम, उसका वर्ण, संस्थान, पौद्गालिक रचना, स्पर्श और उसकी अनुपम सुन्दरता का वर्णन किया गया है। ईषत्प्राग्भारा के उपरि तल से लोकान्त का अन्तर और कोश के छठे भाग में सिद्धों की अवस्थिति आदि बताई गई है।
अन्त में बाईस गाथाओं के द्वारा सिद्धों का वर्णन है। ये गाथायें सिद्धों के वर्णन को समझने में अत्यन्त उपयोगी हैं। इसमें भील-पुत्र के उदाहरण से सिद्धों के सुख को स्पष्ट किया गया है। यह उदाहरण बहुत ही हृदयस्पर्शी है।
. इस प्रकार यह आगम अपने आप में महत्त्वपूर्ण सामग्री लिये हुए है। नगर, चैत्य, राजा और रानियों का सांगोपांग वर्णन अन्य आगमों के लिए आधार रूप रहा है। चम्पा नगरी का आलंकारिक वर्णन प्राकृत-साहित्य के लिए स्रोत रूप में रहा है।
- आवश्यकभाष्य, गाथा १३१
- आवश्यकभाष्य, गाथा १३३
१३३. वीसा दो वाससया तइया सिद्धिं गयस्स वीरस्स ।
सामुच्छेइअदिट्ठी मिहिलपुरीए समुप्पन्ना ॥ १३४. अट्ठावीसा दो वाससया तइया सिद्धिंगयस्स वीरस्स ।
दो किरियाणं दिट्ठी उल्लगतीरे समुप्पन्ना ॥ १३५. पंच सया चोयाला तइया सिद्धिं गयस्स वीरस्स ।
पुरिमंतरंजियाए तेरासियदिट्ठी उप्पन्ना ॥ १३६. पंचसया चुलसीया तइया सिद्धिं गयस्स वीरस्स ।
अबद्धिगाण दिट्ठी दसपुरनयरे समुप्पन्ना ॥ १३७. मुण्डक उपनिषद्- १/१/६
[३४]
- आवश्यकभाष्य, गाथा १३५
- आवश्यकभाष्य, गाथा-१४१