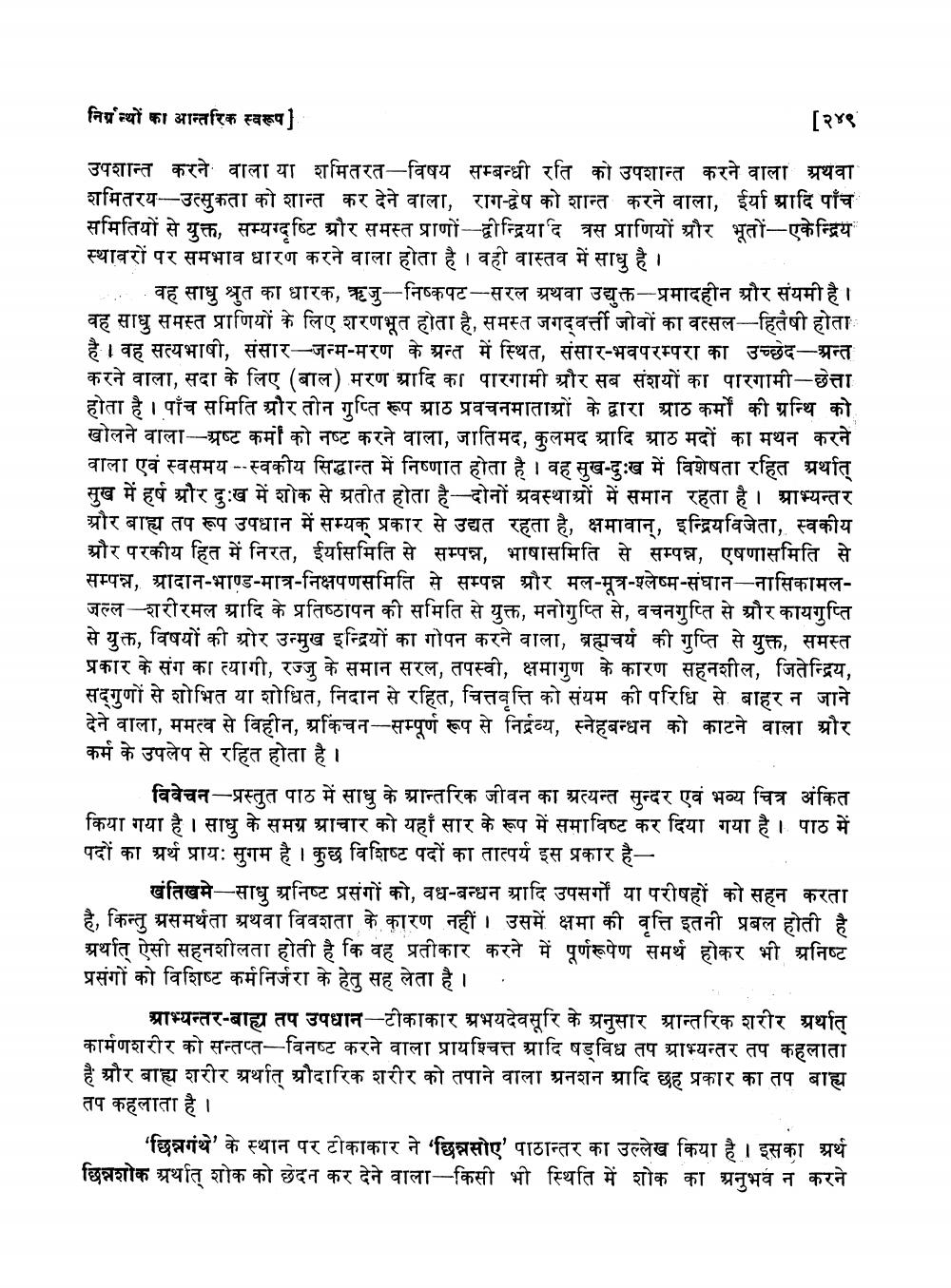________________
निर्ग्रन्थों का आन्तरिक स्वरूप]
[२४९
उपशान्त करने वाला या शमितरत-विषय सम्बन्धी रति को उपशान्त करने वाला अथवा शमितरय-उत्सुकता को शान्त कर देने वाला, राग-द्वेष को शान्त करने वाला, ईर्या आदि पाँच समितियों से युक्त, सम्यग्दृष्टि और समस्त प्राणों द्वीन्द्रिया द त्रस प्राणियों और भूतों-एकेन्द्रिय स्थावरों पर समभाव धारण करने वाला होता है । वही वास्तव में साधु है।
...... वह साधु श्रुत का धारक, ऋजु-निष्कपट-सरल अथवा उद्युक्त-प्रमादहीन और संयमी है। वह साधु समस्त प्राणियों के लिए शरणभूत होता है, समस्त जगद्वर्ती जोवों का वत्सल-हितैषी होता है । वह सत्यभाषी, संसार-जन्म-मरण के अन्त में स्थित, संसार-भवपरम्परा का उच्छेद–अन्त करने वाला, सदा के लिए (बाल) मरण आदि का पारगामी और सब संशयों का पारगामी-छेत्ता होता है । पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप पाठ प्रवचनमाताओं के द्वारा पाठ कर्मों की ग्रन्थि को खोलने वाला-अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाला, जातिमद, कुलमद आदि पाठ मदों का मथन करने वाला एवं स्वसमय -- स्वकीय सिद्धान्त में निष्णात होता है । वह सुख-दुःख में विशेषता रहित अर्थात् सुख में हर्ष और दुःख में शोक से प्रतीत होता है—दोनों अवस्थाओं में समान रहता है। प्राभ्यन्तर और बाह्य तप रूप उपधान में सम्यक् प्रकार से उद्यत रहता है, क्षमावान्, इन्द्रियविजेता, स्वकीय और परकीय हित में निरत, ईर्यासमिति से सम्पन्न, भाषासमिति से सम्पन्न, एषणासमिति से सम्पन्न, आदान-भाण्ड-मात्र-निक्षपणसमिति से सम्पन्न और मल-मूत्र-श्लेष्म-संघान–नासिकामलजल्ल-शरीरमल आदि के प्रतिष्ठापन की समिति से युक्त, मनोगुप्ति से, वचनगुप्ति से और कायगुप्ति से युक्त, विषयों की ओर उन्मुख इन्द्रियों का गोपन करने वाला, ब्रह्मचर्य की गुप्ति से युक्त, समस्त प्रकार के संग का त्यागी, रज्जु के समान सरल, तपस्वी, क्षमागुण के कारण सहनशील, जितेन्द्रिय, सद्गुणों से शोभित या शोधित, निदान से रहित, चित्तवृत्ति को संयम की परिधि से बाहर न जाने देने वाला, ममत्व से विहीन, अकिंचन-सम्पूर्ण रूप से निर्द्रव्य, स्नेहबन्धन को काटने वाला और कर्म के उपलेप से रहित होता है।
विवेचन-प्रस्तुत पाठ में साधु के आन्तरिक जीवन का अत्यन्त सुन्दर एवं भव्य चित्र अंकित किया गया है । साधु के समग्र प्राचार को यहाँ सार के रूप में समाविष्ट कर दिया गया है। पाठ में पदों का अर्थ प्रायः सुगम है । कुछ विशिष्ट पदों का तात्पर्य इस प्रकार है
खंतिखमे–साधु अनिष्ट प्रसंगों को, वध-बन्धन आदि उपसर्गों या परीषहों को सहन करता है, किन्तु असमर्थता अथवा विवशता के कारण नहीं। उसमें क्षमा की वृत्ति इतनी प्रबल होती है अर्थात् ऐसी सहनशीलता होती है कि वह प्रतीकार करने में पूर्णरूपेण समर्थ होकर भी अनिष्ट प्रसंगों को विशिष्ट कर्मनिर्जरा के हेतु सह लेता है। .
आभ्यन्तर-बाह्य तप उपधान-टीकाकार अभयदेवसूरि के अनुसार आन्तरिक शरीर अर्थात् कार्मणशरीर को सन्तप्त-विनष्ट करने वाला प्रायश्चित्त आदि षड्विध तपाभ्यन्तर तप कहलाता है और बाह्य शरीर अर्थात् प्रौदारिक शरीर को तपाने वाला अनशन आदि छह प्रकार का तप बाह्य तप कहलाता है।
"छिन्नगंथे' के स्थान पर टीकाकार ने 'छिन्नसोए' पाठान्तर का उल्लेख किया है । इसका अर्थ छिन्नशोक अर्थात् शोक को छेदन कर देने वाला-किसी भी स्थिति में शोक का अनुभव न करने