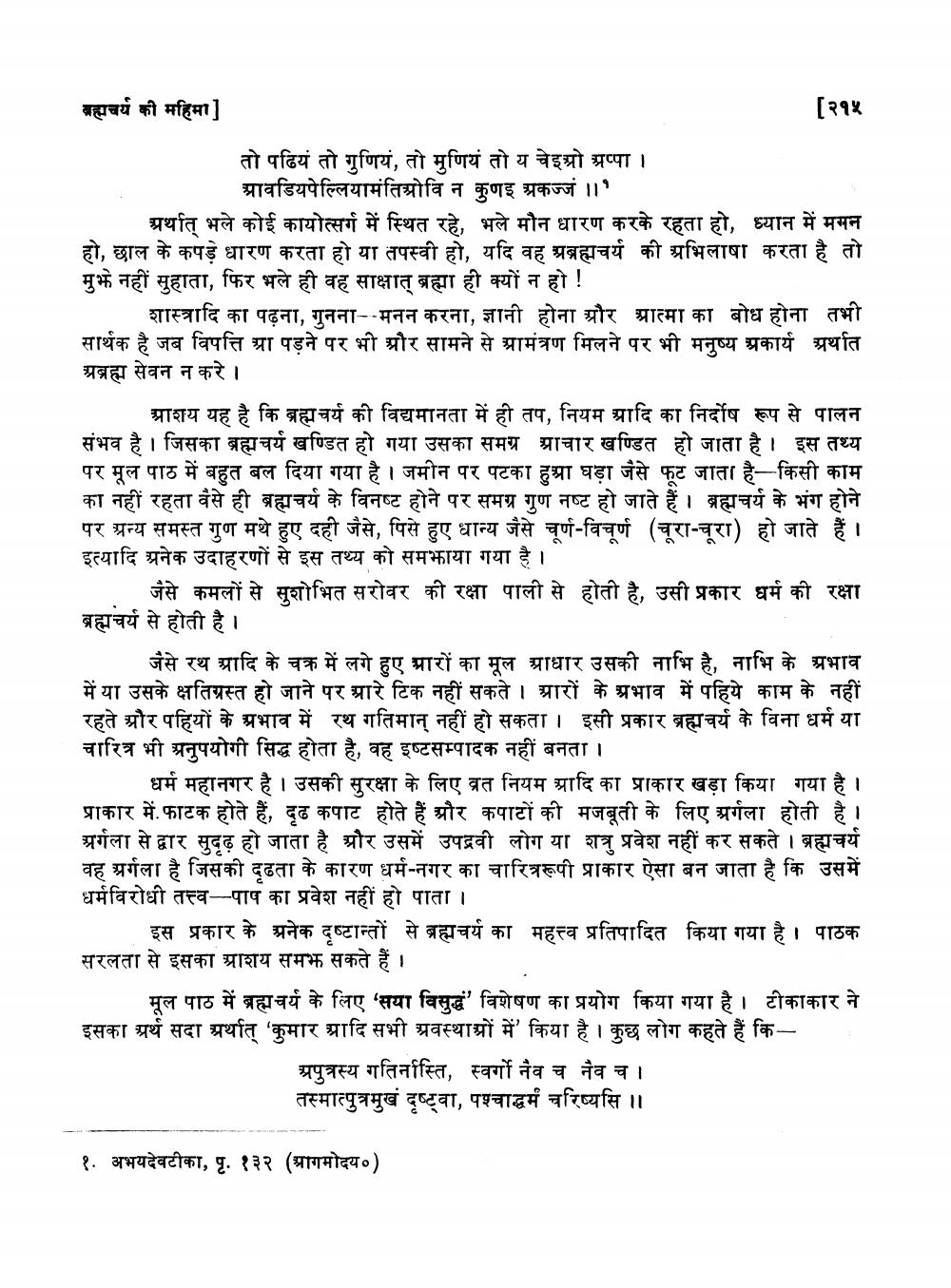________________
ब्रह्मचर्य की महिमा
[२१५
तो पढियं तो गुणियं, तो मणियं तो य चेइयो अप्पा ।
आवडियपेल्लियामंतिप्रोवि न कुणइ अकज्जं ।' अर्थात् भले कोई कायोत्सर्ग में स्थित रहे, भले मौन धारण करके रहता हो, ध्यान में ममन हो, छाल के कपड़े धारण करता हो या तपस्वी हो, यदि वह अब्रह्मचर्य की अभिलाषा करता है तो मुझे नहीं सुहाता, फिर भले ही वह साक्षात् ब्रह्मा ही क्यों न हो!
शास्त्रादि का पढ़ना, गुनना--मनन करना, ज्ञानी होना और आत्मा का बोध होना तभी सार्थक है जब विपत्ति आ पड़ने पर भी और सामने से आमंत्रण मिलने पर भी मनुष्य अकार्य अर्थात अब्रह्म सेवन न करे।
आशय यह है कि ब्रह्मचर्य की विद्यमानता में ही तप, नियम आदि का निर्दोष रूप से पालन संभव है। जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया उसका समग्र प्राचार खण्डित हो जाता है। इस तथ्य पर मूल पाठ में बहुत बल दिया गया है। जमीन पर पटका हुआ घड़ा जैसे फूट जाता है किसी काम का नहीं रहता वैसे ही ब्रह्मचर्य के विनष्ट होने पर समग्र गुण नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के भंग होने पर अन्य समस्त गुण मथे हुए दही जैसे, पिसे हुए धान्य जैसे चूर्ण-विचूर्ण (चूरा-चूरा) हो जाते हैं। इत्यादि अनेक उदाहरणों से इस तथ्य को समझाया गया है।
जैसे कमलों से सुशोभित सरोवर की रक्षा पाली से होती है, उसी प्रकार धर्म की रक्षा ब्रह्मचर्य से होती है।
जैसे रथ आदि के चक्र में लगे हुए पारों का मूल आधार उसकी नाभि है, नाभि के अभाव
उसके क्षतिग्रस्त हो जाने पर पारे टिक नहीं सकते । अारों के अभाव में पहिये काम के नहीं रहते और पहियों के अभाव में रथ गतिमान् नहीं हो सकता। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के विना धर्म या चारित्र भी अनुपयोगी सिद्ध होता है, वह इष्टसम्पादक नहीं बनता।
धर्म महानगर है । उसकी सुरक्षा के लिए व्रत नियम आदि का प्राकार खड़ा किया गया है । प्राकार में.फाटक होते हैं, दृढ कपाट होते हैं और कपाटों की मजबूती के लिए अर्गला होती है। अर्गला से द्वार सुदृढ़ हो जाता है और उसमें उपद्रवी लोग या शत्रु प्रवेश नहीं कर सकते । ब्रह्मचर्य वह अर्गला है जिसकी दृढता के कारण धर्म-नगर का चारित्ररूपी प्राकार ऐसा बन जाता है कि उसमें धर्मविरोधी तत्त्व-पाप का प्रवेश नहीं हो पाता।
इस प्रकार के अनेक दृष्टान्तों से ब्रह्मचर्य का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। पाठक सरलता से इसका आशय समझ सकते हैं।
मूल पाठ में ब्रह्मचर्य के लिए 'सया विसुद्ध' विशेषण का प्रयोग किया गया है। टीकाकार ने इसका अर्थ सदा अर्थात् 'कुमार आदि सभी अवस्थाओं में किया है । कुछ लोग कहते हैं कि
अपुत्रस्य गति स्ति, स्वर्गो नैव च नैव च । तस्मात्पुत्रमुखं दृष्ट्वा, पश्चाद्धर्मं चरिष्यसि ।।
१. अभयदेवटीका, पृ. १३२ (प्रागमोदय०)