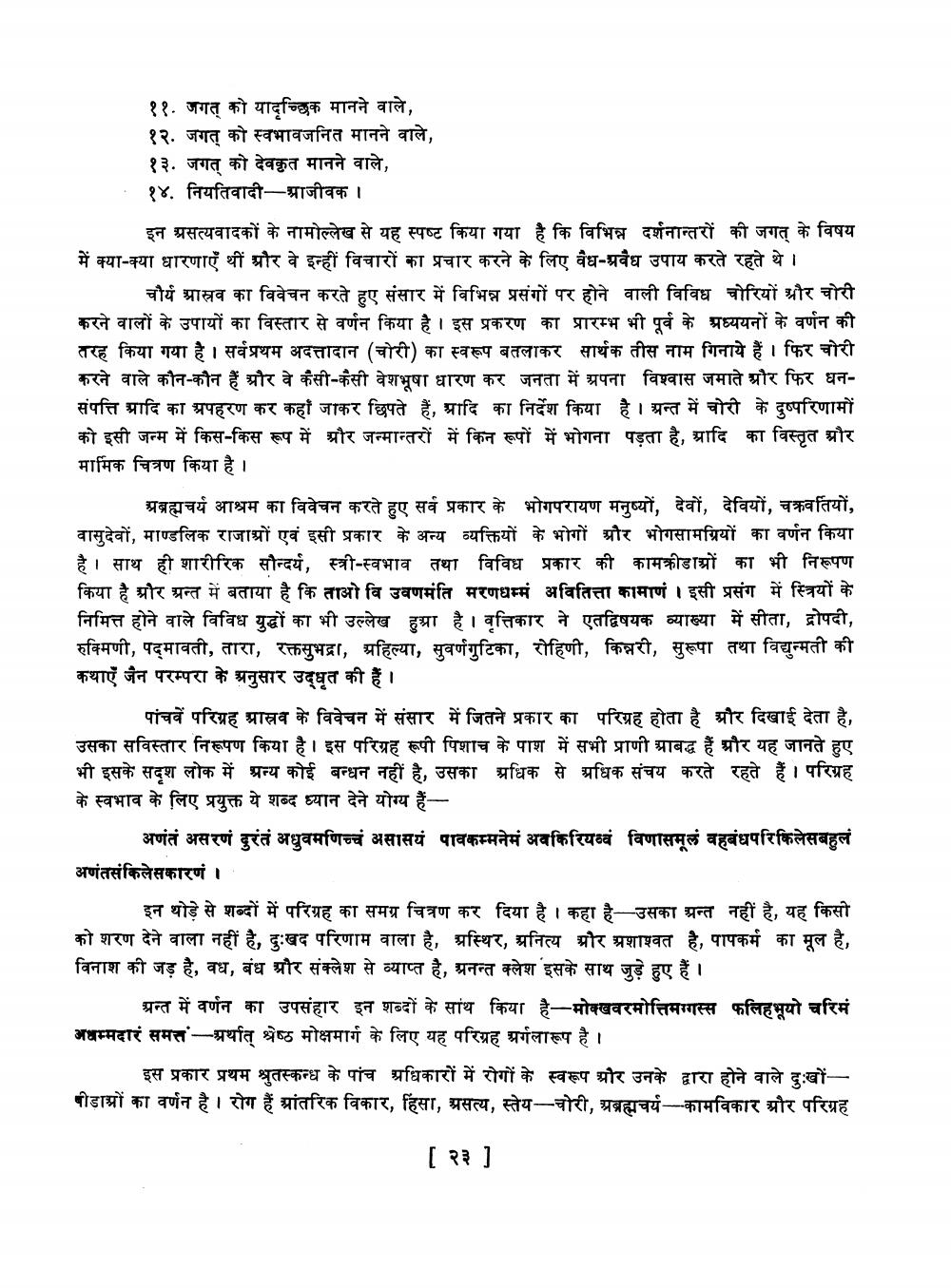________________
११. जगत् को यादृच्छिक मानने वाले, १२. जगत् को स्वभावजनित मानने वाले, १३. जगत् को देवकृत मानने वाले, १४. नियतिवादी-आजीवक ।
इन असत्यवादकों के नामोल्लेख से यह स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न दर्शनान्तरों की जगत् के विषय में क्या-क्या धारणाएँ थीं और वे इन्हीं विचारों का प्रचार करने के लिए वैध-अवैध उपाय करते रहते थे।
चौर्य आस्रव का विवेचन करते हए संसार में विभिन्न प्रसंगों पर होने वाली विविध चोरियों और चोरी करने वालों के उपायों का विस्तार से वर्णन किया है। इस प्रकरण का प्रारम्भ भी पूर्व के अध्ययनों के वर्णन की तरह किया गया है। सर्वप्रथम अदत्तादान (चोरी) का स्वरूप बतलाकर सार्थक तीस नाम गिनाये हैं। फिर चोरी करने वाले कौन-कौन हैं और वे कैसी-कैसी वेशभूषा धारण कर जनता में अपना विश्वास जमाते और फिर धनसंपत्ति आदि का अपहरण कर कहाँ जाकर छिपते हैं, आदि का निर्देश किया है। अन्त में चोरी के दुष्परिणामों को इसी जन्म में किस-किस रूप में और जन्मान्तरों में किन रूपों में भोगना पड़ता है, आदि का विस्तृत और मार्मिक चित्रण किया है।
अब्रह्मचर्य आश्रम का विवेचन करते हुए सर्व प्रकार के भोगपरायण मनुष्यों, देवों, देवियों, चक्रवर्तियों, वासुदेवों, माण्डलिक राजाओं एवं इसी प्रकार के अन्य व्यक्तियों के भोगों और भोगसामग्रियों का वर्णन किया है। साथ ही शारीरिक सौन्दर्य, स्त्री-स्वभाव तथा विविध प्रकार की कामक्रीडाओं का भी निरूपण किया है और अन्त में बताया है कि ताओ वि उवणमंति मरणधम्म अवितित्ता कामाणं । इसी प्रसंग में स्त्रियों के निमित्त होने वाले विविध युद्धों का भी उल्लेख हुआ है। वृत्तिकार ने एतद्विषयक व्याख्या में सीता, द्रोपदी, रुक्मिणी, पद्मावती, तारा, रक्तसुभद्रा, अहिल्या, सुवर्णगुटिका, रोहिणी, किन्नरी, सुरूपा तथा विद्युन्मती की कथाएँ जैन परम्परा के अनुसार उद्धृत की हैं।
पांचवें परिग्रह प्रास्रव के विवेचन में संसार में जितने प्रकार का परिग्रह होता है और दिखाई देता है, उसका सविस्तार निरूपण किया है। इस परिग्रह रूपी पिशाच के पाश में सभी प्राणी आबद्ध हैं और यह जानते हुए भी इसके सदश लोक में अन्य कोई बन्धन नहीं है, उसका अधिक से अधिक संचय करते रहते हैं। परिग्रह के स्वभाव के लिए प्रयुक्त ये शब्द ध्यान देने योग्य हैं
अणंतं असरणं दुरंतं अधुवमणिच्चं असासयं पावकम्मनेम अवकिरियव्वं विणासमूलं वहबंधपरिकिलेसबहुलं अणंतसंकिलेसकारणं ।
इन थोड़े से शब्दों में परिग्रह का समग्र चित्रण कर दिया है। कहा है-उसका अन्त नहीं है, यह किसी को शरण देने वाला नहीं है, दुःखद परिणाम वाला है, अस्थिर, अनित्य और अशाश्वत है, पापकर्म का मूल है, विनाश की जड़ है, वध, बंध और संक्लेश से व्याप्त है, अनन्त क्लेश इसके साथ जुड़े हुए हैं।
अन्त में वर्णन का उपसंहार इन शब्दों के साथ किया है-मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूयो चरिमं अधम्मदारं समत्त-अर्थात् श्रेष्ठ मोक्षमार्ग के लिए यह परिग्रह अर्गलारूप है।
इस प्रकार प्रथम श्रुतस्कन्ध के पांच अधिकारों में रोगों के स्वरूप और उनके द्वारा होने वाले दुःखोंपीड़ाओं का वर्णन है । रोग हैं आंतरिक विकार, हिंसा, असत्य, स्तेय-चोरी, अब्रह्मचर्य-कामविकार और परिग्रह
[२३ ]