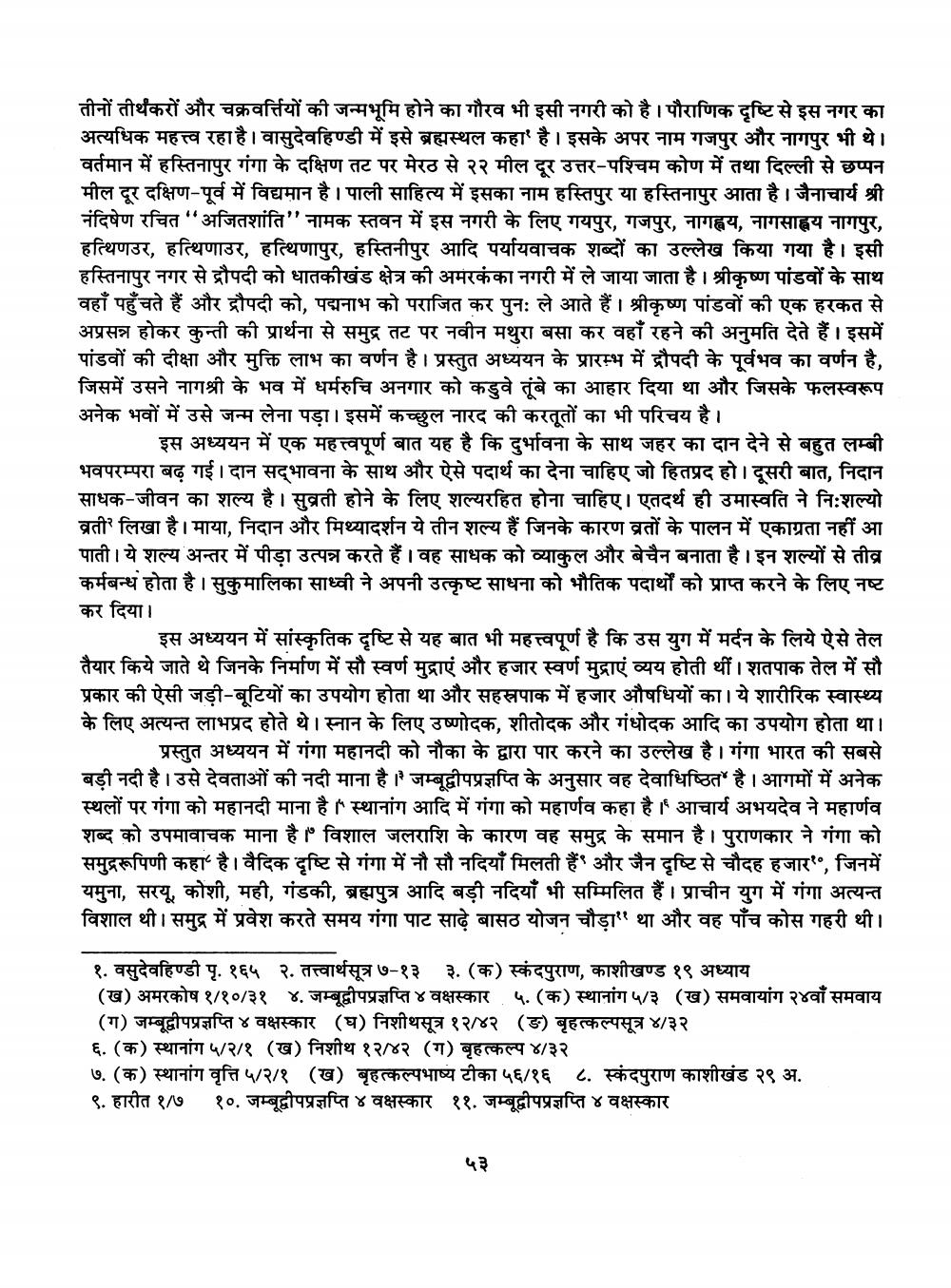________________
तीनों तीर्थंकरों और चक्रवर्तियों की जन्मभूमि होने का गौरव भी इसी नगरी को है। पौराणिक दृष्टि से इस नगर का अत्यधिक महत्त्व रहा है। वासुदेवहिण्डी में इसे ब्रह्मस्थल कहा है। इसके अपर नाम गजपुर और नागपुर भी थे। वर्तमान में हस्तिनापुर गंगा के दक्षिण तट पर मेरठ से २२ मील दूर उत्तर-पश्चिम कोण में तथा दिल्ली से छप्पन मील दूर दक्षिण-पूर्व में विद्यमान है। पाली साहित्य में इसका नाम हस्तिपुर या हस्तिनापुर आता है। जैनाचार्य श्री नंदिषेण रचित "अजितशांति" नामक स्तवन में इस नगरी के लिए गयपुर, गजपुर, नागह्वय, नागसाह्वय नागपुर, हत्थिणउर, हत्थिणाउर, हत्थिणापुर, हस्तिनीपुर आदि पर्यायवाचक शब्दों का उल्लेख किया गया है। इसी हस्तिनापुर नगर से द्रौपदी को धातकीखंड क्षेत्र की अमरकंका नगरी में ले जाया जाता है। श्रीकृष्ण पांडवों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और द्रौपदी को, पद्मनाभ को पराजित कर पुनः ले आते हैं। श्रीकृष्ण पांडवों की एक हरकत से अप्रसन्न होकर कुन्ती की प्रार्थना से समुद्र तट पर नवीन मथुरा बसा कर वहाँ रहने की अनुमति देते हैं। इसमें पांडवों की दीक्षा और मुक्ति लाभ का वर्णन है। प्रस्तुत अध्ययन के प्रारम्भ में द्रौपदी के पूर्वभव का वर्णन है, जिसमें उसने नागश्री के भव में धर्मरुचि अनगार को कडुवे तूंबे का आहार दिया था और जिसके फलस्वरूप अनेक भवों में उसे जन्म लेना पड़ा। इसमें कच्छुल नारद की करतूतों का भी परिचय है।
इस अध्ययन में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दुर्भावना के साथ जहर का दान देने से बहुत लम्बी भवपरम्परा बढ़ गई । दान सद्भावना के साथ और ऐसे पदार्थ का देना चाहिए जो हितप्रद हो। दूसरी बात, निदान साधक-जीवन का शल्य है। सुव्रती होने के लिए शल्यरहित होना चाहिए। एतदर्थ ही उमास्वति ने निःशल्यो व्रती लिखा है। माया, निदान और मिथ्यादर्शन ये तीन शल्य हैं जिनके कारण व्रतों के पालन में एकाग्रता नहीं आ पाती। ये शल्य अन्तर में पीड़ा उत्पन्न करते हैं। वह साधक को व्याकुल और बेचैन बनाता है। इन शल्यों से तीव्र कर्मबन्ध होता है । सुकुमालिका साध्वी ने अपनी उत्कृष्ट साधना को भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए नष्ट कर दिया।
___इस अध्ययन में सांस्कृतिक दृष्टि से यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि उस युग में मर्दन के लिये ऐसे तेल तैयार किये जाते थे जिनके निर्माण में सौ स्वर्ण मुद्राएं और हजार स्वर्ण मुद्राएं व्यय होती थीं। शतपाक तेल में सौ प्रकार की ऐसी जड़ी-बूटियों का उपयोग होता था और सहस्रपाक में हजार औषधियों का। ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त लाभप्रद होते थे। स्नान के लिए उष्णोदक, शीतोदक और गंधोदक आदि का उपयोग होता था।
प्रस्तुत अध्ययन में गंगा महानदी को नौका के द्वारा पार करने का उल्लेख है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है । उसे देवताओं की नदी माना है। जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति के अनुसार वह देवाधिष्ठित है। आगमों में अनेक स्थलों पर गंगा को महानदी माना है। स्थानांग आदि में गंगा को महार्णव कहा है। आचार्य अभयदेव ने महार्णव शब्द को उपमावाचक माना है। विशाल जलराशि के कारण वह समुद्र के समान है। पुराणकार ने गंगा को समुद्ररूपिणी कहा है। वैदिक दृष्टि से गंगा में नौ सौ नदियाँ मिलती हैं और जैन दृष्टि से चौदह हजार, जिनमें यमुना, सरयू, कोशी, मही, गंडकी, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियाँ भी सम्मिलित हैं। प्राचीन युग में गंगा अत्यन्त विशाल थी। समुद्र में प्रवेश करते समय गंगा पाट साढ़े बासठ योजन चौड़ा था और वह पाँच कोस गहरी थी।
१. वसुदेवहिण्डी पृ. १६५ २. तत्त्वार्थसूत्र ७-१३ ३. (क) स्कंदपुराण, काशीखण्ड १९ अध्याय (ख) अमरकोष १/१०/३१ ४. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ४ वक्षस्कार ५. (क) स्थानांग ५/३ (ख) समवायांग २४वा समवाय (ग) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ४ वक्षस्कार (घ) निशीथसूत्र १२/४२ (ङ) बृहत्कल्पसूत्र ४/३२ ६. (क) स्थानांग ५/२/१ (ख) निशीथ १२/४२ (ग) बृहत्कल्प ४/३२ ७. (क) स्थानांग वृत्ति ५/२/१ (ख) बृहत्कल्पभाष्य टीका ५६/१६ ८. स्कंदपुराण काशीखंड २९ अ. ९. हारीत १/७ १०. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ४ वक्षस्कार ११. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ४ वक्षस्कार