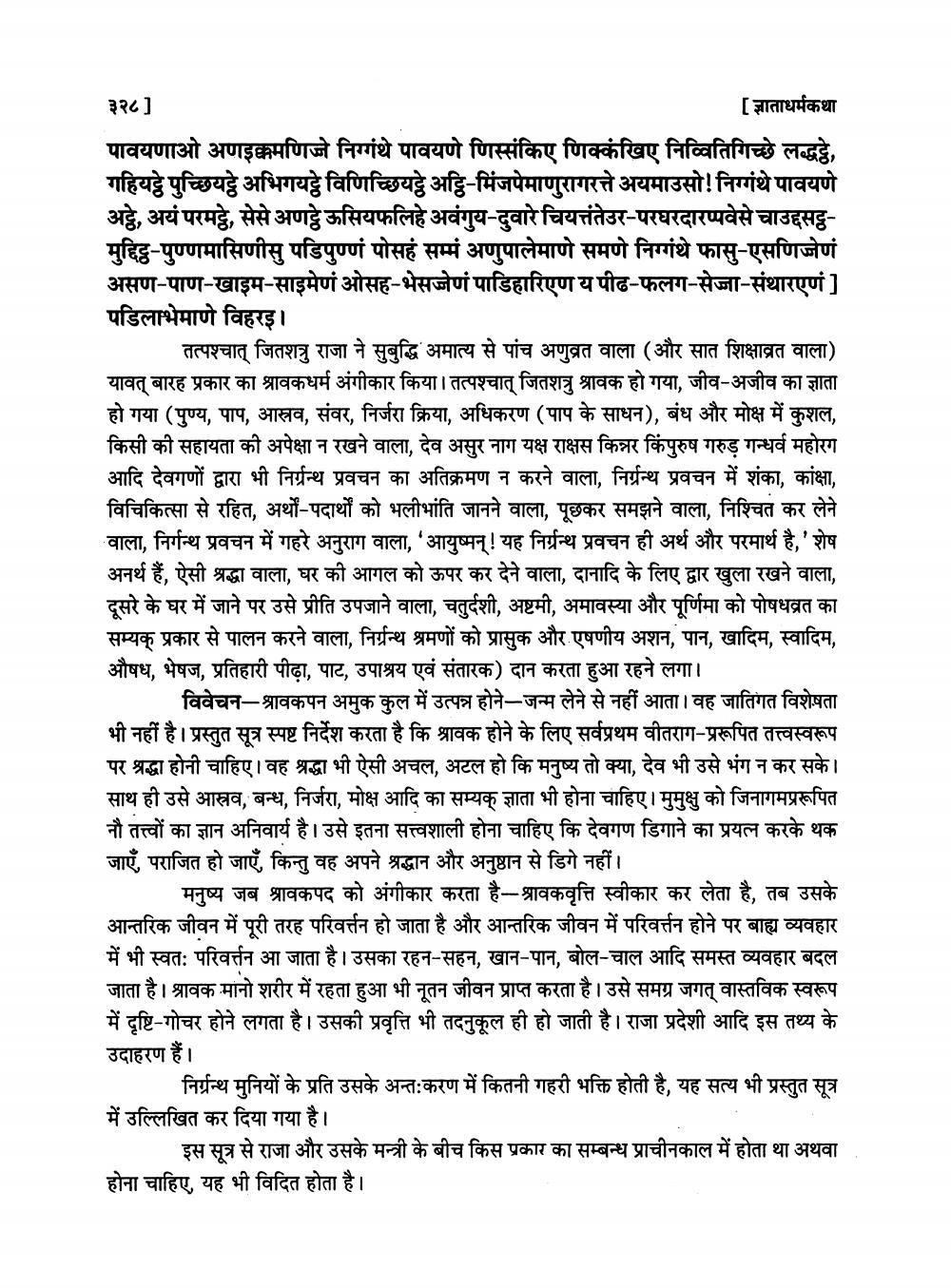________________
३२८]
[ज्ञाताधर्मकथा
पावयणाओ अणइक्कमणिज्जे निग्गंथे पावयणे णिस्संकिए णिक्कंखिए निव्वितिगिच्छे लद्धद्वे, गहियढे पुच्छियढे अभिगयढे विणिच्छियढे अट्ठि-मिंजपेमाणुरागरत्ते अयमाउसो! निग्गंथे पावयणे अटे, अयं परमटे, सेसे अणढेऊसियफलिहे अवंगुय-दुवारे चियत्तंतेउर-परघरदारप्पवेसे चाउद्दसट्ठमुट्ठि-पुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणे समणे निग्गंथे फासु-एसणिज्जेणं असण-पाण-खाइम-साइमेणं ओसह-भेसजेणं पाडिहारिएण य पीढ-फलग-सेजा-संथारएणं] पडिलाभेमाणे विहरइ।
तत्पश्चात् जितशत्रु राजा ने सुबुद्धि अमात्य से पांच अणुव्रत वाला (और सात शिक्षाव्रत वाला) यावत् बारह प्रकार का श्रावकधर्म अंगीकार किया। तत्पश्चात् जितशत्रु श्रावक हो गया, जीव-अजीव का ज्ञाता हो गया (पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा क्रिया, अधिकरण (पाप के साधन), बंध और मोक्ष में कुशल, किसी की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला, देव असुर नाग यक्ष राक्षस किन्नर किंपुरुष गरुड़ गन्धर्व महोरग आदि देवगणों द्वारा भी निर्ग्रन्थ प्रवचन का अतिक्रमण न करने वाला, निर्ग्रन्थ प्रवचन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा से रहित, अर्थों-पदार्थों को भलीभांति जानने वाला, पूछकर समझने वाला, निश्चित कर लेने वाला, निर्गन्थ प्रवचन में गहरे अनुराग वाला, 'आयुष्मन्! यह निर्ग्रन्थ प्रवचन ही अर्थ और परमार्थ है, ' शेष अनर्थ हैं, ऐसी श्रद्धा वाला, घर की आगल को ऊपर कर देने वाला, दानादि के लिए द्वार खुला रखने वाला, दूसरे के घर में जाने पर उसे प्रीति उपजाने वाला, चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा को पोषधव्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने वाला, निर्ग्रन्थ श्रमणों को प्रासुक और एषणीय अशन, पान, खादिम, स्वादिम, औषध, भेषज, प्रतिहारी पीढ़ा, पाट, उपाश्रय एवं संतारक) दान करता हुआ रहने लगा।
विवेचन-श्रावकपन अमुक कुल में उत्पन्न होने-जन्म लेने से नहीं आता। वह जातिगत विशेषता भी नहीं है। प्रस्तुत सूत्र स्पष्ट निर्देश करता है कि श्रावक होने के लिए सर्वप्रथम वीतराग-प्ररूपित तत्त्वस्वरूप पर श्रद्धा होनी चाहिए। वह श्रद्धा भी ऐसी अचल, अटल हो कि मनुष्य तो क्या, देव भी उसे भंग न कर सके। साथ ही उसे आस्रव, बन्ध, निर्जरा, मोक्ष आदि का सम्यक् ज्ञाता भी होना चाहिए। मुमुक्षु को जिनागमप्ररूपित नौ तत्त्वों का ज्ञान अनिवार्य है। उसे इतना सत्त्वशाली होना चाहिए कि देवगण डिगाने का प्रयत्न करके थक जाएँ, पराजित हो जाएँ, किन्तु वह अपने श्रद्धान और अनुष्ठान से डिगे नहीं।
मनुष्य जब श्रावकपद को अंगीकार करता है-श्रावकवृत्ति स्वीकार कर लेता है, तब उसके आन्तरिक जीवन में पूरी तरह परिवर्तन हो जाता है और आन्तरिक जीवन में परिवर्तन होने पर बाह्य व्यवहार में भी स्वतः परिवर्तन आ जाता है। उसका रहन-सहन, खान-पान, बोल-चाल आदि समस्त व्यवहार बदल जाता है। श्रावक मानो शरीर में रहता हुआ भी नूतन जीवन प्राप्त करता है। उसे समग्र जगत् वास्तविक स्वरूप में दृष्टि-गोचर होने लगता है। उसकी प्रवृत्ति भी तदनुकूल ही हो जाती है। राजा प्रदेशी आदि इस तथ्य के उदाहरण हैं।
निर्ग्रन्थ मुनियों के प्रति उसके अन्तःकरण में कितनी गहरी भक्ति होती है, यह सत्य भी प्रस्तुत सूत्र में उल्लिखित कर दिया गया है।
इस सूत्र से राजा और उसके मन्त्री के बीच किस प्रकार का सम्बन्ध प्राचीनकाल में होता था अथवा होना चाहिए, यह भी विदित होता है।