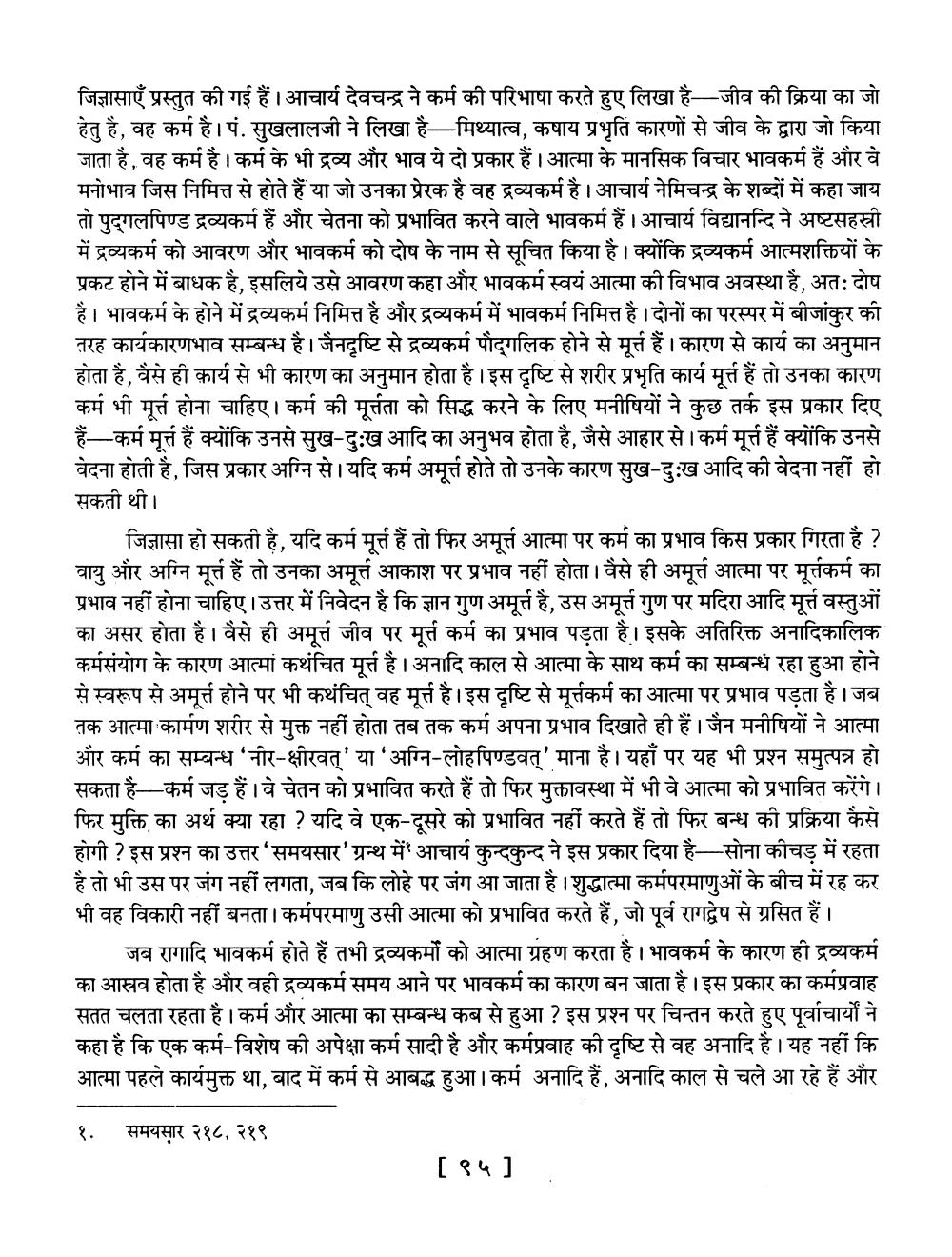________________
जिज्ञासाएँ प्रस्तुत की गई हैं। आचार्य देवचन्द्र ने कर्म की परिभाषा करते हुए लिखा है— जीव की क्रिया का जो हेतु है, वह कर्म है। पं. सुखलालजी ने लिखा है— मिथ्यात्व, कषाय प्रभृति कारणों से जीव के द्वारा जो किया जाता है, वह कर्म है। कर्म के भी द्रव्य और भाव ये दो प्रकार हैं। आत्मा के मानसिक विचार भावकर्म हैं और वे मनोभाव जिस निमित्त से होते हैं या जो उनका प्रेरक है वह द्रव्यकर्म है। आचार्य नेमिचन्द्र के शब्दों में कहा जाय तो पुद्गलपिण्ड द्रव्यकर्म हैं और चेतना को प्रभावित करने वाले भावकर्म हैं। आचार्य विद्यानन्दि ने अष्टसहस्त्री में द्रव्यकर्म को आवरण और भावकर्म को दोष के नाम से सूचित किया है। क्योंकि द्रव्यकर्म आत्मशक्तियों के प्रकट होने में बाधक है, इसलिये उसे आवरण कहा और भावकर्म स्वयं आत्मा की विभाव अवस्था है, अत: दोष हैं। भावकर्म के होने में द्रव्यकर्म निमित्त हैं और द्रव्यकर्म में भावकर्म निमित्त है। दोनों का परस्पर में बीजांकुर की तरह कार्यकारणभाव सम्बन्ध है। जैनदृष्टि से द्रव्यकर्म पौद्गलिक होने से मूर्त हैं । कारण से कार्य का अनुमान होता है, वैसे ही कार्य से भी कारण का अनुमान होता है । इस दृष्टि से शरीर प्रभृति कार्य मूर्त्त हैं तो उनका कारण कर्म भी मूर्त्त होना चाहिए। कर्म की मूर्तता को सिद्ध करने के लिए मनीषियों ने कुछ तर्क इस प्रकार दिए हैं— कर्म मूर्त हैं क्योंकि उनसे सुख-दुःख आदि का अनुभव होता है, जैसे आहार से । कर्म मूर्त्त हैं क्योंकि उनसे वेदना होती हैं, जिस प्रकार अग्नि से । यदि कर्म अमूर्त्त होते तो उनके कारण सुख-दुःख आदि की वेदना नहीं हो सकती थी ।
T
जिज्ञासा हो सकती है, यदि कर्म मूर्त हैं तो फिर अमूर्त आत्मा पर कर्म का प्रभाव किस प्रकार गिरता है ? वायु और अग्नि मूर्त हैं उनका अमूर्त आकाश पर प्रभाव नहीं होता। वैसे ही अमूर्त्त आत्मा पर मूर्त्तकर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए । उत्तर में निवेदन है कि ज्ञान गुण अमूर्त है, उस अमूर्त गुण पर मदिरा आदि मूर्त वस्तुओं का असर होता है। वैसे ही अमूर्त जीव पर मूर्त कर्म का प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनादिकालिक कर्मसंयोग के कारण आत्मा कथंचित मूर्त्त है । अनादि काल से आत्मा के साथ कर्म का सम्बन्ध रहा हुआ होने से स्वरूप से अमूर्त होने पर भी कथंचित् वह मूर्त्त है । इस दृष्टि से मूर्त्तकर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जब तक आत्मा कार्मण शरीर से मुक्त नहीं होता तब तक कर्म अपना प्रभाव दिखाते ही हैं। जैन मनीषियों ने आत्मा और कर्म का सम्बन्ध ‘नीर-क्षीरवत्' या 'अग्नि- लोहपिण्डवत्' माना है। यहाँ पर यह भी प्रश्न समुत्पन्न हो सकता है—कर्म जड़ हैं। वे चेतन को प्रभावित करते हैं तो फिर मुक्तावस्था में भी वे आत्मा को प्रभावित करेंगे। फिर मुक्ति का अर्थ क्या रहा ? यदि वे एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं तो फिर बन्ध की प्रक्रिया कैसे होगी ? इस प्रश्न का उत्तर 'समयसार' ग्रन्थ में' आचार्य कुन्दकुन्द ने इस प्रकार दिया है— सोना कीचड़ में रहता है तो भी उस पर जंग नहीं लगता, जब कि लोहे पर जंग आ जाता है। शुद्धात्मा कर्मपरमाणुओं के बीच में रह कर भी वह विकारी नहीं बनता । कर्मपरमाणु उसी आत्मा को प्रभावित करते हैं, जो पूर्व रागद्वेष से ग्रसित हैं ।
जब रागादि भावकर्म होते हैं तभी द्रव्यकर्मों को आत्मा ग्रहण करता है । भावकर्म के कारण ही द्रव्यकर्म का आस्रव होता है और वही द्रव्यकर्म समय आने पर भावकर्म का कारण बन जाता है। इस प्रकार का कर्मप्रवाह सतत चलता रहता है । कर्म और आत्मा का सम्बन्ध कब से हुआ ? इस प्रश्न पर चिन्तन करते हुए पूर्वाचार्यों ने कहा है कि एक कर्म-विशेष की अपेक्षा कर्म सादी है और कर्मप्रवाह की दृष्टि से वह अनादि है। यह नहीं कि आत्मा पहले कार्यमुक्त था, बाद में कर्म से आबद्ध हुआ । कर्म अनादि हैं, अनादि काल से चले आ रहे हैं और
समयसार २१८, २१९
१.
[ ९५ ]