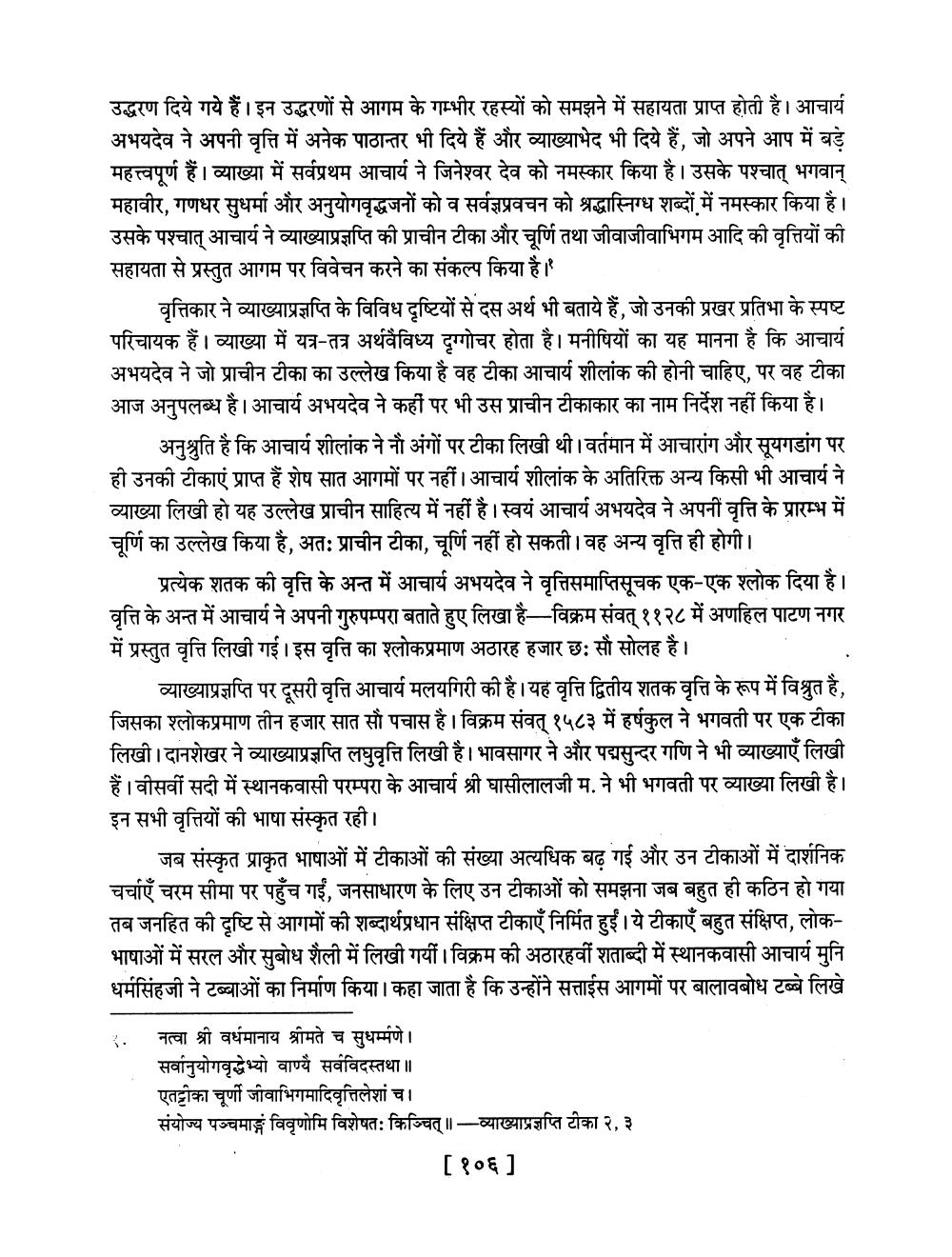________________
उद्धरण दिये गये हैं । इन उद्धरणों से आगम के गम्भीर रहस्यों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। आचार्य अभयदेव ने अपनी वृत्ति में अनेक पाठान्तर भी दिये हैं और व्याख्याभेद भी दिये हैं, जो अपने आप में बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। व्याख्या में सर्वप्रथम आचार्य ने जिनेश्वर देव को नमस्कार किया है। उसके पश्चात् भगवान् महावीर, गणधर सुधर्मा और अनुयोगवृद्धजनों को व सर्वज्ञप्रवचन को श्रद्धास्निग्ध शब्दों में नमस्कार किया है। उसके पश्चात् आचार्य ने व्याख्याप्रज्ञप्ति की प्राचीन टीका और चूर्णि तथा जीवाजीवाभिगम आदि की वृत्तियों की सहायता से प्रस्तुत आगम पर विवेचन करने का संकल्प किया है।
वृत्तिकार ने व्याख्याप्रज्ञप्ति के विविध दृष्टियों से दस अर्थ भी बताये हैं, जो उनकी प्रखर प्रतिभा के स्पष्ट परिचायक हैं। व्याख्या में यत्र-तत्र अर्थवैविध्य दृग्गोचर होता है। मनीषियों का यह मानना है कि आचार्य अभयदेव ने जो प्राचीन टीका का उल्लेख किया है वह टीका आचार्य शीलांक की होनी चाहिए, पर वह टीका आज अनुपलब्ध है। आचार्य अभयदेव ने कहीं पर भी उस प्राचीन टीकाकार का नाम निर्देश नहीं किया है।
अनुश्रुति है कि आचार्य शीलांक ने नौ अंगों पर टीका लिखी थी। वर्तमान में आचारांग और सूयगडांग पर ही उनकी टीकाएं प्राप्त हैं शेष सात आगमों पर नहीं । आचार्य शीलांक के अतिरिक्त अन्य किसी भी आचार्य ने व्याख्या लिखी हो यह उल्लेख प्राचीन साहित्य में नहीं है। स्वयं आचार्य अभयदेव ने अपनीं वृत्ति के प्रारम्भ में चूर्णि का उल्लेख किया है, अत: प्राचीन टीका, चूर्णि नहीं हो सकती। वह अन्य वृत्ति ही होगी ।
प्रत्येक शतक की वृत्ति के अन्त में आचार्य अभयदेव ने वृत्तिसमाप्तिसूचक एक-एक श्लोक दिया है। वृत्ति के अन्त में आचार्य ने अपनी गुरुपम्परा बताते हुए लिखा है — विक्रम संवत् ११२८ में अणहिल पाटण नगर प्रस्तुत वृत्ति लिखी गई। इस वृत्ति का श्लोकप्रमाण अठारह हजार छः सौ सोलह है ।
व्याख्याप्रज्ञप्ति पर दूसरी वृत्ति आचार्य मलयगिरी की है। यह वृत्ति द्वितीय शतक वृत्ति के रूप में विश्रुत है, जिसका श्लोकप्रमाण तीन हजार सात सौ पचास है। विक्रम संवत् १५८३ में हर्षकुल ने भगवती पर एक टीका लिखी । दानशेखर ने व्याख्याप्रज्ञप्ति लघुवृत्ति लिखी है। भावसागर ने और पद्मसुन्दर गणि ने भी व्याख्याएँ लिखी हैं। वीसवीं सदी में स्थानकवासी परम्परा के आचार्य श्री घासीलालजी म. ने भी भगवती पर व्याख्या लिखी है। इन सभी वृत्तियों की भाषा संस्कृत रही।
जब संस्कृत प्राकृत भाषाओं में टीकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई और उन टीकाओं में दार्शनिक चर्चाएँ चरम सीमा पर पहुँच गईं, जनसाधारण के लिए उन टीकाओं को समझना जब बहुत ही कठिन हो गया तब जनहित की दृष्टि से आगमों की शब्दार्थप्रधान संक्षिप्त टीकाएँ निर्मित हुईं। ये टीकाएँ बहुत संक्षिप्त, लोकभाषाओं में सरल और सुबोध शैली में लिखी गयीं। विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में स्थानकवासी आचार्य मुनि धर्मसिंहजी ने टब्बाओं का निर्माण किया। कहा जाता है कि उन्होंने सत्ताईस आगमों पर बालावबोध टब्बे लिखे
3.
नत्वा श्री वर्धमानाय श्रीमते च सुधर्म्मणे । सर्वानुयोगवृद्धेभ्यो वाण्यै सर्वविदस्तथा ॥ एतट्टीका चूर्णी जीवाभिगमादिवृत्तिलेशां च ।
संयोज्य पञ्चमाङ्गं विवृणोमि विशेषतः किञ्चित् ॥ - व्याख्याप्रज्ञप्ति टीका २, ३
[ १०६ ]