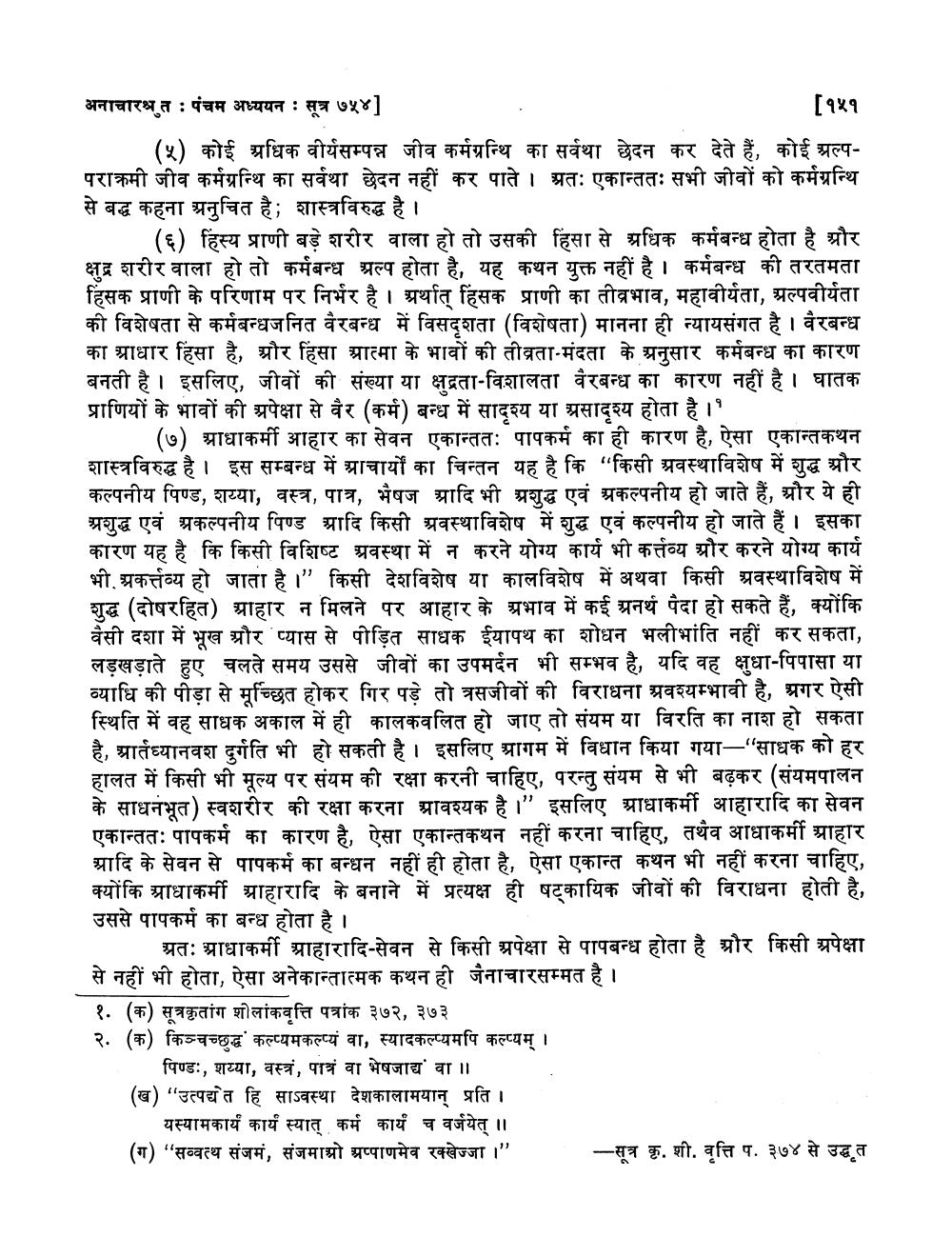________________
अनाचारभु त : पंचम अध्ययन : सूत्र ७५४]
[१५१ (५) कोई अधिक वीर्यसम्पन्न जीव कर्मग्रन्थि का सर्वथा छेदन कर देते हैं, कोई अल्पपराक्रमी जीव कर्मग्रन्थि का सर्वथा छेदन नहीं कर पाते। अतः एकान्ततः सभी जीवों को कर्मग्रन्थि से बद्ध कहना अनुचित है; शास्त्रविरुद्ध है।
(६) हिंस्य प्राणी बड़े शरीर वाला हो तो उसकी हिंसा से अधिक कर्मबन्ध होता है और क्षुद्र शरीर वाला हो तो कर्मबन्ध अल्प होता है, यह कथन युक्त नहीं है। कर्मबन्ध की तरतमता हिंसक प्राणी के परिणाम पर निर्भर है । अर्थात् हिंसक प्राणी का तीव्रभाव, महावीर्यता, अल्पवीर्यता की विशेषता से कर्मबन्धजनित वैरबन्ध में विसदृशता (विशेषता) मानना ही न्यायसंगत है । वैरबन्ध का आधार हिंसा है, और हिंसा आत्मा के भावों की तीव्रता-मंदता के अनुसार कर्मबन्ध का कारण बनती है। इसलिए, जीवों की संख्या या क्षुद्रता-विशालता वैरबन्ध का कारण नहीं है। घातक प्राणियों के भावों की अपेक्षा से वैर (कर्म) बन्ध में सादृश्य या असादृश्य होता है।'
(७) प्राधाकर्मी आहार का सेवन एकान्ततः पापकर्म का ही कारण है, ऐसा एकान्तकथन शास्त्रविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में प्राचार्यों का चिन्तन यह है कि "किसी अवस्थाविशेष में शुद्ध और कल्पनीय पिण्ड. शय्या. वस्त्र, पात्र. भैषज आदि भी प्रशद्ध एवं अकल्पनीय हो जाते हैं, और ये ही अशुद्ध एवं अकल्पनीय पिण्ड आदि किसी अवस्थाविशेष में शुद्ध एवं कल्पनीय हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि किसी विशिष्ट अवस्था में न करने योग्य कार्य भी कर्तव्य और करने योग्य कार्य भी, अकर्त्तव्य हो जाता है।" किसी देशविशेष या कालविशेष में अथवा किसी अवस्थाविशेष में शुद्ध (दोषरहित) आहार न मिलने पर आहार के अभाव में कई अनर्थ पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वैसी दशा में भूख और प्यास से पीड़ित साधक ईयापथ का शोधन भलीभांति नहीं कर सकता, लड़खड़ाते हुए चलते समय उससे जीवों का उपमर्दन भी सम्भव है, यदि वह क्षुधा-पिपासा या व्याधि की पीड़ा से मूच्छित होकर गिर पड़े तो त्रसजीवों की विराधना अवश्यम्भावी है, अगर ऐसी स्थिति में वह साधक अकाल में ही कालकवलित हो जाए तो संयम या विरति का नाश हो सकता है, आर्तध्यानवश दुर्गति भी हो सकती है। इसलिए आगम में विधान किया गया—साधक को हर हालत में किसी भी मूल्य पर संयम की रक्षा करनी चाहिए, परन्तु संयम से भी बढ़कर (संयमपालन के साधनभूत) स्वशरीर की रक्षा करना आवश्यक है।" इसलिए प्राधाकर्मी आहारादि का सेवन एकान्ततः पापकर्म का कारण है, ऐसा एकान्तकथन नहीं करना चाहिए, तथैव आधाकर्मी आहार आदि के सेवन से पापकर्म का बन्धन नहीं ही होता है, ऐसा एकान्त कथन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधाकर्मी आहारादि के बनाने में प्रत्यक्ष ही षट्कायिक जीवों की विराधना होती है, उससे पापकर्म का बन्ध होता है।
अतः प्राधाकर्मी आहारादि-सेवन से किसी अपेक्षा से पापबन्ध होता है और किसी अपेक्षा से नहीं भी होता, ऐसा अनेकान्तात्मक कथन ही जैनाचारसम्मत है । १. (क) सूत्रकृतांग शीलांकत्ति पत्रांक ३७२, ३७३ २. (क) किञ्चच्छुद्ध कल्प्यमकल्प्यं वा, स्यादकल्प्यमपि कल्प्यम् ।
पिण्डः, शय्या, वस्त्र, पात्र वा भेषजाद्य वा ॥ ) "उत्पद्यत हि साऽवस्था देशकालामयान् प्रति ।
यस्यामकार्य कार्यं स्यात् कर्म कायं च वर्जयेत् ।। (ग) “सव्वत्थ संजमं, संजमामो अप्पाणमेव रक्खेज्जा।"
-सूत्र कृ. शी. वृत्ति प. ३७४ से उद्ध त