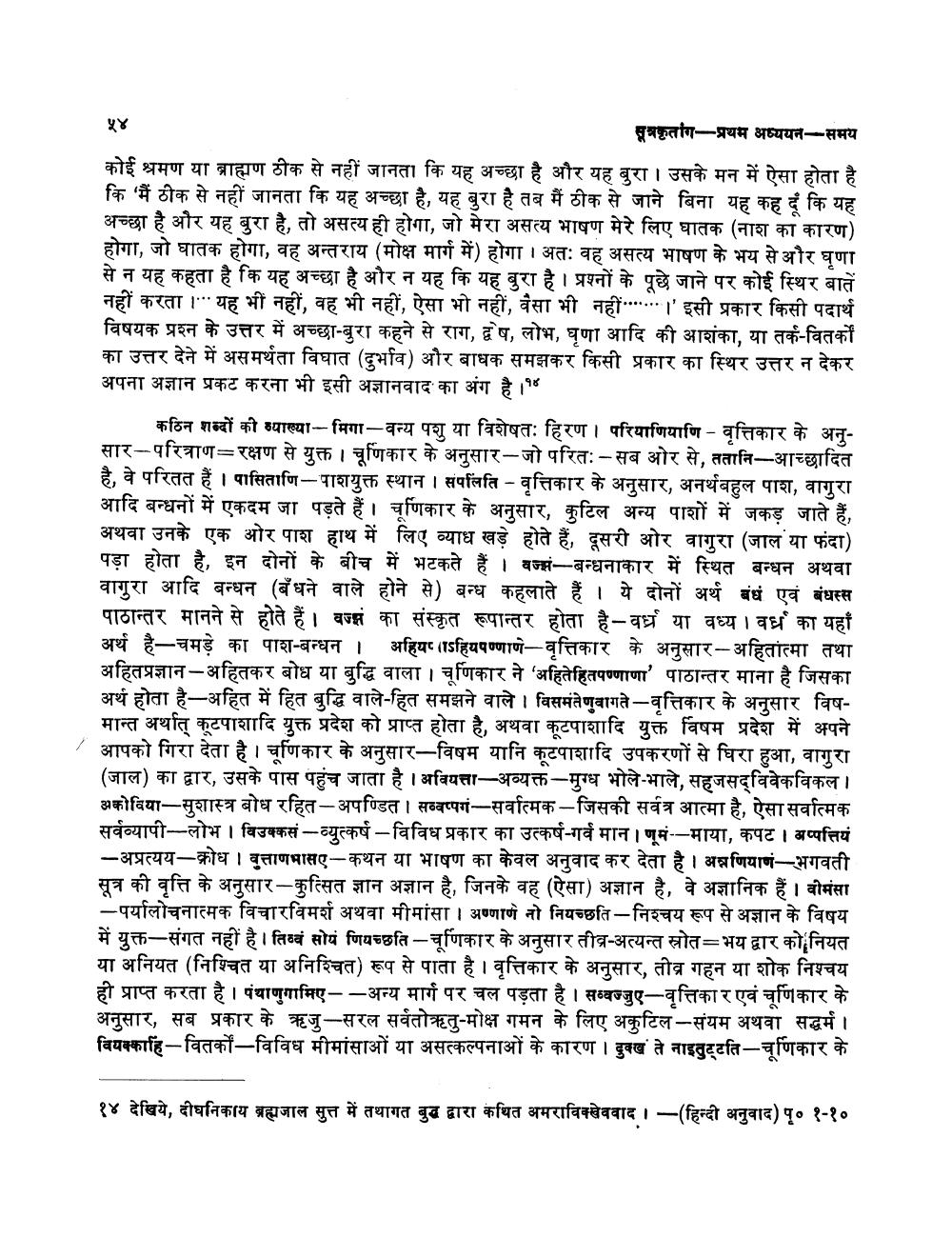________________
५४
सूत्रकृतांग-प्रथम अध्ययन-समय
कोई श्रमण या ब्राह्मण ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा। उसके मन में ऐसा होता है कि 'मैं ठीक से नहीं जानता कि यह अच्छा है, यह बुरा है तब मैं ठीक से जाने बिना यह कह दूं कि यह अच्छा है और यह बुरा है, तो असत्य ही होगा, जो मेरा असत्य भाषण मेरे लिए घातक (नाश का कारण) होगा, जो घातक होगा, वह अन्तराय (मोक्ष मार्ग में) होगा। अतः वह असत्य भाषण के भय से और घृणा से न यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कि यह बुरा है। प्रश्नों के पूछे जाने पर कोई स्थिर बातें नहीं करता। यह भी नहीं, वह भी नहीं, ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं......।' इसी प्रकार किसी पदार्थ विषयक प्रश्न के उत्तर में अच्छा-बुरा कहने से राग, द्वेष, लोभ, घृणा आदि की आशंका, या तर्क-वितर्कों का उत्तर देने में असमर्थता विघात (दुर्भाव) और बाधक समझकर किसी प्रकार का स्थिर उत्तर न देकर अपना अज्ञान प्रकट करना भी इसी अज्ञानवाद का अंग है।१४
कठिन शब्दों की व्याख्या-मिगा-वन्य पशू या विशेषतः हिरण। परियाणियाणि - वृत्तिकार के अनूसार-परित्राणरक्षण से युक्त । चूर्णिकार के अनुसार-जो परितः-सब ओर से, ततानि-आच्छादित है, वे परितत हैं । पासिताणि-पाशयुक्त स्थान । संपलिति - वृत्तिकार के अनुसार, अनर्थबहुल पाश, वागुरा आदि बन्धनों में एकदम जा पडते हैं। चर्णिकार के अनसार, कटिल अन्य पाशों में जकड जाते हैं. अथवा उनके एक ओर पाश हाथ में लिए व्याध खड़े होते हैं, दूसरी ओर वागुरा (जाल या फंदा) पड़ा होता है, इन दोनों के बीच में भटकते हैं । बझ-बन्धनाकार में स्थित बन्धन अथवा वागुरा आदि बन्धन (बँधने वाले होने से) बन्ध कहलाते हैं । ये दोनों अर्थ बंधं एवं बंधस्स पाठान्तर मानने से होते हैं। वज्झं का संस्कृत रूपान्तर होता है- वर्ध या वध्य । वधं का यहाँ अर्थ है-चमड़े का पाश-बन्धन । अहिया (ऽहियपण्णाणे-वृत्तिकार के अनुसार-अहितात्मा तथा अहितप्रज्ञान-अहितकर बोध या बुद्धि वाला। चूर्णिकार ने 'अहितेहितपण्णाणा' पाठान्तर माना है जिसका अर्थ होता है-अहित में हित बुद्धि वाले-हित समझने वाले। विसमतेणवागते-वत्तिकार के अनुसार विषमान्त अर्थात् कूटपाशादि युक्त प्रदेश को प्राप्त होता है, अथवा कूटपाशादि युक्त विषम प्रदेश में अपने आपको गिरा देता है । चूर्णिकार के अनुसार-विषम यानि कूटपाशादि उपकरणों से घिरा हुआ, वागुरा (जाल) का द्वार, उसके पास पहुंच जाता है । अवियत्ता-अव्यक्त-मुग्ध भोले-भाले, सहजसद्विवेकविकल। अकोविया-सुशास्त्र बोध रहित-अपण्डित । सव्वप्पगं-सर्वात्मक-जिसकी सर्वत्र आत्मा है, ऐसा सर्वात्मक सर्वव्यापी-लोभ । विउक्कसं-व्युत्कर्ष-विविध प्रकार का उत्कर्ष-गर्व मान। णूम-माया, कपट । अप्पत्तियं -अप्रत्यय-क्रोध । वुत्ताणभासए-कथन या भाषण का केवल अनुवाद कर देता है। अन्नणियाणं-भगवती सूत्र की वृत्ति के अनुसार-कुत्सित ज्ञान अज्ञान है, जिनके वह (ऐसा) अज्ञान है, वे अज्ञानिक हैं । वोमंसा -पर्यालोचनात्मक विचारविमर्श अथवा मीमांसा । अण्णाणे नो नियच्छति-निश्चय रूप से अज्ञान के विषय में युक्त-संगत नहीं है। तिव्वं सोयं णियच्छति-चूर्णिकार के अनुसार तीव्र-अत्यन्त स्रोत=भय द्वार को नियत या अनियत (निश्चित या अनिश्चित रूप से पाता है । वृत्तिकार के अनुसार, तीव्र गहन या शोक निश्चय ही प्राप्त करता है । पंथाणुगामिए --अन्य मार्ग पर चल पड़ता है । सम्वज्जुए-वृत्तिका र एवं चूर्णिकार के अनुसार, सब प्रकार के ऋजु-सरल सर्वतोऋतु-मोक्ष गमन के लिए अकुटिल-संयम अथवा सद्धर्म । वियक्काहि-वितर्कों-विविध मीमांसाओं या असत्कल्पनाओं के कारण । दुक्ख ते नाइतुट्टति-चूर्णिकार के
१४ देखिये, दीघनिकाय ब्रह्मजाल सुत्त में तथागत बुद्ध द्वारा कथित अमराविक्खेववाद। -(हिन्दी अनुवाद) पृ० १-१०