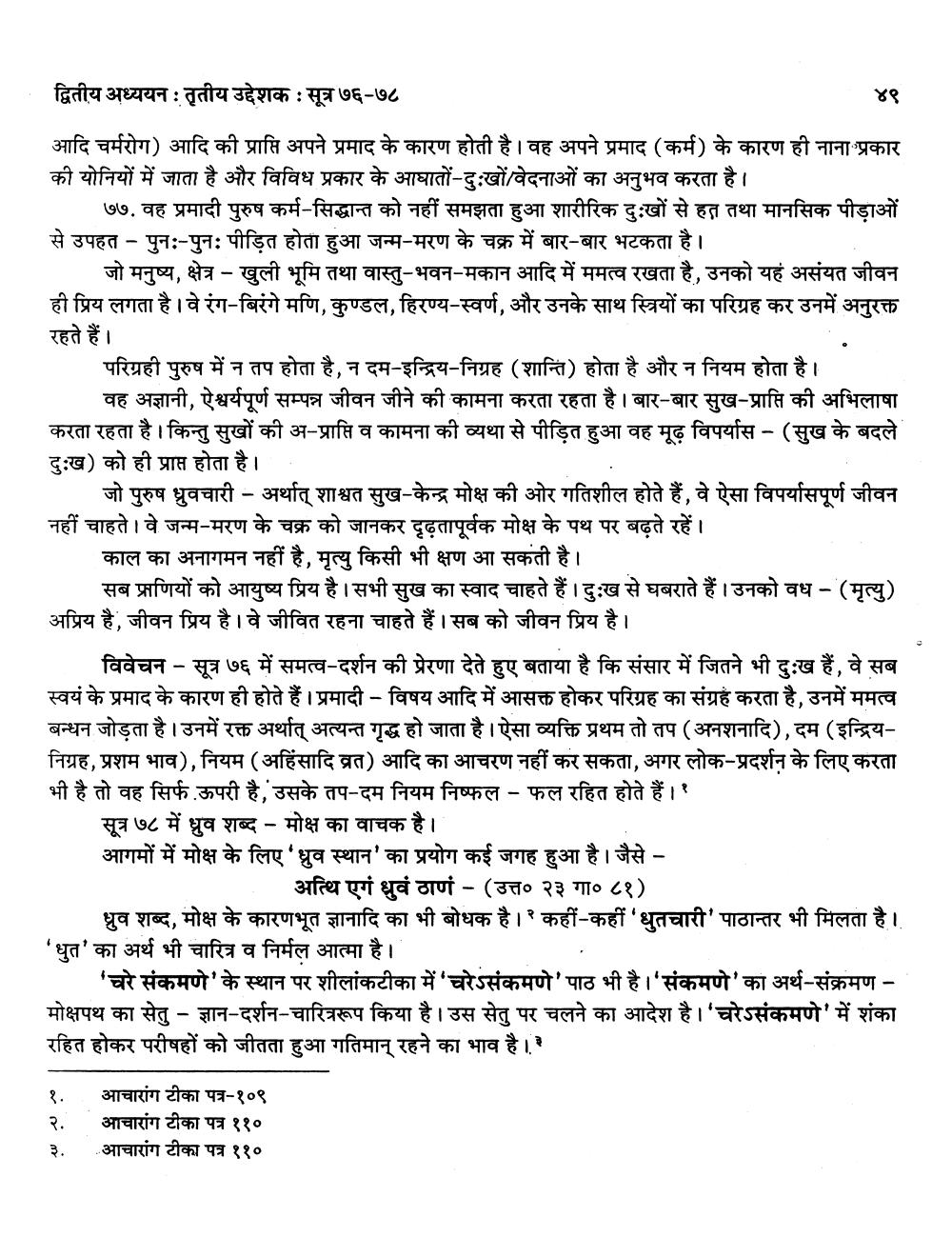________________
द्वितीय अध्ययन : तृतीय उद्देशक: सूत्र ७६-७८
आदि चर्मरोग) आदि की प्राप्ति अपने प्रमाद के कारण होती है। वह अपने प्रमाद (कर्म) के कारण ही नाना प्रकार की योनियों में जाता है और विविध प्रकार के आघातों-दुःखों/वेदनाओं का अनुभव करता है।
७७. वह प्रमादी पुरुष कर्म - सिद्धान्त को नहीं समझता हुआ शारीरिक दुःखों से हत तथा मानसिक पीड़ाओं से उपहत पुन: पुन: पीड़ित होता हुआ जन्म-मरण के चक्र में बार-बार भटकता है ।
जो 'मनुष्य, क्षेत्र - खुली भूमि तथा वास्तु भवन-मकान आदि में ममत्व रखता है, उनको यहं असंयत जीवन ही प्रिय लगता है। वे रंग-बिरंगे मणि, कुण्डल, हिरण्य-स्वर्ण, और उनके साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमें अनुरक्त रहते हैं ।
-
परिग्रही पुरुष में न तप होता है, न दम-इन्द्रिय - निग्रह (शान्ति) होता है और न नियम होता है ।
वह अज्ञानी, ऐश्वर्यपूर्ण सम्पन्न जीवन जीने की कामना करता रहता है। बार-बार सुख प्राप्ति की अभिलाषा करता रहता है । किन्तु सुखों की अ-प्राप्ति व कामना की व्यथा से पीड़ित हुआ वह मूढ़ विपर्यास - (सुख के बदले दुःख) को ही प्राप्त होता है।
जो
पुरुष ध्रुवचारी
अर्थात् शाश्वत सुख-केन्द्र मोक्ष की ओर गतिशील होते हैं, वे ऐसा विपर्यासपूर्ण जीवन नहीं चाहते। वे जन्म-मरण के चक्र को जानकर दृढ़तापूर्वक मोक्ष के पथ पर बढ़ते रहें ।
काल का अनागमन नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है।
४९
सब प्राणियों को आयुष्य प्रिय है। सभी सुख का स्वाद चाहते हैं । दुःख से घबराते हैं । उनको वध - (मृत्यु) अप्रिय है, जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते हैं । सब को जीवन प्रिय है ।
विवेचन - सूत्र ७६ में समत्व-दर्शन की प्रेरणा देते हुए बताया है कि संसार में जितने भी दुःख हैं, वे सब स्वयं के प्रमाद के कारण ही होते हैं। प्रमादी - विषय आदि में आसक्त होकर परिग्रह का संग्रह करता है, उनमें ममत्व बन्धन जोड़ता है। उनमें रक्त अर्थात् अत्यन्त गृद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रथम तो तप ( अनशनादि), दम (इन्द्रियनिग्रह, प्रशम भाव ), नियम (अहिंसादि व्रत) आदि का आचरण नहीं कर सकता, अगर लोक-प्रदर्शन के लिए करता भी है तो वह सिर्फ ऊपरी है, उसके तप-दम नियम निष्फल - फल रहित होते हैं । '
सूत्र ७८ में ध्रुव शब्द - मोक्ष का वाचक है।
आगमों में मोक्ष के लिए 'ध्रुव स्थान' का प्रयोग कई जगह हुआ है। जैसे
अत्थि एगं ध्रुवं ठाणं (उत्त० २३ गा० ८१ )
ध्रुव शब्द, मोक्ष के कारणभूत ज्ञानादि का भी बोधक है। कहीं-कहीं 'धुतचारी' पाठान्तर भी मिलता है। 'धुत' का अर्थ भी चारित्र व निर्मल आत्मा है ।
"
१.
२.
३.
-
'चरे संकमणे' के स्थान पर शीलांकटीका में 'चरेऽसंकमणे' पाठ भी है। 'संकमणे' का अर्थ-संक्रमण - मोक्षपथ का सेतु - ज्ञान - दर्शन - चारित्ररूप किया है। उस सेतु पर चलने का आदेश है । 'चरेऽसंकमणे' में शंका रहित होकर परीषहों को जीतता हुआ गतिमान् रहने का भाव है।
आचारांग टीका पत्र - १०९
आचारांग टीका पत्र ११०
• आचारांग टीका पत्र ११०