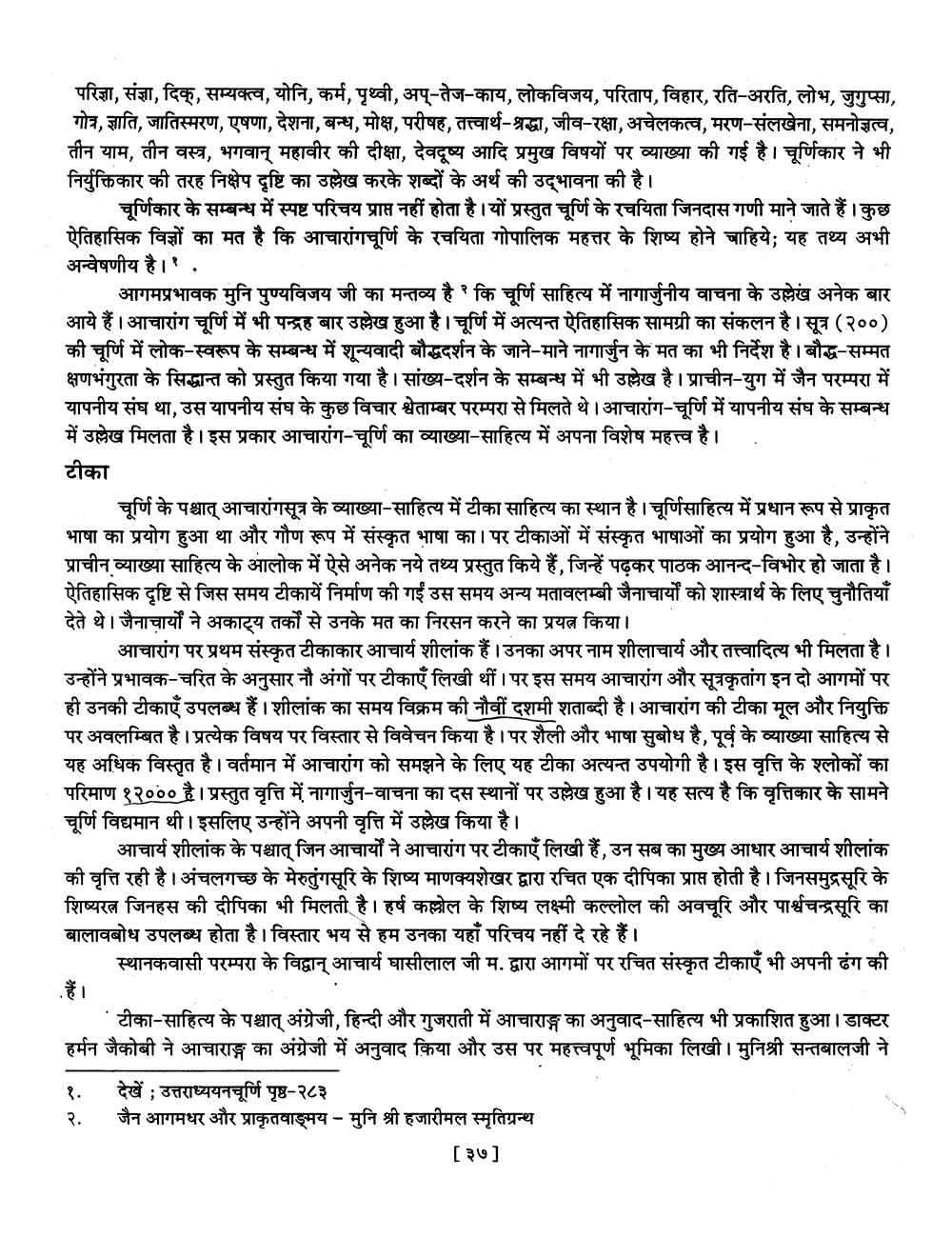________________
परिज्ञा, संज्ञा, दिक्, सम्यक्त्व, योनि, कर्म, पृथ्वी, अप्-तेज-काय, लोकविजय, परिताप, विहार, रति-अरति, लोभ, जुगुप्सा, गोत्र, ज्ञाति, जातिस्मरण, एषणा, देशना, बन्ध, मोक्ष, परीषह, तत्त्वार्थ-श्रद्धा, जीव-रक्षा, अचेलकत्व, मरण-संलखेना, समनोज्ञत्व, तीन याम, तीन वस्त्र, भगवान् महावीर की दीक्षा, देवदूष्य आदि प्रमुख विषयों पर व्याख्या की गई है। चूर्णिकार ने भी नियुक्तिकार की तरह निक्षेप दृष्टि का उल्लेख करके शब्दों के अर्थ की उद्भावना की है।
चूर्णिकार के सम्बन्ध में स्पष्ट परिचय प्राप्त नहीं होता है। यों प्रस्तुत चूर्णि के रचयिता जिनदास गणी माने जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक विज्ञों का मत है कि आचारांगचूर्णि के रचयिता गोपालिक महत्तर के शिष्य होने चाहिये; यह तथ्य अभी अन्वेषणीय है। .
आगमप्रभावक मुनि पुण्यविजय जी का मन्तव्य है कि चूर्णि साहित्य में नागार्जुनीय वाचना के उल्लेख अनेक बार आये हैं। आचारांग चूर्णि में भी पन्द्रह बार उल्लेख हुआ है। चूर्णि में अत्यन्त ऐतिहासिक सामग्री का संकलन है। सूत्र (२००) की चूर्णि में लोक-स्वरूप के सम्बन्ध में शून्यवादी बौद्धदर्शन के जाने-माने नागार्जुन के मत का भी निर्देश है। बौद्ध-सम्मत क्षणभंगुरता के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया गया है। सांख्य-दर्शन के सम्बन्ध में भी उल्लेख है। प्राचीन-युग में जैन परम्परा में यापनीय संघ था, उस यापनीय संघ के कुछ विचार श्वेताम्बर परम्परा से मिलते थे। आचारांग-चूर्णि में यापनीय संघ के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है। इस प्रकार आचारांग-चूर्णि का व्याख्या-साहित्य में अपना विशेष महत्त्व है। . टीका
चूर्णि के पश्चात् आचारांगसूत्र के व्याख्या-साहित्य में टीका साहित्य का स्थान है । चूर्णिसाहित्य में प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और गौण रूप में संस्कृत भाषा का। पर टीकाओं में संस्कृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है, उन्होंने प्राचीन व्याख्या साहित्य के आलोक में ऐसे अनेक नये तथ्य प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक आनन्द-विभोर हो जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जिस समय टीकायें निर्माण की गईं उस समय अन्य मतावलम्बी जैनाचार्यों को शास्त्रार्थ के लिए चुनौतियाँ देते थे। जैनाचार्यों ने अकाट्य तर्कों से उनके मत का निरसन करने का प्रयत्न किया।
आचारांग पर प्रथम संस्कृत टीकाकार आचार्य शीलांक हैं। उनका अपर नाम शीलाचार्य और तत्त्वादित्य भी मिलता है। उन्होंने प्रभावक-चरित के अनुसार नौ अंगों पर टीकाएँ लिखी थीं। पर इस समय आचारांग और सूत्रकृतांग इन दो आगमों पर ही उनकी टीकाएँ उपलब्ध हैं। शीलांक का समय विक्रम की नौवीं दशमी शताब्दी है। आचारांग की टीका पर अवलम्बित है। प्रत्येक विषय पर विस्तार से विवेचन किया है। पर शैली और भाषा सुबोध है, पूर्व के व्याख्या साहित्य से यह अधिक विस्तृत है। वर्तमान में आचारांग को समझने के लिए यह टीका अत्यन्त उपयोगी है। इस वृत्ति के श्लोकों का परिमाण १२००० है। प्रस्तुत वृत्ति में नागार्जुन-वाचना का दस स्थानों पर उल्लेख हुआ है। यह सत्य है कि वृत्तिकार के सामने चूर्णि विद्यमान थी। इसलिए उन्होंने अपनी वृत्ति में उल्लेख किया है।
आचार्य शीलांक के पश्चात् जिन आचार्यों ने आचारांग पर टीकाएँ लिखी हैं, उन सब का मुख्य आधार आचार्य शीलांक की वृत्ति रही है। अंचलगच्छ के मेरुतुंगसूरि के शिष्य माणक्यशेखर द्वारा रचित एक दीपिका प्राप्त होती है। जिनसमुद्रसूरि के शिष्यरत्न जिनहस की दीपिका भी मिलती है। हर्ष कल्लोल के शिष्य लक्ष्मी कल्लोल की अवचूरि और पार्श्वचन्द्रसूरि का बालावबोध उपलब्ध होता है। विस्तार भय से हम उनका यहाँ परिचय नहीं दे रहे हैं।
स्थानकवासी परम्परा के विद्वान् आचार्य घासीलाल जी म. द्वारा आगमों पर रचित संस्कृत टीकाएँ भी अपनी ढंग की
टीका-साहित्य के पश्चात् अंग्रेजी, हिन्दी और गुजराती में आचाराङ्ग का अनुवाद-साहित्य भी प्रकाशित हुआ। डाक्टर हर्मन जैकोबी ने आचाराङ्ग का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उस पर महत्त्वपूर्ण भूमिका लिखी। मुनिश्री सन्तबालजी ने
१. २.
देखें ; उत्तराध्ययनचूर्णि पृष्ठ-२८३ जैन आगमधर और प्राकृतवाङ्मय - मुनि श्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ
[३७]