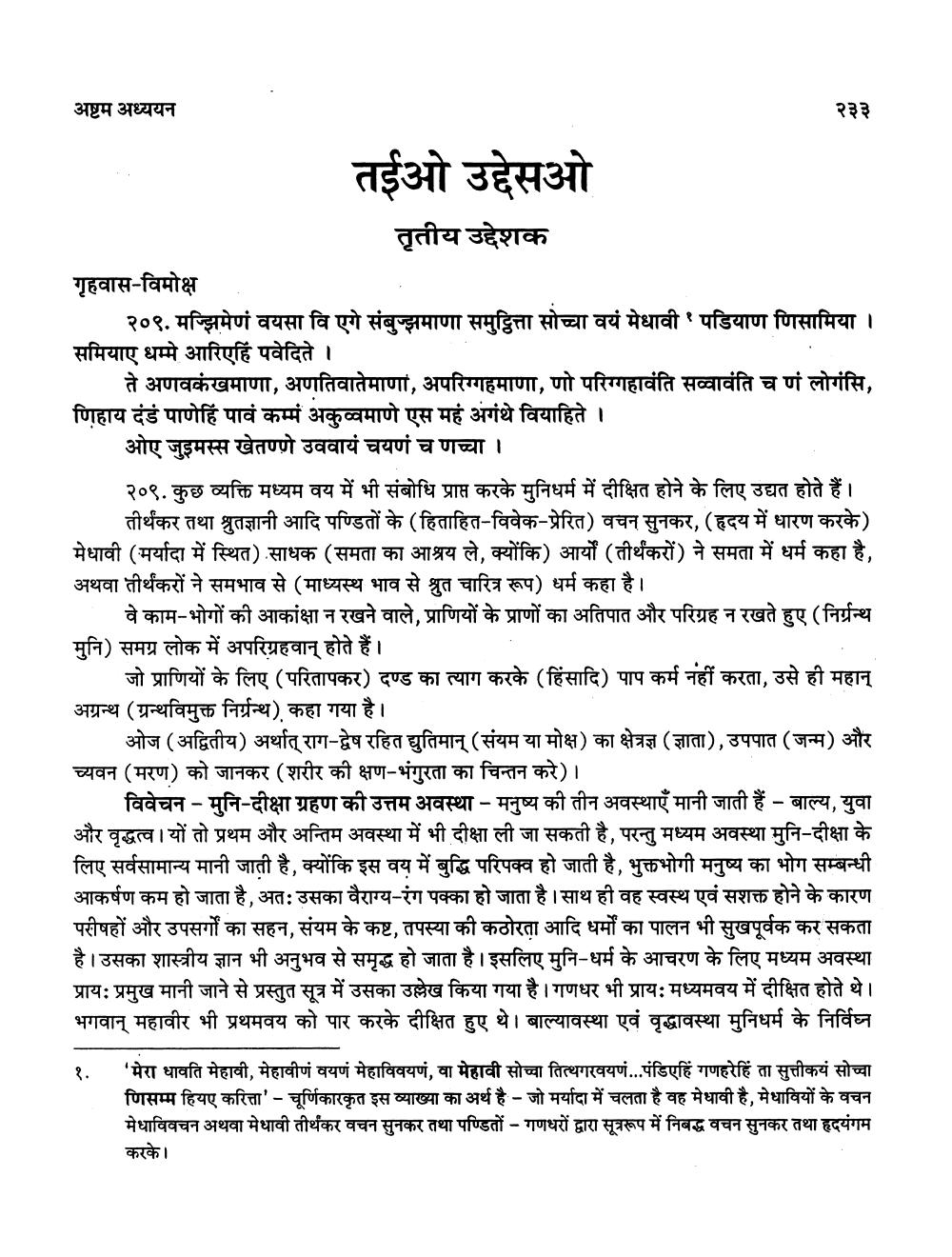________________
अष्टम अध्ययन
तईओ उद्देसओ
तृतीय उद्देशक
२३३
गृहवास-विमोक्ष
२०९. मज्झिमेणं वयसा वि एगे संबुज्झमाणा समुट्ठित्ता सोच्चा वयं मेधावी ' पडियाण णिसामिया । समिया धम्मे आरिएहिं पवेदिते ।
ते अणवखमाणा, अणतिवातेमाणां, अपरिग्गहमाणा, णो परिग्गहावंति सव्वावंति च णं लोगंसि, निहाय दंडं पाणेहिं पावं कम्मं अकुव्वमाणे एस महं अंगंथे वियाहिते ।
ओए जुइमस्स खेतण्णे उववायं चयणं च णच्चा ।
२०९. कुछ व्यक्ति मध्यम वय में भी संबोधि प्राप्त करके मुनिधर्म में दीक्षित होने के लिए उद्यत होते हैं । तीर्थंकर तथा श्रुतज्ञानी आदि पण्डितों के ( हिताहित- विवेक - प्रेरित) वचन सुनकर, (हृदय में धारण करके) मेधावी (मर्यादा में स्थित ) साधक (समता का आश्रय ले, क्योंकि) आर्यों (तीर्थंकरों) ने समता में धर्म कहा है, अथवा तीर्थंकरों ने समभाव से (माध्यस्थ भाव से श्रुत चारित्र रूप) धर्म कहा है।
वे काम-भोगों की आकांक्षा न रखने वाले, प्राणियों के प्राणों का अतिपात और परिग्रह न रखते मुनि) समग्र लोक में अपरिग्रहवान् होते हैं ।
जो प्राणियों के लिए (परितापकर) दण्ड का त्याग करके (हिंसादि) पाप कर्म नहीं करता, अग्रन्थ (ग्रन्थविमुक्त निर्ग्रन्थ) कहा गया है।
१.
हुए (निर्ग्रन्थ
उसे ही महान्
ओज (अद्वितीय) अर्थात् राग-द्वेष रहित द्युतिमान् (संयम या मोक्ष) का क्षेत्रज्ञ (ज्ञाता), उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) को जानकर (शरीर की क्षण- -भंगुरता का चिन्तन करे) ।
विवेचन – मुनि-दीक्षा ग्रहण की उत्तम अवस्था - मनुष्य की तीन अवस्थाएँ मानी जाती हैं - बाल्य, युवा
-
और वृद्धत्व। यों तो प्रथम और अन्तिम अवस्था में भी दीक्षा ली जा सकती है, परन्तु मध्यम अवस्था मुनि दीक्षा के लिए सर्वसामान्य मानी जाती है, क्योंकि इस वय में बुद्धि परिपक्व हो जाती है, भुक्तभोगी मनुष्य का भोग सम्बन्धी आकर्षण कम हो जाता है, अतः उसका वैराग्य-रंग पक्का हो जाता है। साथ ही वह स्वस्थ एवं सशक्त होने के कारण परीषहों और उपसर्गों का सहन, संयम के कष्ट, तपस्या की कठोरता आदि धर्मों का पालन भी सुखपूर्वक कर सकता है। उसका शास्त्रीय ज्ञान भी अनुभव से समृद्ध हो जाता है। इसलिए मुनि-धर्म के आचरण के लिए मध्यम अवस्था प्राय: प्रमुख मानी जाने से प्रस्तुत सूत्र में उसका उल्लेख किया गया है। गणधर भी प्रायः मध्यमवय में दीक्षित होते थे । भगवान् महावीर भी प्रथमवय को पार करके दीक्षित हुए थे । बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था मुनिधर्म के निर्विघ्न
'मेरा धावति मेहावी, मेहावीणं वयणं मेहाविवयणं, वा मेहावी सोच्चा तित्थगरवयणं... पंडिएहिं गणहरेहिं ता सुत्तीकयं सोच्चा णिसम्म हियए करित्ता' - चूर्णिकारकृत इस व्याख्या का अर्थ है - जो मर्यादा में चलता है वह मेधावी है, मेधावियों के वचन मेधाविवचन अथवा मेधावी तीर्थंकर वचन सुनकर तथा पण्डितों - गणधरों द्वारा सूत्ररूप में निबद्ध वचन सुनकर तथा हृदयंगम करके ।