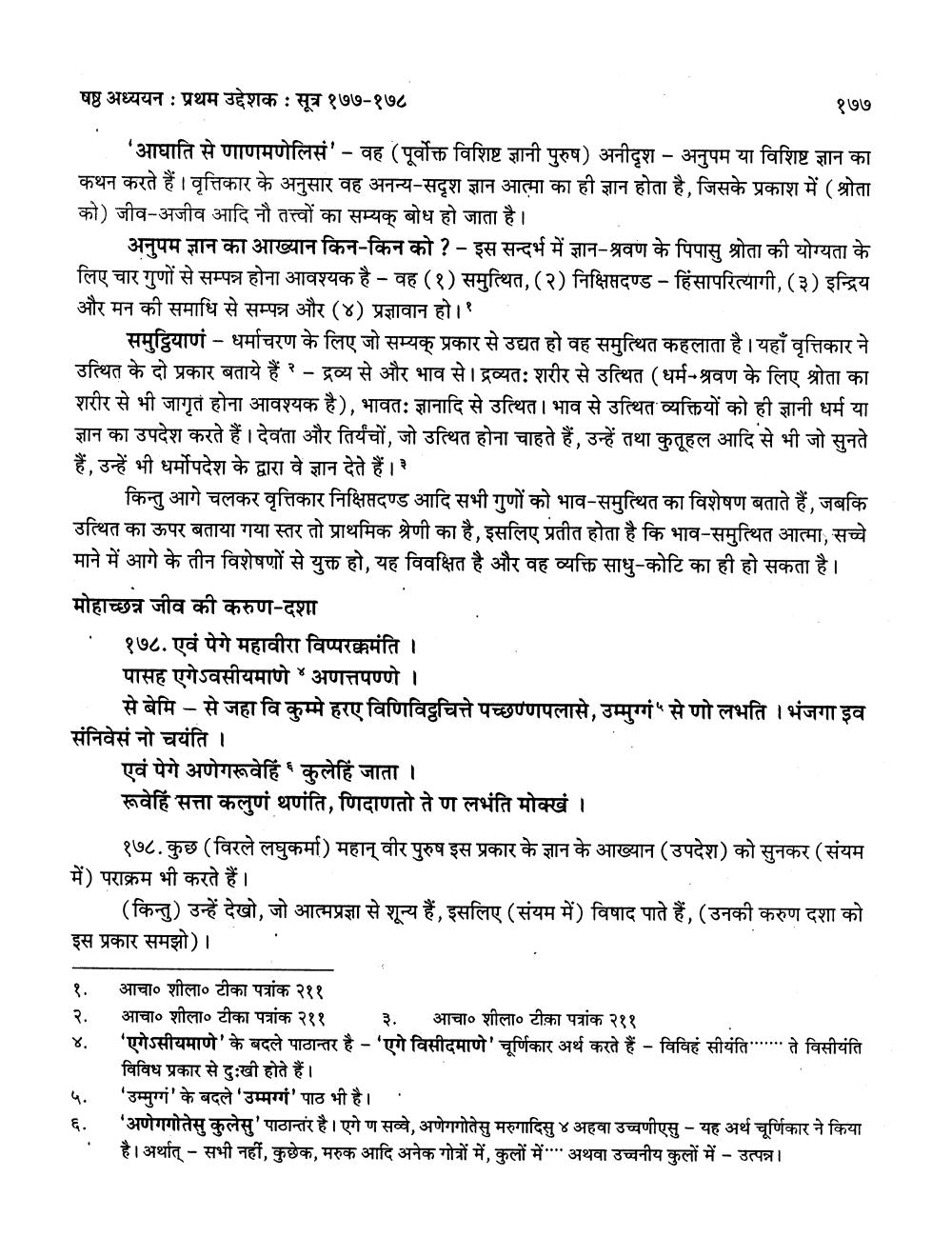________________
षष्ठ अध्ययन : प्रथम उद्देशक : सूत्र १७७-१७८
१७७
__ 'आघाति से णाणमणेलिसं' - वह (पूर्वोक्त विशिष्ट ज्ञानी पुरुष) अनीदृश - अनुपम या विशिष्ट ज्ञान का कथन करते हैं । वृत्तिकार के अनुसार वह अनन्य-सदृश ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान होता है, जिसके प्रकाश में (श्रोता को) जीव-अजीव आदि नौ तत्त्वों का सम्यक् बोध हो जाता है।
अनुपम ज्ञान का आख्यान किन-किन को ? - इस सन्दर्भ में ज्ञान-श्रवण के पिपासु श्रोता की योग्यता के लिए चार गुणों से सम्पन्न होना आवश्यक है - वह (१) समुत्थित, (२) निक्षिप्तदण्ड - हिंसापरित्यागी, (३) इन्द्रिय और मन की समाधि से सम्पन्न और (४) प्रज्ञावान हो।
समुट्ठियाणं - धर्माचरण के लिए जो सम्यक् प्रकार से उद्यत हो वह समुत्थित कहलाता है । यहाँ वृत्तिकार ने उत्थित के दो प्रकार बताये हैं २ - द्रव्य से और भाव से। द्रव्यतः शरीर से उत्थित (धर्म-श्रवण के लिए श्रोता का शरीर से भी जागृत होना आवश्यक है), भावतः ज्ञानादि से उत्थित । भाव से उत्थित व्यक्तियों को ही ज्ञानी धर्म या ज्ञान का उपदेश करते हैं । देवता और तिर्यंचों, जो उत्थित होना चाहते हैं, उन्हें तथा कुतूहल आदि से भी जो सुनते हैं, उन्हें भी धर्मोपदेश के द्वारा वे ज्ञान देते हैं। ३
किन्तु आगे चलकर वृत्तिकार निक्षिप्तदण्ड आदि सभी गुणों को भाव-समुत्थित का विशेषण बताते हैं, जबकि उत्थित का ऊपर बताया गया स्तर तो प्राथमिक श्रेणी का है, इसलिए प्रतीत होता है कि भाव-समुत्थित आत्मा, सच्चे माने में आगे के तीन विशेषणों से युक्त हो, यह विवक्षित है और वह व्यक्ति साधु-कोटि का ही हो सकता है। मोहाच्छन्न जीव की करुण-दशा
१७८. एवं पेगे महावीरा विप्परक्कमंति । पासह एगेऽवसीयमाणे ४ अणत्तपण्णे।
से बेमि - से जहा वि कुम्मे हरए विणिविट्ठचित्ते पच्छण्णपलासे, उम्मुग्गं से णो लभति । भंजगा इव संनिवेसं नो चयंति ।
एवं पेगे अणेगरूवेहि कुलेहिं जाता ।
रूवेहिं सत्ता कलुणं थणंति, णिदाणतो ते ण लभंति मोक्खं । __ १७८. कुछ (विरले लघुकर्मा) महान् वीर पुरुष इस प्रकार के ज्ञान के आख्यान (उपदेश) को सुनकर (संयम में) पराक्रम भी करते हैं।
(किन्तु) उन्हें देखो, जो आत्मप्रज्ञा से शून्य हैं, इसलिए (संयम में) विषाद पाते हैं, (उनकी करुण दशा को इस प्रकार समझो)।
आचा० शीला० टीका पत्रांक २११
आचा० शीला० टीका पत्रांक २११ ३. आचा० शीला० टीका पत्रांक २११ ४. 'एगेऽसीयमाणे' के बदले पाठान्तर है - 'एगे विसीदमाणे' चूर्णिकार अर्थ करते हैं - विविहं सीयंति....." ते विसीयंति
विविध प्रकार से दुःखी होते हैं।
'उम्मुग्गं' के बदले 'उम्मग्गं' पाठ भी है। . ६. 'अणेगगोतेसु कुलेसु' पाठान्तर है। एगे ण सव्वे, अणेगगोतेसु मरुगादिसु ४ अहवा उच्चणीएसु - यह अर्थ चूर्णिकार ने किया
है। अर्थात् - सभी नहीं, कुछेक, मरुक आदि अनेक गोत्रों में, कुलों में "" अथवा उच्चनीय कुलों में - उत्पन्न ।