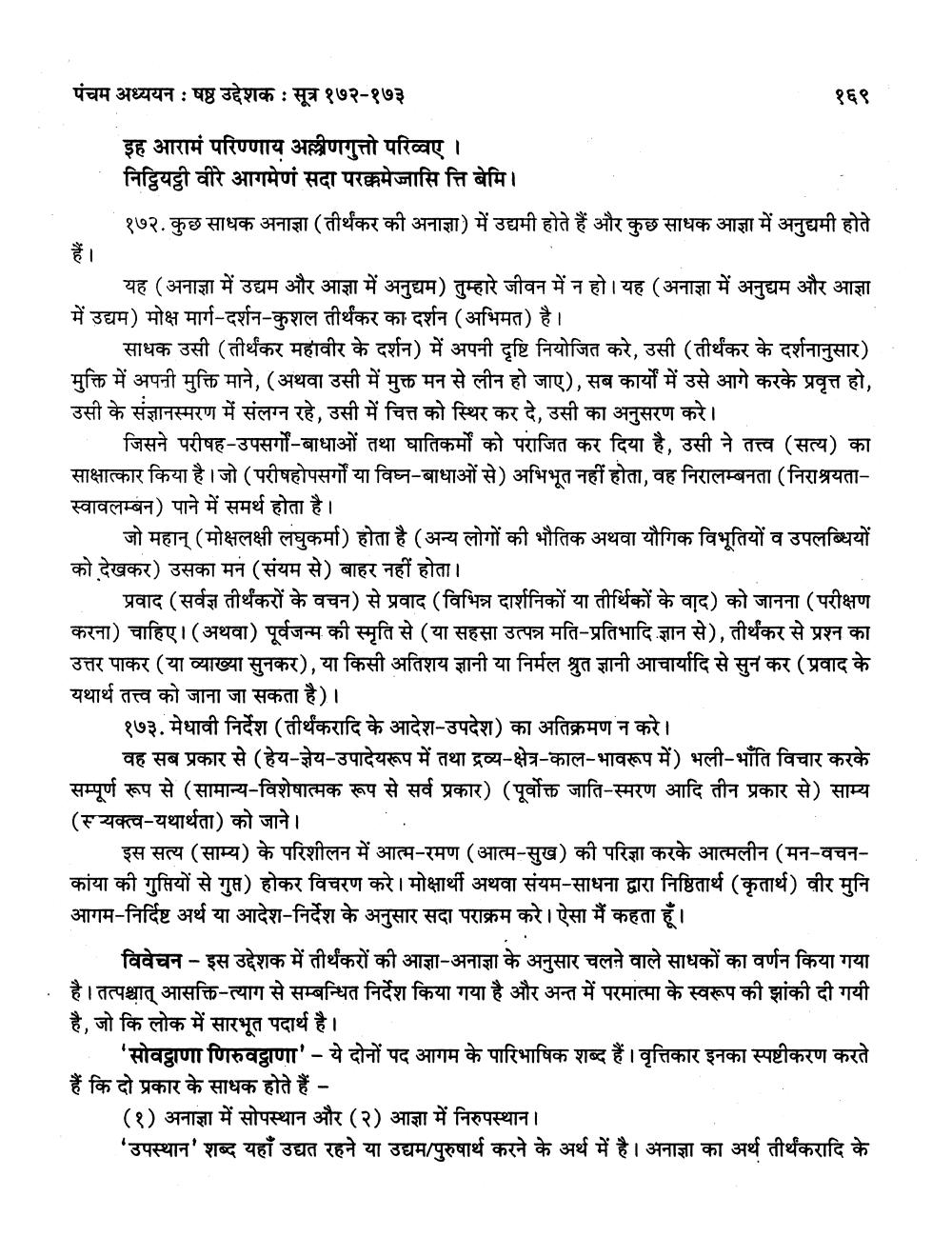________________
१६९
पंचम अध्ययन : षष्ठ उद्देशक : सूत्र १७२-१७३
इह आरामं परिणाय अल्लीणगुत्तो परिव्वए । निट्ठियट्ठी वीरे आगमेणं सदा परक्कमेजासि त्ति बेमि। १७२. कुछ साधक अनाज्ञा (तीर्थंकर की अनाज्ञा) में उद्यमी होते हैं और कुछ साधक आज्ञा में अनुद्यमी होते
यह (अनाज्ञा में उद्यम और आज्ञा में अनुद्यम) तुम्हारे जीवन में न हो। यह (अनाज्ञा में अनुद्यम और आज्ञा में उद्यम) मोक्ष मार्ग-दर्शन-कुशल तीर्थंकर का दर्शन (अभिमत) है।
साधक उसी (तीर्थंकर महावीर के दर्शन) में अपनी दृष्टि नियोजित करे, उसी (तीर्थंकर के दर्शनानुसार) मुक्ति में अपनी मुक्ति माने, (अथवा उसी में मुक्त मन से लीन हो जाए), सब कार्यों में उसे आगे करके प्रवृत्त हो, उसी के संज्ञानस्मरण में संलग्न रहे, उसी में चित्त को स्थिर कर दे, उसी का अनुसरण करे।
जिसने परीषह-उपसर्गों-बाधाओं तथा घातिकर्मों को पराजित कर दिया है, उसी ने तत्त्व (सत्य) का साक्षात्कार किया है। जो (परीषहोपसर्गों या विघ्न-बाधाओं से) अभिभूत नहीं होता, वह निरालम्बनता (निराश्रयतास्वावलम्बन) पाने में समर्थ होता है।
जो महान् (मोक्षलक्षी लघुकर्मा) होता है (अन्य लोगों की भौतिक अथवा यौगिक विभूतियों व उपलब्धियों को देखकर) उसका मन (संयम से) बाहर नहीं होता।
प्रवाद (सर्वज्ञ तीर्थंकरों के वचन) से प्रवाद (विभिन्न दार्शनिकों या तीर्थकों के वाद) को जानना (परीक्षण करना) चाहिए। (अथवा) पूर्वजन्म की स्मृति से (या सहसा उत्पन्न मति-प्रतिभादि ज्ञान से), तीर्थंकर से प्रश्न का उत्तर पाकर (या व्याख्या सुनकर), या किसी अतिशय ज्ञानी या निर्मल श्रुत ज्ञानी आचार्यादि से सुन कर (प्रवाद के यथार्थ तत्त्व को जाना जा सकता है)।
१७३. मेधावी निर्देश (तीर्थंकरादि के आदेश-उपदेश) का अतिक्रमण न करे।
वह सब प्रकार से (हेय-ज्ञेय-उपादेयरूप में तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप में) भली-भाँति विचार करके सम्पूर्ण रूप से (सामान्य-विशेषात्मक रूप से सर्व प्रकार) (पूर्वोक्त जाति-स्मरण आदि तीन प्रकार से) साम्य (सयक्त्व-यथार्थता) को जाने।
____ इस सत्य (साम्य) के परिशीलन में आत्म-रमण (आत्म-सुख) की परिज्ञा करके आत्मलीन (मन-वचनकाया की गुप्तियों से गुप्त) होकर विचरण करे । मोक्षार्थी अथवा संयम-साधना द्वारा निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर मुनि आगम-निर्दिष्ट अर्थ या आदेश-निर्देश के अनुसार सदा पराक्रम करे। ऐसा मैं कहता हूँ।
विवेचन - इस उद्देशक में तीर्थंकरों की आज्ञा-अनाज्ञा के अनुसार चलने वाले साधकों का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् आसक्ति-त्याग से सम्बन्धित निर्देश किया गया है और अन्त में परमात्मा के स्वरूप की झांकी दी गयी है, जो कि लोक में सारभूत पदार्थ है।
'सोवट्ठाणा णिरुवट्ठाणा' - ये दोनों पद आगम के पारिभाषिक शब्द हैं । वृत्तिकार इनका स्पष्टीकरण करते हैं कि दो प्रकार के साधक होते हैं -
(१) अनाज्ञा में सोपस्थान और (२) आज्ञा में निरुपस्थान। 'उपस्थान' शब्द यहाँ उद्यत रहने या उद्यम/पुरुषार्थ करने के अर्थ में है। अनाज्ञा का अर्थ तीर्थंकरादि के