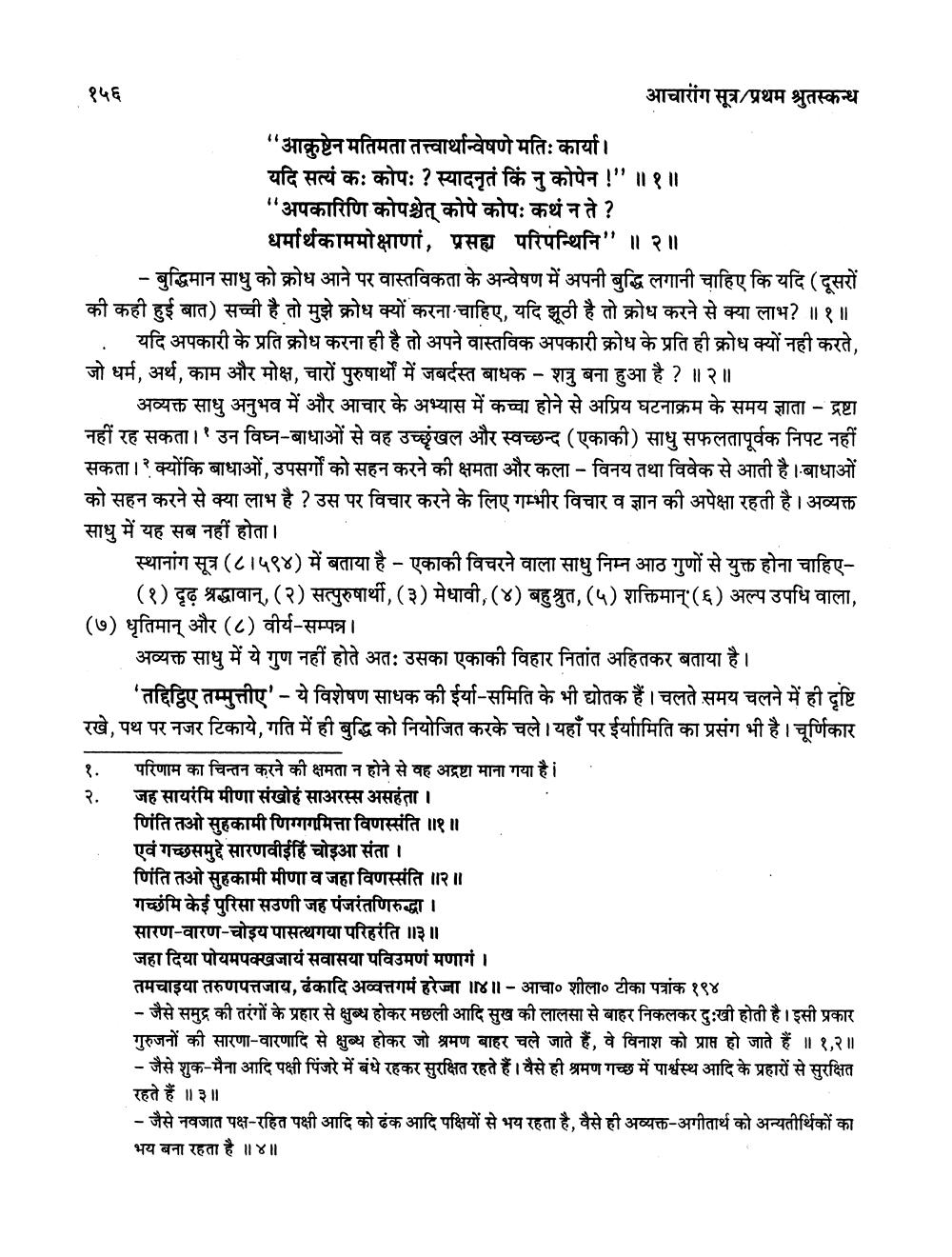________________
१५६
आचारांग सूत्र/प्रथम श्रुतस्कन्ध
"आनुष्टेन मतिमता तत्त्वार्थान्वेषणे मतिः कार्या। यदि सत्यं कः कोपः ? स्यादनृतं किं नु कोपेन !" ॥१॥ "अपकारिणि कोपश्चेत् कोपे कोपः कथं न ते ?
धर्मार्थकाममोक्षाणां, प्रसह्य परिपन्थिनि" ॥ २॥ - बुद्धिमान साधु को क्रोध आने पर वास्तविकता के अन्वेषण में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए कि यदि (दूसरों की कही हुई बात) सच्ची है तो मुझे क्रोध क्यों करना चाहिए, यदि झूठी है तो क्रोध करने से क्या लाभ? ॥१॥
यदि अपकारी के प्रति क्रोध करना ही है तो अपने वास्तविक अपकारी क्रोध के प्रति ही क्रोध क्यों नही करते, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों में जबर्दस्त बाधक - शत्रु बना हुआ है ? ॥२॥ ____ अव्यक्त साधु अनुभव में और आचार के अभ्यास में कच्चा होने से अप्रिय घटनाक्रम के समय ज्ञाता - द्रष्टा नहीं रह सकता। उन विघ्न-बाधाओं से वह उच्छृखल और स्वच्छन्द (एकाकी) साधु सफलतापूर्वक निपट नहीं सकता। क्योंकि बाधाओं, उपसर्गों को सहन करने की क्षमता और कला - विनय तथा विवेक से आती है। बाधाओं को सहन करने से क्या लाभ है ? उस पर विचार करने के लिए गम्भीर विचार व ज्ञान की अपेक्षा रहती है। अव्यक्त साधु में यह सब नहीं होता।
स्थानांग सूत्र (८१५९४) में बताया है - एकाकी विचरने वाला साधु निम्न आठ गुणों से युक्त होना चाहिए___ (१) दृढ़ श्रद्धावान्, (२) सत्पुरुषार्थी, (३) मेधावी, (४) बहुश्रुत, (५) शक्तिमान् (६) अल्प उपधि वाला, (७) धृतिमान् और (८) वीर्य-सम्पन्न।
अव्यक्त साधु में ये गुण नहीं होते अतः उसका एकाकी विहार नितांत अहितकर बताया है।
'तद्दिट्ठिए तम्मुत्तीए' - ये विशेषण साधक की ईर्या-समिति के भी द्योतक हैं। चलते समय चलने में ही दृष्टि रखे, पथ पर नजर टिकाये, गति में ही बुद्धि को नियोजित करके चले। यहाँ पर ईर्यामिति का प्रसंग भी है। चूर्णिकार
परिणाम का चिन्तन करने की क्षमता न होने से वह अद्रष्टा माना गया है। जह सायरंमि मीणा संखोहं साअरस्स असहंता । णिति तओ सुहकामी णिग्गगमित्ता विणस्संति ॥१॥ एवं गच्छसमुद्दे सारणवीईहिं चोइआ संता। णिति तओ सुहकामी मीणा व जहा विणस्संति ॥२॥ गच्छंमि केई पुरिसा सउणीजह पंजरंतणिरुद्धा। सारण-वारण-चोइय पासस्थगया परिहरंति ॥३॥ जहा दिया पोयमपक्खजायं सवासया पविउमणं मणागं । तमचाइया तरुणपत्तजाय, ढंकादि अव्वत्तगमं हरेजा ॥४॥- आचा० शीला० टीका पत्रांक १९४ - जैसे समुद्र की तरंगों के प्रहार से क्षुब्ध होकर मछली आदि सुख की लालसा से बाहर निकलकर दुःखी होती है। इसी प्रकार गुरुजनों की सारणा-वारणादि से क्षुब्ध होकर जो श्रमण बाहर चले जाते हैं, वे विनाश को प्राप्त हो जाते हैं ॥ १,२॥ - जैसे शुक-मैना आदि पक्षी पिंजरे में बंधे रहकर सुरक्षित रहते हैं। वैसे ही श्रमण गच्छ में पार्श्वस्थ आदि के प्रहारों से सुरक्षित रहते हैं ॥३॥ - जैसे नवजात पक्ष-रहित पक्षी आदि को ढंक आदि पक्षियों से भय रहता है, वैसे ही अव्यक्त-अगीतार्थ को अन्यतीर्थिकों का भय बना रहता है ॥४॥