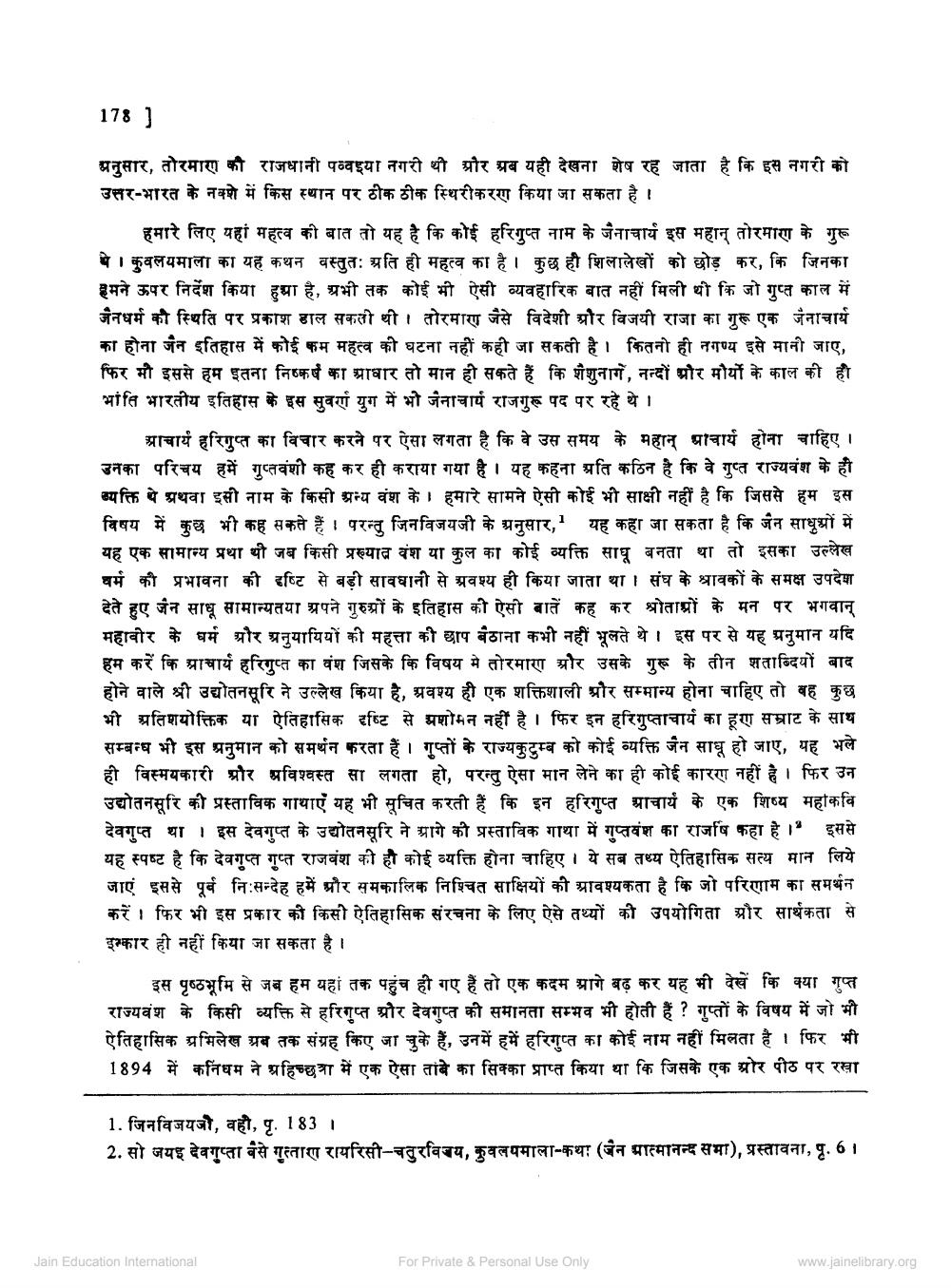________________
178 ]
अनुसार, तोरमाण की राजधानी पव्वइया नगरी थी और अब यही देखना शेष रह जाता है कि इस नगरी को उत्तर- भारत के नक्शे में किस स्थान पर ठीक ठीक स्थिरीकरण किया जा सकता है ।
हमारे लिए यहां महत्व की बात तो यह है कि कोई हरिगुप्त नाम के जैनाचार्य इस महान् तोरमाण के गुरू थे । कुवलयमाला का यह कथन वस्तुतः प्रति ही महत्व का है। कुछ ही शिलालेखों को छोड़ कर, कि जिनका हमने ऊपर निर्देश किया हुआ है, अभी तक कोई भी ऐसी व्यवहारिक बात नहीं मिली थी कि जो गुप्त काल में जैनधर्म की स्थिति पर प्रकाश डाल सकती थी। तोरमाण जैसे विदेशी और विजयी राजा का गुरू एक जैनाचार्य का होना जैन इतिहास में कोई कम महत्व की घटना नहीं कही जा सकती है। कितनो ही नगण्य इसे मानी जाए, फिर भी इससे हम इतना निष्कर्ष का आधार तो मान ही सकते हैं कि शैशुनार्ग, नन्दों और मौर्यो के काल की हो भांति भारतीय इतिहास के इस सुवर्ण युग में भी जंनाचार्य राजगुरू पद पर रहे थे।
1
प्राचार्य हरिगुप्त का विचार करने पर ऐसा लगता है कि वे उस समय के महान् आचार्य होना चाहिए । उनका परिचय हमें गुप्तवंशी कह कर ही कराया गया है। यह कहना अति कठिन है कि वे गुप्त राज्यवंश के ही व्यक्ति थे अथवा इसी नाम के किसी अन्य वंश के हमारे सामने ऐसी कोई भी साक्षी नहीं है कि जिससे हम इस विषय में कुछ भी कह सकते हैं । परन्तु जिनविजयजी के अनुसार, ' यह कहा जा सकता है कि जैन साधुओं में यह एक सामान्य प्रथा थी जब किसी प्रख्यात वंश या कुल का कोई व्यक्ति साधू बनता था तो इसका उल्लेख धर्म को प्रभावना की दृष्टि से बड़ी सावधानी से अवश्य ही किया जाता था। संघ के श्रावकों के समक्ष उपदेश देते हुए जैन साधू सामान्यतया अपने गुरुत्रों के इतिहास की ऐसी बातें कह कर श्रोताओं के मन पर भगवान् महावीर के धर्म और अनुयायियों की महत्ता की छाप बैठाना कभी नहीं भूलते थे । इस पर से यह अनुमान यदि हम करें कि प्राचार्य हरिगुप्त का वंश जिसके कि विषय मे तोरमाण और उसके गुरू के तीन शताब्दियों बाद होने वाले श्री उद्योतनसूरि ने उल्लेख किया है, अवश्य ही एक शक्तिशाली और सम्मान्य होना चाहिए तो वह कुछ भी अतिशयोक्तिक या ऐतिहासिक दृष्टि से अशोमन नहीं है । फिर इन हरिगुप्ताचार्य का हूण सम्राट के साथ सम्बन्ध भी इस अनुमान को समर्थन करता हैं। गुप्तों के राज्यकुटुम्ब को कोई व्यक्ति जैन साधू हो जाए, यह भले ही विस्मयकारी और अविश्वस्त सा लगता हो, परन्तु ऐसा मान लेने का ही कोई कारण नहीं है। फिर उन उद्योतनसूरि की प्रस्ताविक गाथाएँ यह भी सूचित करती हैं कि इन हरिगुप्त आचार्य के एक शिष्य महाकवि देवगुप्त था इस देवगुप्त के उद्योतनसूरि ने धागे की प्रस्ताविक गाथा में गुप्तवंश का राजवि कहा है।" इससे यह स्पष्ट है कि देवगुप्त गुप्त राजवंश की ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। ये सब तथ्य ऐतिहासिक सत्य मान लिये जाएं इससे पूर्व निःसन्देह हमें और समकालिक निश्चित साक्षियों की आवश्यकता है कि जो परिणाम का समर्थन करें । फिर भी इस प्रकार को किसी ऐतिहासिक संरचना के लिए ऐसे तथ्यों की उपयोगिता और सार्थकता से इकार ही नहीं किया जा सकता है ।
इस पृष्ठभूमि से जब हम यहां तक पहुंच ही गए हैं तो एक कदम आगे बढ़ कर यह भी देखें कि क्या गुप्त राज्यवंश के किसी व्यक्ति से हरिगुप्त और देवगुप्त की समानता सम्भव भी होती हैं ? गुप्तों के विषय में जो भी ऐतिहासिक अभिलेख यब तक संग्रह किए जा चुके हैं, उनमें हमें हरिगुप्त का कोई नाम नहीं मिलता है। फिर भी 1894 में कनिधम ने अहिच्छत्रा में एक ऐसा तांबे का सिक्का प्राप्त किया था कि जिसके एक ओर पीठ पर रखा
1. जिनविजयजी, वही, पृ. 183
2. सो जय देवगुप्ता से गुस्तारा रावरिसी चतुरविजय कुवलयमाला - कथा (जैन मात्मानन्द सभा), प्रस्तावना, पृ.61
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org