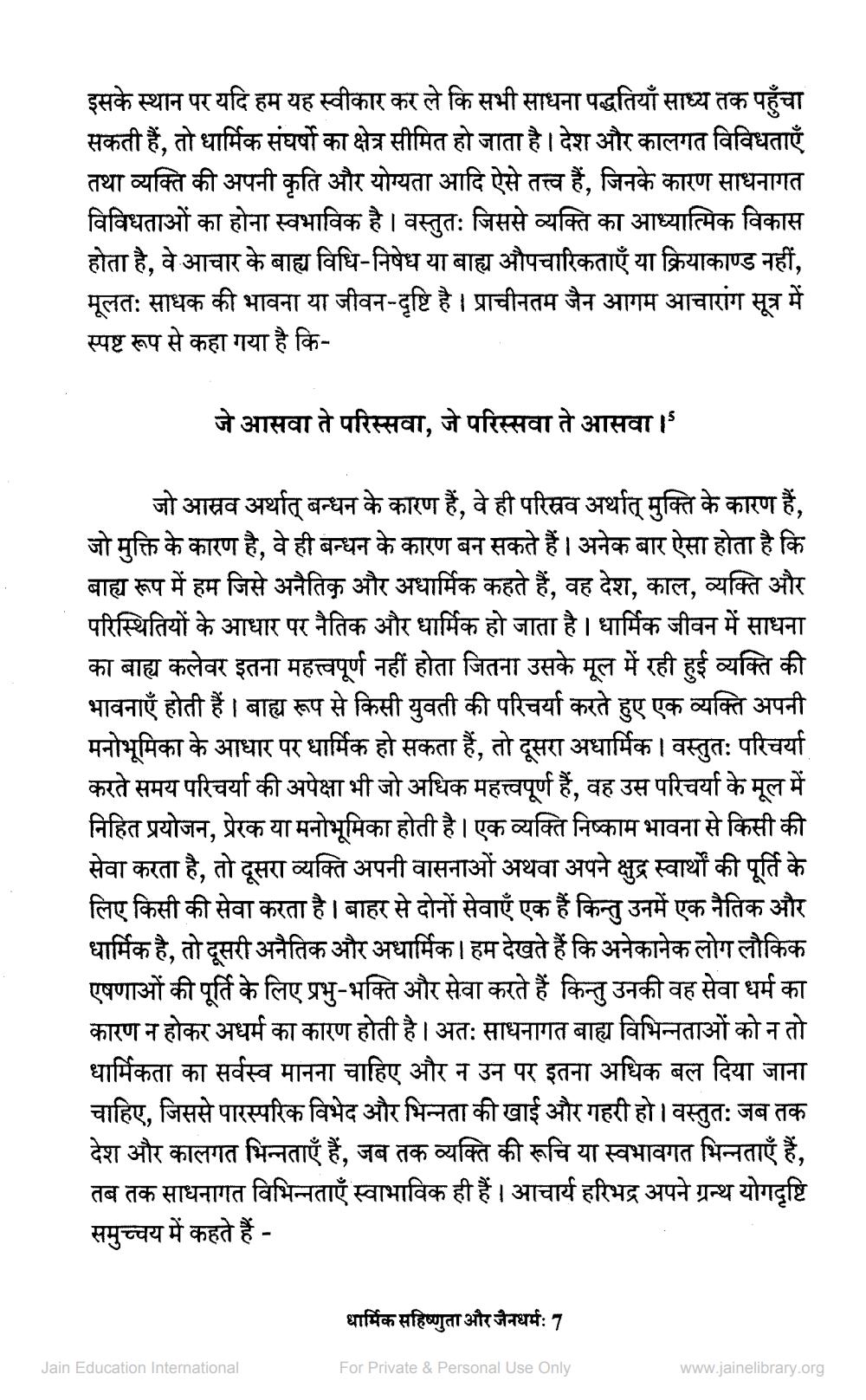________________
इसके स्थान पर यदि हम यह स्वीकार कर ले कि सभी साधना पद्धतियाँ साध्य तक पहुँचा सकती हैं, तो धार्मिक संघर्षो का क्षेत्र सीमित हो जाता है। देश और कालगत विविधताएँ तथा व्यक्ति की अपनी कृति और योग्यता आदि ऐसे तत्त्व हैं, जिनके कारण साधनागत विविधताओं का होना स्वभाविक है । वस्तुतः जिससे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होता है, वे आचार के बाह्य विधि-निषेध या बाह्य औपचारिकताएँ या क्रियाकाण्ड नहीं, मूलतः साधक की भावना या जीवन-दृष्टि है। प्राचीनतम जैन आगम आचारांग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि
जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा । '
जो आसव अर्थात् बन्धन के कारण हैं, वे ही परिस्रव अर्थात् मुक्ति के कारण हैं, मुक्तिकरण है, वे ही बन्धन के कारण बन सकते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि बाह्य रूप में हम जिसे अनैतिक और अधार्मिक कहते हैं, वह देश, काल, व्यक्ति और परिस्थितियों के आधार पर नैतिक और धार्मिक हो जाता है। धार्मिक जीवन में साधना का बाह्य कलेवर इतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता जितना उसके मूल में रही हुई व्यक्ति की भावनाएँ होती हैं । बाह्य रूप से किसी युवती की परिचर्या करते हुए एक व्यक्ति अपनी मनोभूमिका के आधार पर धार्मिक हो सकता हैं, तो दूसरा अधार्मिक । वस्तुतः परिचर्या करते समय परिचर्या की अपेक्षा भी जो अधिक महत्त्वपूर्ण हैं, वह उस परिचर्या के मूल में निहित प्रयोजन, प्रेरक या मनोभूमिका होती है। एक व्यक्ति निष्काम भावना से किसी की सेवा करता है, तो दूसरा व्यक्ति अपनी वासनाओं अथवा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी की सेवा करता है। बाहर से दोनों सेवाएँ एक हैं किन्तु उनमें एक नैतिक और धार्मिक है, तो दूसरी अनैतिक और अधार्मिक। हम देखते हैं कि अनेकानेक लोग लौकिक एषणाओं की पूर्ति के लिए प्रभु भक्ति और सेवा करते हैं किन्तु उनकी वह सेवा धर्म का कारण न होकर अधर्म का कारण होती है । अत: साधनागत बाह्य विभिन्नताओं को न तो धार्मिकता का सर्वस्व मानना चाहिए और न उन पर इतना अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे पारस्परिक विभेद और भिन्नता की खाई और गहरी हो । वस्तुतः जब तक देश और कालगत भिन्नताएँ हैं, जब तक व्यक्ति की रूचि या स्वभावगत भिन्नताएँ हैं, तब तक साधनागत विभिन्नताएँ स्वाभाविक ही हैं। आचार्य हरिभद्र अपने ग्रन्थ योगदृष्टि समुच्चय में कहते हैं -
Jain Education International
धार्मिक सहिष्णुता और जैनधर्मः 7
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org