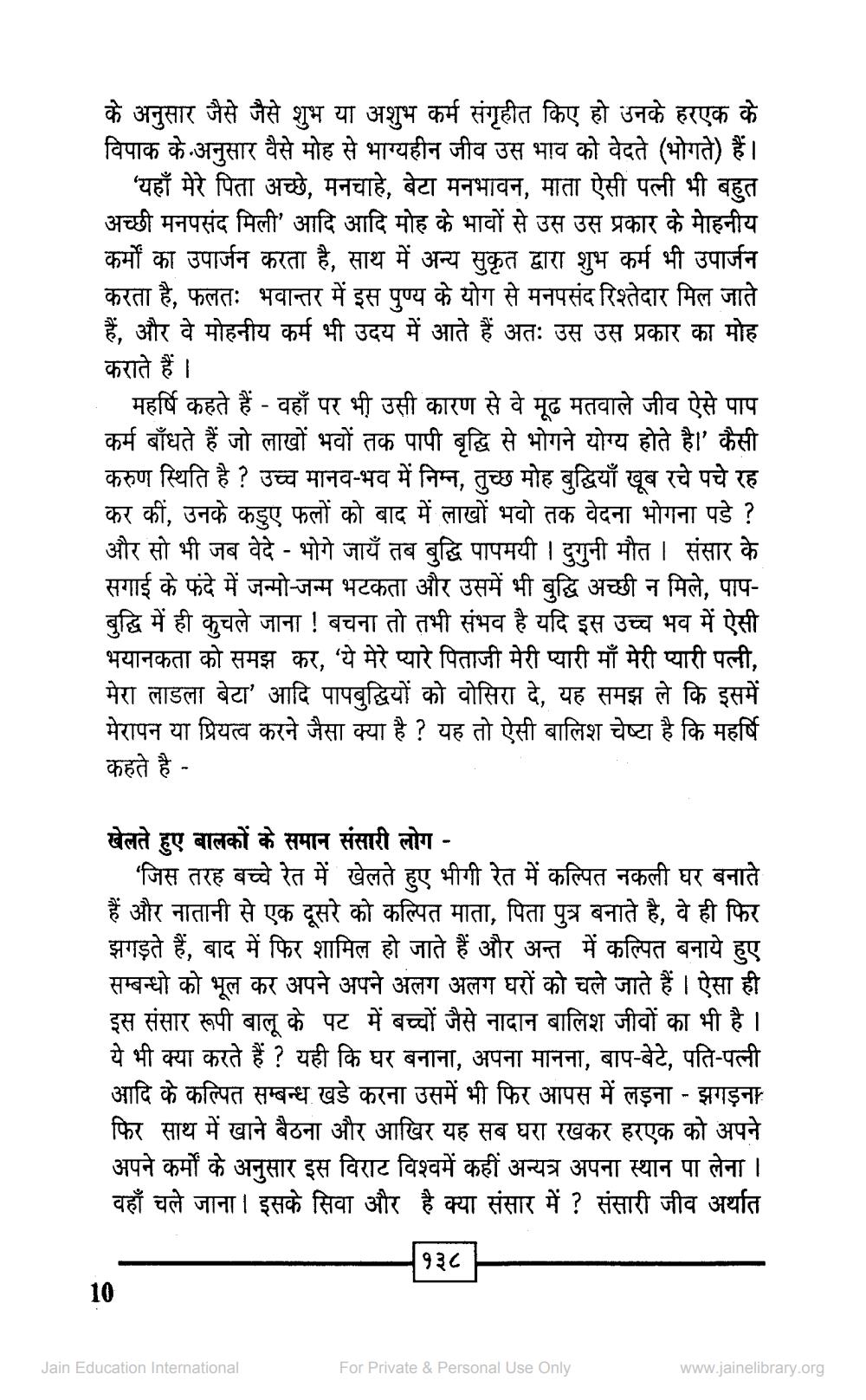________________
के अनुसार जैसे जैसे शुभ या अशुभ कर्म संगृहीत किए हो उनके हरएक के विपाक के अनुसार वैसे मोह से भाग्यहीन जीव उस भाव को वेदते (भोगते) हैं। __'यहाँ मेरे पिता अच्छे, मनचाहे, बेटा मनभावन, माता ऐसी पत्नी भी बहुत अच्छी मनपसंद मिली' आदि आदि मोह के भावों से उस उस प्रकार के मोहनीय कर्मों का उपार्जन करता है, साथ में अन्य सुकृत द्वारा शुभ कर्म भी उपार्जन करता है, फलतः भवान्तर में इस पुण्य के योग से मनपसंद रिश्तेदार मिल जाते हैं, और वे मोहनीय कर्म भी उदय में आते हैं अतः उस उस प्रकार का मोह कराते हैं। __महर्षि कहते हैं - वहाँ पर भी उसी कारण से वे मूढ मतवाले जीव ऐसे पाप कर्म बाँधते हैं जो लाखों भवों तक पापी बुद्धि से भोगने योग्य होते है।' कैसी करुण स्थिति है ? उच्च मानव-भव में निम्न, तुच्छ मोह बुद्धियाँ खूब रचे पचे रह कर की, उनके कडुए फलों को बाद में लाखों भवो तक वेदना भोगना पडे ?
और सो भी जब वेदे - भोगे जायँ तब बुद्धि पापमयी । दुगुनी मौत | संसार के सगाई के फंदे में जन्मो-जन्म भटकता और उसमें भी बुद्धि अच्छी न मिले, पापबुद्धि में ही कुचले जाना ! बचना तो तभी संभव है यदि इस उच्च भव में ऐसी भयानकता को समझ कर, 'ये मेरे प्यारे पिताजी मेरी प्यारी माँ मेरी प्यारी पत्नी, मेरा लाडला बेटा' आदि पापबुद्धियों को वोसिरा दे, यह समझ ले कि इसमें मेरापन या प्रियत्व करने जैसा क्या है ? यह तो ऐसी बालिश चेष्टा है कि महर्षि कहते है -
खेलते हुए बालकों के समान संसारी लोग -
'जिस तरह बच्चे रेत में खेलते हुए भीगी रेत में कल्पित नकली घर बनाते हैं और नातानी से एक दूसरे को कल्पित माता, पिता पुत्र बनाते है, वे ही फिर झगड़ते हैं, बाद में फिर शामिल हो जाते हैं और अन्त में कल्पित बनाये हुए सम्बन्धो को भूल कर अपने अपने अलग अलग घरों को चले जाते हैं । ऐसा ही इस संसार रूपी बालू के पट में बच्चों जैसे नादान बालिश जीवों का भी है । ये भी क्या करते हैं ? यही कि घर बनाना, अपना मानना, बाप-बेटे, पति-पत्नी
आदि के कल्पित सम्बन्ध खडे करना उसमें भी फिर आपस में लड़ना - झगड़ना फिर साथ में खाने बैठना और आखिर यह सब घरा रखकर हरएक को अपने अपने कर्मों के अनुसार इस विराट विश्वमें कहीं अन्यत्र अपना स्थान पा लेना। वहाँ चले जाना। इसके सिवा और है क्या संसार में ? संसारी जीव अर्थात
१३८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org