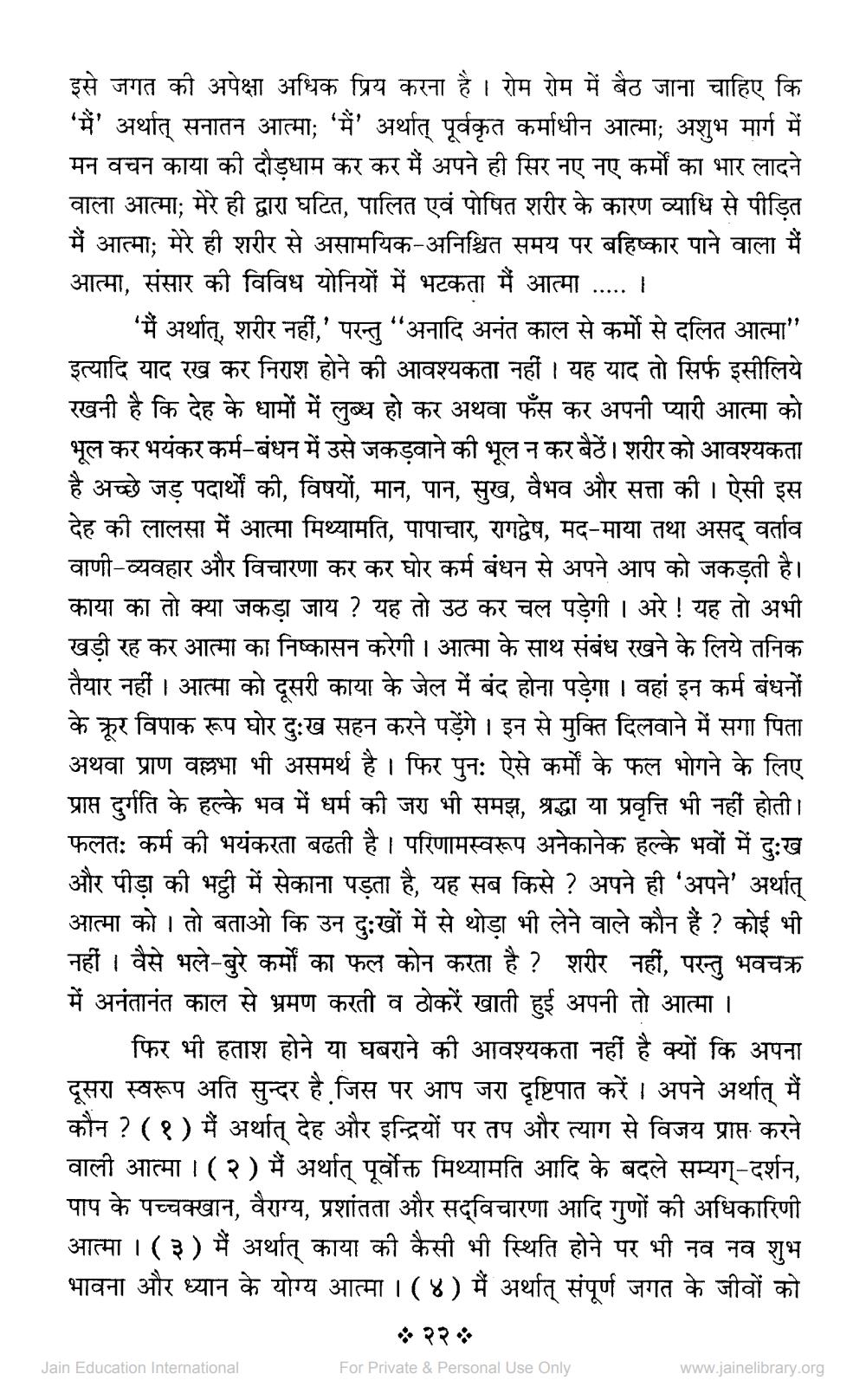________________
इसे जगत की अपेक्षा अधिक प्रिय करना है । रोम रोम में बैठ जाना चाहिए कि 'मैं' अर्थात् सनातन आत्मा; 'मैं' अर्थात् पूर्वकृत कर्माधीन आत्मा; अशुभ मार्ग में मन वचन काया की दौड़धाम कर कर मैं अपने ही सिर नए नए कर्मों का भार लादने वाला आत्मा; मेरे ही द्वारा घटित, पालित एवं पोषित शरीर के कारण व्याधि से पीड़ित मैं आत्मा; मेरे ही शरीर से असामयिक-अनिश्चित समय पर बहिष्कार पाने वाला मैं आत्मा, संसार की विविध योनियों में भटकता मैं आत्मा ..... ।
___ 'मैं अर्थात्, शरीर नहीं, परन्तु "अनादि अनंत काल से कर्मो से दलित आत्मा" इत्यादि याद रख कर निराश होने की आवश्यकता नहीं । यह याद तो सिर्फ इसीलिये रखनी है कि देह के धामों में लुब्ध हो कर अथवा फँस कर अपनी प्यारी आत्मा को भूल कर भयंकर कर्म-बंधन में उसे जकड़वाने की भूल न कर बैठें। शरीर को आवश्यकता है अच्छे जड़ पदार्थों की, विषयों, मान, पान, सुख, वैभव और सत्ता की । ऐसी इस देह की लालसा में आत्मा मिथ्यामति, पापाचार, रागद्वेष, मद-माया तथा असद् वर्ताव वाणी-व्यवहार और विचारणा कर कर घोर कर्म बंधन से अपने आप को जकड़ती है। काया का तो क्या जकड़ा जाय? यह तो उठ कर चल पड़ेगी । अरे ! यह तो अभी खड़ी रह कर आत्मा का निष्कासन करेगी। आत्मा के साथ संबंध रखने के लिये तनिक तैयार नहीं। आत्मा को दूसरी काया के जेल में बंद होना पडेगा । वहां इन कर्म बंधनों के क्रूर विपाक रूप घोर दुःख सहन करने पड़ेंगे। इन से मुक्ति दिलवाने में सगा पिता अथवा प्राण वल्लभा भी असमर्थ है। फिर पुनः ऐसे कर्मों के फल भोगने के लिए प्राप्त दुर्गति के हल्के भव में धर्म की जरा भी समझ, श्रद्धा या प्रवृत्ति भी नहीं होती। फलतः कर्म की भयंकरता बढती है। परिणामस्वरूप अनेकानेक हल्के भवों में दुःख
और पीड़ा की भट्ठी में सेकाना पड़ता है, यह सब किसे? अपने ही 'अपने' अर्थात् आत्मा को । तो बताओ कि उन दु:खों में से थोड़ा भी लेने वाले कौन हैं ? कोई भी नहीं । वैसे भले-बुरे कर्मों का फल कोन करता है ? शरीर नहीं, परन्तु भवचक्र में अनंतानंत काल से भ्रमण करती व ठोकरें खाती हुई अपनी तो आत्मा ।
फिर भी हताश होने या घबराने की आवश्यकता नहीं है क्यों कि अपना दूसरा स्वरूप अति सुन्दर है जिस पर आप जरा दृष्टिपात करें। अपने अर्थात् मैं कौन ? (१) मैं अर्थात् देह और इन्द्रियों पर तप और त्याग से विजय प्राप्त करने वाली आत्मा । (२) मैं अर्थात् पूर्वोक्त मिथ्यामति आदि के बदले सम्यग्-दर्शन, पाप के पच्चक्खान, वैराग्य, प्रशांतता और सद्विचारणा आदि गुणों की अधिकारिणी आत्मा । (३) मैं अर्थात् काया की कैसी भी स्थिति होने पर भी नव नव शुभ भावना और ध्यान के योग्य आत्मा । (४) मैं अर्थात् संपूर्ण जगत के जीवों को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org