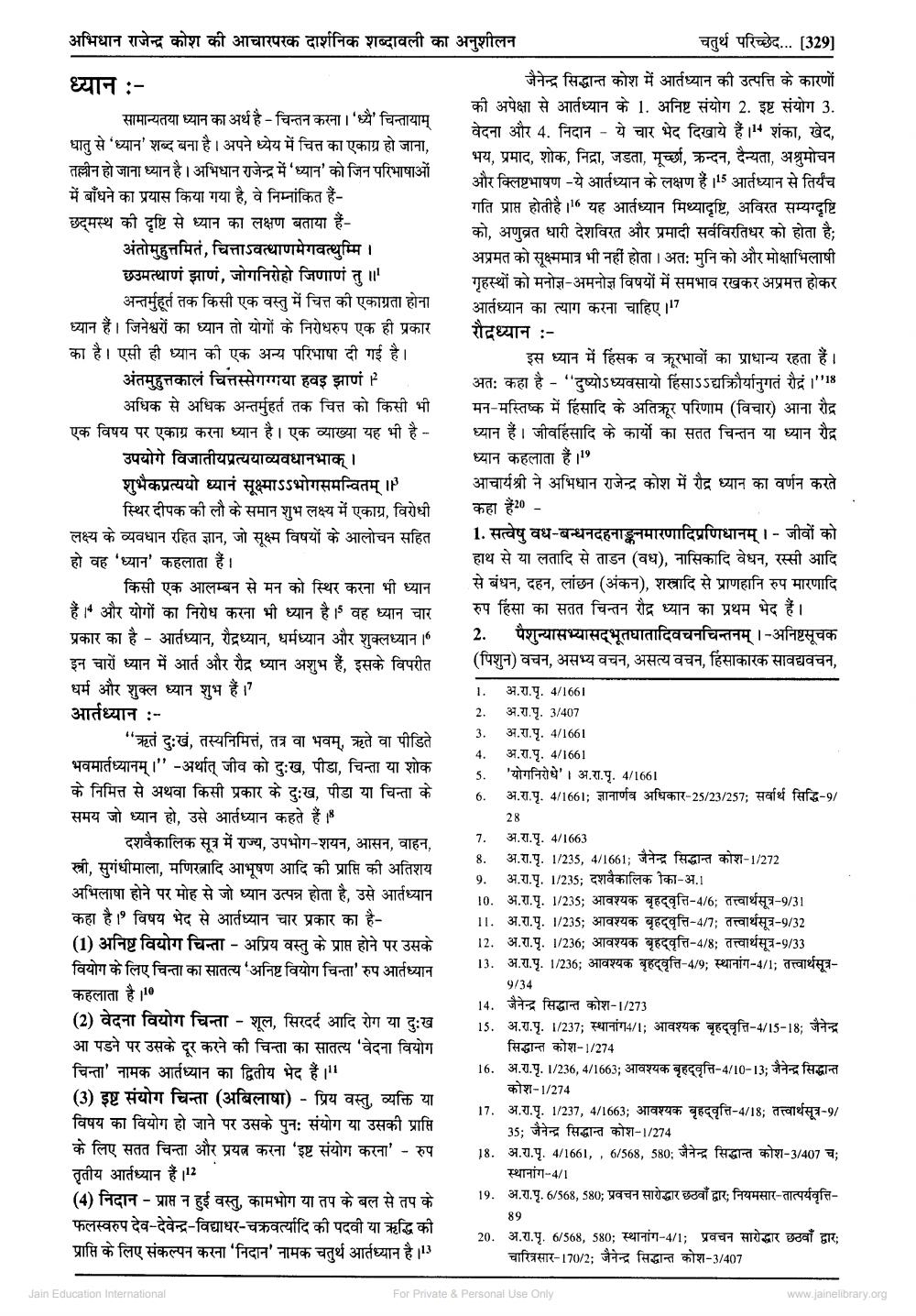________________
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन
चतुर्थ परिच्छेद... [329]
ध्यान :
सामान्यतया ध्यान का अर्थ है - चिन्तन करना। ध्यै' चिन्तायाम् धातु से 'ध्यान' शब्द बना है। अपने ध्येय में चित्त का एकाग्र हो जाना, तल्लीन हो जाना ध्यान है। अभिधान राजेन्द्र में 'ध्यान' को जिन परिभाषाओं में बाँधने का प्रयास किया गया है, वे निम्नांकित हैंछद्मस्थ की दृष्टि से ध्यान का लक्षण बताया हैं
अंतोमुहुत्तमितं, चित्ताऽवत्थाणमेगवत्थुम्मि। छउमत्थाणं झाणं, जोगनिरोहो जिणाणं तु ॥
अन्तर्मुहूर्त तक किसी एक वस्तु में चित्त की एकाग्रता होना ध्यान हैं। जिनेश्वरों का ध्यान तो योगों के निरोधरुप एक ही प्रकार का है। एसी ही ध्यान की एक अन्य परिभाषा दी गई है।
अंतमुहुत्तकालं चित्तस्सेगग्गया हवइ झाणं
अधिक से अधिक अन्तर्मुहर्त तक चित्त को किसी भी एक विषय पर एकाग्र करना ध्यान है। एक व्याख्या यह भी है -
उपयोगे विजातीयप्रत्ययाव्यवधानभाक् । शुभैकप्रत्ययो ध्यानं सूक्ष्माऽऽभोगसमन्वितम् ।
स्थिर दीपक की लौ के समान शुभ लक्ष्य में एकाग्र, विरोधी लक्ष्य के व्यवधान रहित ज्ञान, जो सूक्ष्म विषयों के आलोचन सहित हो वह 'ध्यान' कहलाता हैं।
किसी एक आलम्बन से मन को स्थिर करना भी ध्यान हैं। और योगों का निरोध करना भी ध्यान है। वह ध्यान चार प्रकार का है - आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान ।' इन चारों ध्यान में आर्त और रौद्र ध्यान अशुभ हैं, इसके विपरीत धर्म और शुक्ल ध्यान शुभ हैं।' आर्तध्यान :
"ऋतं दुःखं, तस्यनिमित्तं, तत्र वा भवम्, ऋते वा पीडिते भवमार्तध्यानम्।" -अर्थात् जीव को दुःख, पीडा, चिन्ता या शोक के निमित्त से अथवा किसी प्रकार के दुःख, पीडा या चिन्ता के समय जो ध्यान हो, उसे आर्तध्यान कहते हैं।
दशवैकालिक सूत्र में राज्य, उपभोग-शयन, आसन, वाहन, स्त्री, सुगंधीमाला, मणिरत्नादि आभूषण आदि की प्राप्ति की अतिशय अभिलाषा होने पर मोह से जो ध्यान उत्पन्न होता है, उसे आर्तध्यान कहा है।' विषय भेद से आर्तध्यान चार प्रकार का है(1) अनिष्ट वियोग चिन्ता - अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके वियोग के लिए चिन्ता का सातत्य अनिष्ट वियोग चिन्ता' रुप आर्तध्यान कहलाता है। (2) वेदना वियोग चिन्ता - शूल, सिरदर्द आदि रोग या दुःख आ पड़ने पर उसके दूर करने की चिन्ता का सातत्य 'वेदना वियोग चिन्ता' नामक आर्तध्यान का द्वितीय भेद हैं। (3) इष्ट संयोग चिन्ता (अबिलाषा) - प्रिय वस्तु, व्यक्ति या विषय का वियोग हो जाने पर उसके पुनः संयोग या उसकी प्राप्ति के लिए सतत चिन्ता और प्रयत्न करना 'इष्ट संयोग करना' - रुप तृतीय आर्तध्यान हैं। (4) निदान - प्राप्त न हुई वस्तु, कामभोग या तप के बल से तप के
या नाकेबल सेना फलस्वरुप देव-देवेन्द्र-विद्याधर-चक्रवर्त्यादि की पदवी या ऋद्धि की प्राप्ति के लिए संकल्पन करना 'निदान' नामक चतुर्थ आर्तध्यान है।
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश में आर्तध्यान की उत्पत्ति के कारणों की अपेक्षा से आर्तध्यान के 1. अनिष्ट संयोग 2. इष्ट संयोग 3. वेदना और 4. निदान - ये चार भेद दिखाये हैं। शंका, खेद, भय, प्रमाद, शोक, निद्रा, जडता, मूर्छा, क्रन्दन, दैन्यता, अश्रुमोचन
और क्लिष्टभाषण -ये आर्तध्यान के लक्षण हैं।15 आर्तध्यान से तिर्यंच गति प्राप्त होतीहै। यह आर्तध्यान मिथ्यादृष्टि, अविरत सम्यग्दृष्टि को, अणुव्रत धारी देशविरत और प्रमादी सर्वविरतिधर को होता है; अप्रमत को सूक्ष्ममात्र भी नहीं होता। अत: मुनि को और मोक्षाभिलाषी गृहस्थों को मनोज्ञ-अमनोज्ञ विषयों में समभाव रखकर अप्रमत्त होकर आर्तध्यान का त्याग करना चाहिए। रौद्रध्यान :
इस ध्यान में हिंसक व क्रूरभावों का प्राधान्य रहता हैं। अतः कहा है - "दुष्योऽध्यवसायो हिंसाऽऽद्यक्रिौर्यानुगतं रौद्रं ।''18 मन-मस्तिष्क में हिंसादि के अतिक्रूर परिणाम (विचार) आना रौद्र ध्यान हैं। जीवहिंसादि के कार्यो का सतत चिन्तन या ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता हैं। आचार्यश्री ने अभिधान राजेन्द्र कोश में रौद्र ध्यान का वर्णन करते कहा है-0 - 1. सत्वेषु वध-बन्धनदहनाङ्कनमारणादिप्रणिधानम्। - जीवों को हाथ से या लतादि से ताडन (वध), नासिकादि वेधन, रस्सी आदि से बंधन, दहन, लांछन (अंकन), शस्त्रादि से प्राणहानि रुप मारणादि रुप हिंसा का सतत चिन्तन रौद्र ध्यान का प्रथम भेद हैं। 2. पैशुन्यासभ्यासद्भूतघातादिवचनचिन्तनम् ।-अनिष्टसूचक (पिशुन) वचन, असभ्य वचन, असत्य वचन, हिंसाकारक सावधवचन,
1. अ.रा.पृ. 4/1661 2. अ.रा.पृ. 3/407 3. अ.रा.पृ. 4/1661
अ.रा.पृ. 4/1661 'योगनिरोधे'। अ.रा.पृ. 4/1661
अ.रा.पृ. 4/1661; ज्ञानार्णव अधिकार-25/23/257; सर्वार्थ सिद्धि-9/
28 7. अ.रा.पृ. 4/1663 8. अ.रा.पृ. 1/235, 4/1661; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-1/272 9. अ.रा.पृ. 1/235; दशवैकालिक का-अ.! 10. अ.रा.पृ. 1/235; आवश्यक बृहवृत्ति-4/6; तत्त्वार्थसूत्र-9/31 11. अ.रा.पृ. 1/235; आवश्यक बृहद्वृत्ति-4/7; तत्त्वार्थसूत्र-9/32 12. अ.रा.पृ. 1/236; आवश्यक बृहवृत्ति-4/8; तत्त्वार्थसूत्र-9/33 13. अ.रा.पृ. 1/236; आवश्यक बृहवृत्ति-4/9; स्थानांग-4/1; तत्त्वार्थसूत्र
9/34 14. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-1/273 15. अ.रा.पृ. 1/2379; स्थानांग4/1; आवश्यक बृहद्वृत्ति-4/15-18; जैनेन्द्र
सिद्धान्त कोश-1/274 अ.रा.पृ. 1/236, 4/1663; आवश्यक बृहवृत्ति-4/10-13; जैनेन्द्र सिद्धान्त
कोश-1/274 17. अ.रा.पृ. 1/237, 4/1663; आवश्यक बृहवृत्ति-4/18; तत्त्वार्थसूत्र-9/
35; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-1/274 18. अ.रा.पृ. 4/1661, , 6/568, 580; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-3/407 च;
स्थानांग-4/1 19. अ.रा.पृ. 6/568, 580; प्रवचन सारोद्धार छठवाँ द्वार; नियमसार-तात्पर्यवृत्ति
89 20. अ.रा.पृ. 6/568, 580; स्थानांग-4/1; प्रवचन सारोद्धार छठवाँ द्वार;
चारित्रसार-170/2; जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश-3/407
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org