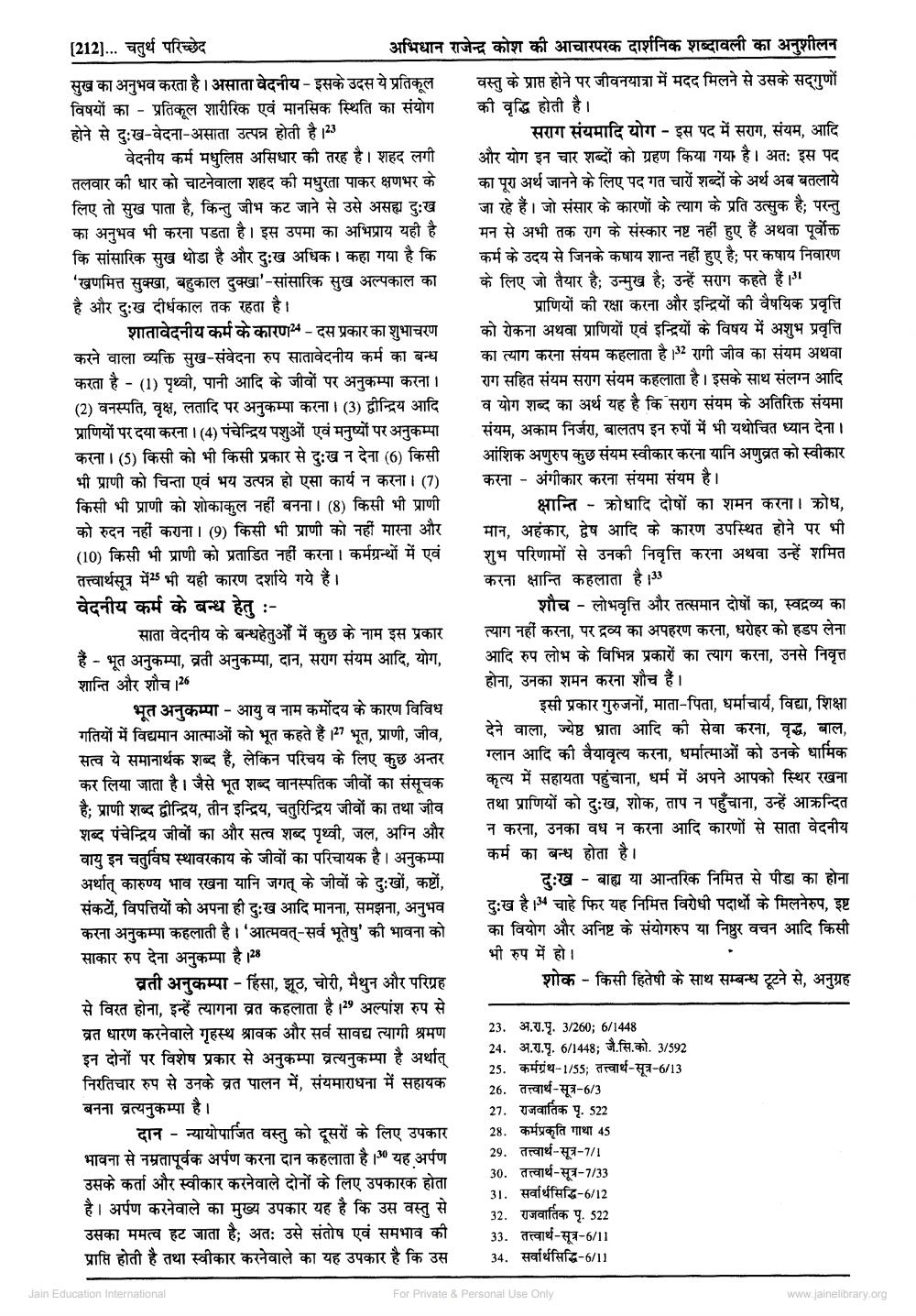________________
[212]... चतुर्थ परिच्छेद
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन सुख का अनुभव करता है। असाता वेदनीय- इसके उदस ये प्रतिकूल वस्तु के प्राप्त होने पर जीवनयात्रा में मदद मिलने से उसके सदगणों विषयों का - प्रतिकूल शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का संयोग की वृद्धि होती है।। होने से दुःख-वेदना-असाता उत्पन्न होती है।
सराग संयमादि योग - इस पद में सराग, संयम, आदि वेदनीय कर्म मधुलिप्त असिधार की तरह है। शहद लगी और योग इन चार शब्दों को ग्रहण किया गया है। अत: इस पद तलवार की धार को चाटनेवाला शहद की मधुरता पाकर क्षणभर के का पूरा अर्थ जानने के लिए पद गत चारों शब्दों के अर्थ अब बतलाये लिए तो सुख पाता है, किन्तु जीभ कट जाने से उसे असह्य दुःख जा रहे हैं। जो संसार के कारणों के त्याग के प्रति उत्सुक है; परन्तु का अनुभव भी करना पडता है। इस उपमा का अभिप्राय यही है मन से अभी तक राग के संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं अथवा पूर्वोक्त कि सांसारिक सुख थोडा है और दुःख अधिक। कहा गया है कि कर्म के उदय से जिनके कषाय शान्त नहीं हुए है; पर कषाय निवारण 'खणमित्त सुक्खा, बहुकाल दुक्खा'-सांसारिक सुख अल्पकाल का के लिए जो तैयार है; उन्मुख है; उन्हें सराग कहते हैं।" है और दुःख दीर्धकाल तक रहता है।
प्राणियों की रक्षा करना और इन्द्रियों की वैषयिक प्रवृत्ति शातावेदनीय कर्म के कारण - दस प्रकार का शुभाचरण को रोकना अथवा प्राणियों एवं इन्द्रियों के विषय में अशुभ प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति सुख-संवेदना रुप सातावेदनीय कर्म का बन्ध का त्याग करना संयम कहलाता है। रागी जीव का संयम अथवा करता है - (1) पृथ्वी, पानी आदि के जीवों पर अनुकम्पा करना। राग सहित संयम सराग संयम कहलाता है। इसके साथ संलग्न आदि (2) वनस्पति, वृक्ष, लतादि पर अनुकम्पा करना । (3) द्वीन्द्रिय आदि व योग शब्द का अर्थ यह है कि सराग संयम के अतिरिक्त संयमा प्राणियों पर दया करना । (4) पंचेन्द्रिय पशुओं एवं मनुष्यों पर अनुकम्पा संयम, अकाम निर्जरा, बालतप इन रुपों में भी यथोचित ध्यान देना । करना । (5) किसी को भी किसी प्रकार से दुःख न देना (6) किसी आंशिक अणुरुप कुछ संयम स्वीकार करना यानि अणुव्रत को स्वीकार भी प्राणी को चिन्ता एवं भय उत्पन्न हो एसा कार्य न करना। (7) करना - अंगीकार करना संयमा संयम है। किसी भी प्राणी को शोकाकुल नहीं बनना। (8) किसी भी प्राणी
क्षान्ति - क्रोधादि दोषों का शमन करना। क्रोध, को रुदन नहीं कराना। (9) किसी भी प्राणी को नहीं मारना और मान, अहंकार, द्वेष आदि के कारण उपस्थित होने पर भी (10) किसी भी प्राणी को प्रताडित नहीं करना। कर्मग्रन्थों में एवं शुभ परिणामों से उनकी निवृत्ति करना अथवा उन्हें शमित तत्त्वार्थसूत्र में भी यही कारण दर्शाये गये हैं।
करना शान्ति कहलाता है। वेदनीय कर्म के बन्ध हेतु :
शौच - लोभवृत्ति और तत्समान दोषों का, स्वद्रव्य का साता वेदनीय के बन्धहेतुओं में कुछ के नाम इस प्रकार त्याग नहीं करना, पर द्रव्य का अपहरण करना, धरोहर को हडप लेना हैं - भूत अनुकम्पा, व्रती अनुकम्पा, दान, सराग संयम आदि, योग, आदि रुप लोभ के विभिन्न प्रकारों का त्याग करना, उनसे निवृत्त शान्ति और शौच ।26
होना, उनका शमन करना शौच है। भूत अनुकम्पा - आयु व नाम कर्मोदय के कारण विविध
इसी प्रकार गुरुजनों, माता-पिता, धर्माचार्य, विद्या, शिक्षा गतियों में विद्यमान आत्माओं को भूत कहते हैं। भूत, प्राणी, जीव, देने वाला, ज्येष्ठ भ्राता आदि की सेवा करना, वृद्ध, बाल, सत्व ये समानार्थक शब्द हैं, लेकिन परिचय के लिए कुछ अन्तर
ग्लान आदि की वैयावृत्य करना, धर्मात्माओं को उनके धार्मिक कर लिया जाता है। जैसे भूत शब्द वानस्पतिक जीवों का संसूचक कृत्य में सहायता पहुंचाना, धर्म में अपने आपको स्थिर रखना है; प्राणी शब्द द्वीन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों का तथा जीव तथा प्राणियों को दुःख, शोक, ताप न पहुँचाना, उन्हें आक्रन्दित शब्द पंचेन्द्रिय जीवों का और सत्व शब्द पृथ्वी, जल, अग्नि और न करना, उनका वध न करना आदि कारणों से साता वेदनीय वायु इन चतुर्विध स्थावरकाय के जीवों का परिचायक है। अनुकम्पा कर्म का बन्ध होता है। अर्थात् कारुण्य भाव रखना यानि जगत् के जीवों के दुःखों, कष्टों,
दुःख - बाह्य या आन्तरिक निमित्त से पीडा का होना संकट, विपत्तियों को अपना ही दुःख आदि मानना, समझना, अनुभव दुःख है। चाहे फिर यह निमित्त विरोधी पदार्थो के मिलनेरुप, इष्ट करना अनुकम्पा कहलाती है। 'आत्मवत्-सर्व भूतेषु' की भावना को का वियोग और अनिष्ट के संयोगरुप या निष्ठुर वचन आदि किसी साकार रुप देना अनुकम्पा है।28
भी रुप में हो। व्रती अनुकम्पा - हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह
शोक - किसी हितेषी के साथ सम्बन्ध टूटने से, अनुग्रह से विरत होना, इन्हें त्यागना व्रत कहलाता है। अल्पांश रुप से व्रत धारण करनेवाले गृहस्थ श्रावक और सर्व सावद्य त्यागी श्रमण
23. अ.रा.पृ. 3/260; 6/1448 इन दोनों पर विशेष प्रकार से अनुकम्पा व्रत्यनुकम्पा है अर्थात्
24. अ.रा.पृ. 6/1448; जै.सि.को. 3/592
25. कर्मग्रंथ-1/55; तत्त्वार्थ-सूत्र-6/13 निरतिचार रुप से उनके व्रत पालन में, संयमाराधना में सहायक
26. तत्त्वार्थ-सूत्र-6/3 बनना व्रत्यनुकम्पा है।
27. राजवार्तिक पृ. 522 दान - न्यायोपाजित वस्तु को दूसरों के लिए उपकार 28. कर्मप्रकृति गाथा 45 भावना से नम्रतापूर्वक अर्पण करना दान कहलाता है। यह अर्पण
29. तत्त्वार्थ-सूत्र-7/1 उसके कर्ता और स्वीकार करनेवाले दोनों के लिए उपकारक होता
30. तत्त्वार्थ-सूत्र-7/33
31. सर्वार्थसिद्धि-6/12 है। अर्पण करनेवाले का मुख्य उपकार यह है कि उस वस्तु से
32. राजवार्तिक पृ. 522 उसका ममत्व हट जाता है; अतः उसे संतोष एवं समभाव की
33. तत्त्वार्थ-सूत्र-6/11 प्राप्ति होती है तथा स्वीकार करनेवाले का यह उपकार है कि उस 34. सर्वार्थसिद्धि-6/11
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org