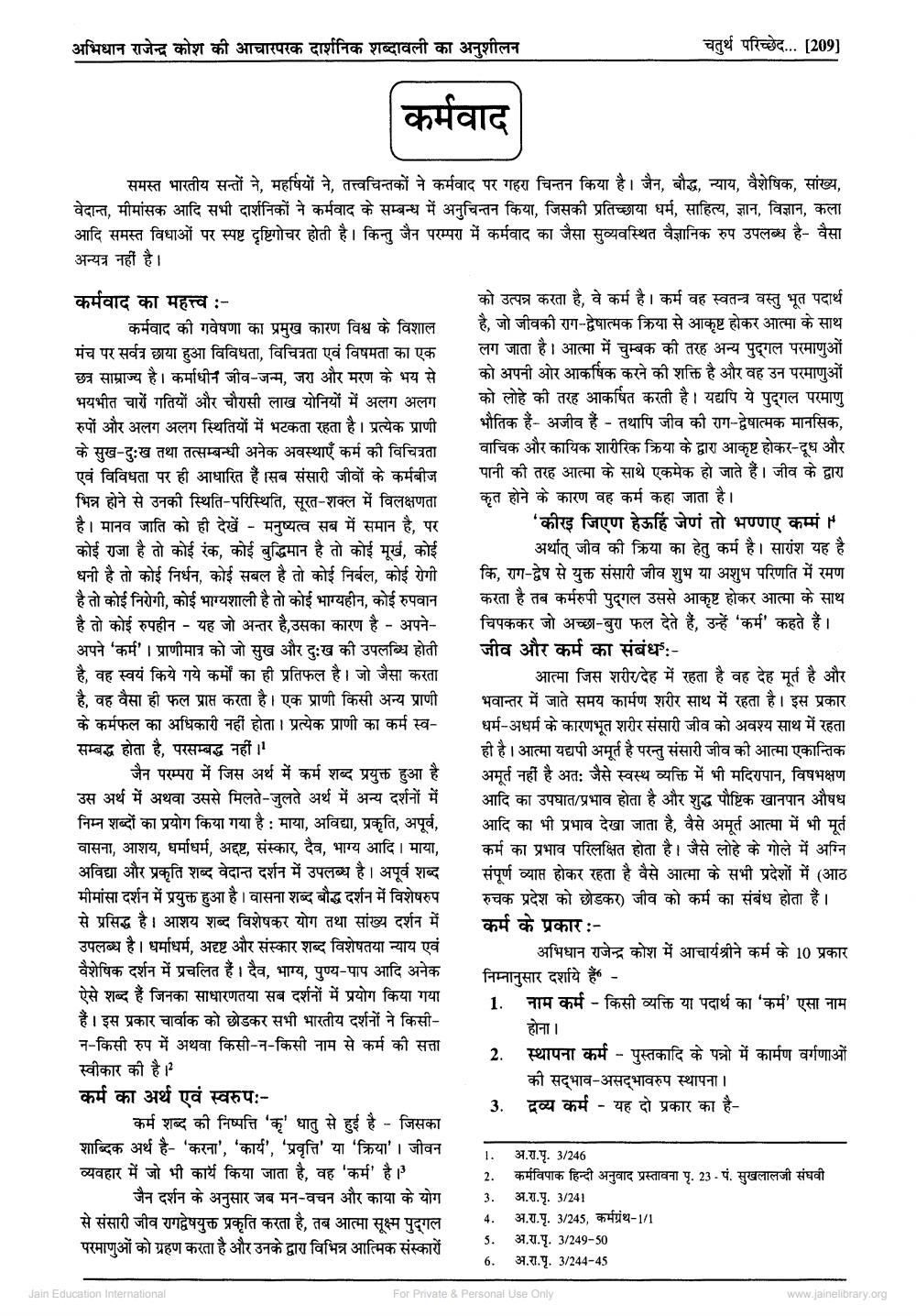________________
अभिधान राजेन्द्र कोश की आचारपरक दार्शनिक शब्दावली का अनुशीलन
चतुर्थ परिच्छेद... [209]
कर्मवाद
समस्त भारतीय सन्तों ने, महर्षियों ने, तत्त्वचिन्तकों ने कर्मवाद पर गहरा चिन्तन किया है। जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदान्त, मीमांसक आदि सभी दार्शनिकों ने कर्मवाद के सम्बन्ध में अनुचिन्तन किया, जिसकी प्रतिच्छाया धर्म, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, कला आदि समस्त विधाओं पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। किन्तु जैन परम्परा में कर्मवाद का जैसा सुव्यवस्थित वैज्ञानिक रुप उपलब्ध है- वैसा अन्यत्र नहीं है।
अर्थात
कर्मवाद का महत्त्व :
कर्मवाद की गवेषणा का प्रमुख कारण विश्व के विशाल मंच पर सर्वत्र छाया हुआ विविधता, विचित्रता एवं विषमता का एक छत्र साम्राज्य है। कर्माधीन जीव-जन्म, जरा और मरण के भय से भयभीत चारों गतियों और चौरासी लाख योनियों में अलग अलग रुपों और अलग अलग स्थितियों में भटकता रहता है। प्रत्येक प्राणी के सुख-दुःख तथा तत्सम्बन्धी अनेक अवस्थाएँ कर्म की विचित्रता एवं विविधता पर ही आधारित है।सब संसारी जीवों के कर्मबीज भिन्न होने से उनकी स्थिति-परिस्थिति, सूरत-शक्ल में विलक्षणता है। मानव जाति को ही देखें - मनुष्यत्व सब में समान है, पर कोई राजा है तो कोई रंक, कोई बुद्धिमान है तो कोई मूर्ख, कोई धनी है तो कोई निर्धन, कोई सबल है तो कोई निर्बल, कोई रोगी है तो कोई निरोगी, कोई भाग्यशाली है तो कोई भाग्यहीन, कोई रुपवान है तो कोई रुपहीन - यह जो अन्तर है,उसका कारण है - अपनेअपने 'कर्म' । प्राणीमात्र को जो सुख और दुःख की उपलब्धि होती। है, वह स्वयं किये गये कर्मों का ही प्रतिफल है। जो जैसा करता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। एक प्राणी किसी अन्य प्राणी के कर्मफल का अधिकारी नहीं होता। प्रत्येक प्राणी का कर्म स्वसम्बद्ध होता है, परसम्बद्ध नहीं।
जैन परम्परा में जिस अर्थ में कर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है उस अर्थ में अथवा उससे मिलते-जुलते अर्थ में अन्य दर्शनों में निम्न शब्दों का प्रयोग किया गया है : माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वासना, आशय, धर्माधर्म, अद्दष्ट, संस्कार, दैव, भाग्य आदि । माया, अविद्या और प्रकृति शब्द वेदान्त दर्शन में उपलब्ध है। अपूर्व शब्द मीमांसा दर्शन में प्रयुक्त हुआ है। वासना शब्द बौद्ध दर्शन में विशेषरुप से प्रसिद्ध है। आशय शब्द विशेषकर योग तथा सांख्य दर्शन में उपलब्ध है। धर्माधर्म, अदृष्ट और संस्कार शब्द विशेषतया न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में प्रचलित हैं। दैव, भाग्य, पुण्य-पाप आदि अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका साधारणतया सब दर्शनों में प्रयोग किया गया हैं। इस प्रकार चार्वाक को छोडकर सभी भारतीय दर्शनों ने किसीन-किसी रुप में अथवा किसी-न-किसी नाम से कर्म की सत्ता स्वीकार की है। कर्म का अर्थ एवं स्वरुपः
कर्म शब्द की निष्पत्ति 'कृ' धातु से हुई है - जिसका शाब्दिक अर्थ है- 'करना', 'कार्य', 'प्रवृत्ति' या 'क्रिया' । जीवन व्यवहार में जो भी कार्य किया जाता है, वह 'कर्म' है।
जैन दर्शन के अनुसार जब मन-वचन और काया के योग से संसारी जीव रागद्वेषयुक्त प्रकृति करता है, तब आत्मा सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता है और उनके द्वारा विभिन्न आत्मिक संस्कारों
को उत्पन्न करता है, वे कर्म है। कर्म वह स्वतन्त्र वस्तु भूत पदार्थ है, जो जीवकी राग-द्वेषात्मक क्रिया से आकृष्ट होकर आत्मा के साथ लग जाता है। आत्मा में चुम्बक की तरह अन्य पुद्गल परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षिक करने की शक्ति है और वह उन परमाणुओं को लोहे की तरह आकर्षित करती है। यद्यपि ये पुद्गल परमाणु भौतिक हैं- अजीव हैं - तथापि जीव की राग-द्वेषात्मक मानसिक, वाचिक और कायिक शारीरिक क्रिया के द्वारा आकृष्ट होकर-दूध और पानी की तरह आत्मा के साथे एकमेक हो जाते हैं। जीव के द्वारा कृत होने के कारण वह कर्म कहा जाता है।
'कीरइ जिएण हेऊहिं जेणं तो भण्णए कम्मं । ____ अर्थात् जीव की क्रिया का हेतु कर्म है। सारांश यह है कि, राग-द्वेष से युक्त संसारी जीव शुभ या अशुभ परिणति में रमण करता है तब कर्मरुपी पुद्गल उससे आकृष्ट होकर आत्मा के साथ चिपककर जो अच्छा-बुरा फल देते हैं, उन्हें 'कर्म' कहते हैं। जीव और कर्म का संबंध:
आत्मा जिस शरीर/देह में रहता है वह देह मूर्त है और भवान्तर में जाते समय कार्मण शरीर साथ में रहता है। इस प्रकार धर्म-अधर्म के कारणभूत शरीर संसारी जीव को अवश्य साथ में रहता ही है। आत्मा यद्यपी अमूर्त है परन्तु संसारी जीव की आत्मा एकान्तिक अमूर्त नहीं है अत: जैसे स्वस्थ व्यक्ति में भी मदिरापान, विषभक्षण आदि का उपघात/प्रभाव होता है और शुद्ध पौष्टिक खानपान औषध आदि का भी प्रभाव देखा जाता है, वैसे अमूर्त आत्मा में भी मूर्त कर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। जैसे लोहे के गोले में अग्नि संपूर्ण व्याप्त होकर रहता है वैसे आत्मा के सभी प्रदेशों में (आठ रुचक प्रदेश को छोडकर) जीव को कर्म का संबंध होता हैं। कर्म के प्रकार :
अभिधान राजेन्द्र कोश में आचार्यश्रीने कर्म के 10 प्रकार निम्नानुसार दर्शाये हैं - 1. नाम कर्म - किसी व्यक्ति या पदार्थ का 'कर्म' एसा नाम
होना। स्थापना कर्म - पुस्तकादि के पन्नो में कार्मण वर्गणाओं
की सद्भाव-असद्भावरुप स्थापना । 3. दव्य कर्म - यह दो प्रकार का है
कास
1. अ.रा.पृ. 3/246 2. कर्मविपाक हिन्दी अनुवाद प्रस्तावना पृ. 23 - पं. सुखलालजी संघवी 3. अ.रा.पृ. 3/241 4. अ.रा.पृ. 3/245, कर्मग्रंथ-1/1 5. अ.रा.पृ. 3/249-50 6. अ.रा.पृ. 3/244-45
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org