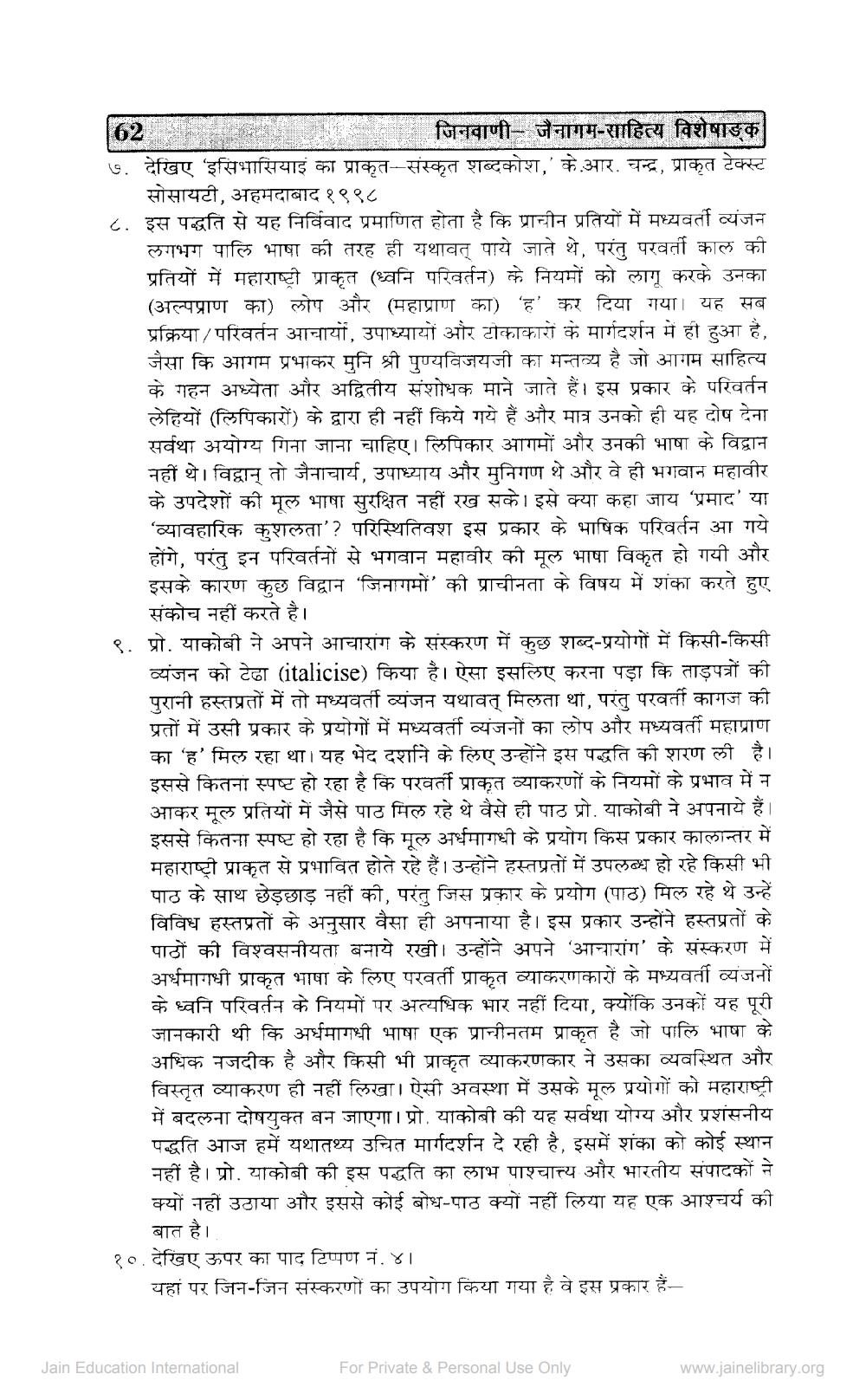________________
62
७. देखिए 'इसिभासियाइं का प्राकृत सोसायटी, अहमदाबाद १९९८
८. इस पद्धति से यह निर्विवाद प्रमाणित होता है कि प्राचीन प्रतियों में मध्यवर्ती व्यंजन लगभग पालि भाषा की तरह ही यथावत् पाये जाते थे, परंतु परवर्ती काल की प्रतियों में महाराष्ट्री प्राकृत (ध्वनि परिवर्तन) के नियमों को लागू करके उनका (अल्पप्राण का) लोप और (महाप्राण का) 'ह' कर दिया गया। यह सब प्रक्रिया / परिवर्तन आचार्यो, उपाध्यायों और टोकाकारों के मार्गदर्शन में ही हुआ है, जैसा कि आगम प्रभाकर मुनि श्री पुण्यविजयजी का मन्तव्य है जो आगम साहित्य के गहन अध्येता और अद्वितीय संशोधक माने जाते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन लेहियों (लिपिकारों) के द्वारा ही नहीं किये गये हैं और मात्र उनको ही यह दोष देना सर्वथा अयोग्य गिना जाना चाहिए। लिपिकार आगमों और उनकी भाषा के विद्वान नहीं थे। विद्वान् तो जैनाचार्य, उपाध्याय और मुनिगण थे और वे ही भगवान महावीर के उपदेशों की मूल भाषा सुरक्षित नहीं रख सके। इसे क्या कहा जाय 'प्रमाद' या 'व्यावहारिक कुशलता' ? परिस्थितिवश इस प्रकार के भाषिक परिवर्तन आ गये होंगे, परंतु इन परिवर्तनों से भगवान महावीर की मूल भाषा विकृत हो गयी और इसके कारण कुछ विद्वान 'जिनागमों' की प्राचीनता के विषय में शंका करते हुए संकोच नहीं करते है ।
• जिनवाणी- जैनागम-साहित्य विशेषाङ्क संस्कृत शब्दकोश, के. आर. चन्द्र, प्राकृत टेक्स्ट
९. प्रो. याकोबी ने अपने आचारांग के संस्करण में कुछ शब्द प्रयोगों में किसी-किसी व्यंजन को टेढा (italicise) किया है। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि ताड़पत्रों की पुरानी हस्तप्रतों में तो मध्यवर्ती व्यंजन यथावत् मिलता था, परंतु परवर्ती कागज की प्रतों में उसी प्रकार के प्रयोगों में मध्यवर्ती व्यंजनों का लोप और मध्यवर्ती महाप्राण का 'ह' मिल रहा था। यह भेद दर्शाने के लिए उन्होंने इस पद्धति की शरण ली है। इससे कितना स्पष्ट हो रहा है कि परवर्ती प्राकृत व्याकरणों के नियमों के प्रभाव में न आकर मूल प्रतियों में जैसे पाठ मिल रहे थे वैसे ही पाठ प्रो. याकोबी ने अपनाये हैं। इससे कितना स्पष्ट हो रहा है कि मूल अर्धमागधी के प्रयोग किस प्रकार कालान्तर में महाराष्ट्री प्राकृत से प्रभावित होते रहे हैं। उन्होंने हस्तप्रतों में उपलब्ध हो रहे किसी भी पाठ के साथ छेड़छाड़ नहीं की, परंतु जिस प्रकार के प्रयोग (पाठ) मिल रहे थे उन्हें विविध हस्तप्रतों के अनुसार वैसा ही अपनाया है। इस प्रकार उन्होंने हस्तप्रतों के पाठों की विश्वसनीयता बनाये रखी। उन्होंने अपने 'आचारांग' के संस्करण में अर्धमागधी प्राकृत भाषा के लिए परवर्ती प्राकृत व्याकरणकारों के मध्यवर्ती व्यंजनों के ध्वनि परिवर्तन के नियमों पर अत्यधिक भार नहीं दिया, क्योंकि उनकों यह पूरी जानकारी थी कि अर्धमागधी भाषा एक प्राचीनतम प्राकृत है जो पालि भाषा के अधिक नजदीक है और किसी भी प्राकृत व्याकरणकार ने उसका व्यवस्थित और विस्तृत व्याकरण ही नहीं लिखा। ऐसी अवस्था में उसके मूल प्रयोगों को महाराष्ट्री में बदलना दोषयुक्त बन जाएगा। प्रो. याकोबी की यह सर्वथा योग्य और प्रशंसनीय पद्धति आज हमें यथातथ्य उचित मार्गदर्शन दे रही है, इसमें शंका को कोई स्थान नहीं है। प्रो. याकोबी की इस पद्धति का लाभ पाश्चात्त्य और भारतीय संपादकों ने क्यों नहीं उठाया और इससे कोई बोध-पाठ क्यों नहीं लिया यह एक आश्चर्य की बात है।
१०. देखिए ऊपर का पाद टिप्पण नं. ४ ।
यहां पर जिन-जिन संस्करणों का उपयोग किया गया है वे इस प्रकार
हैं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org