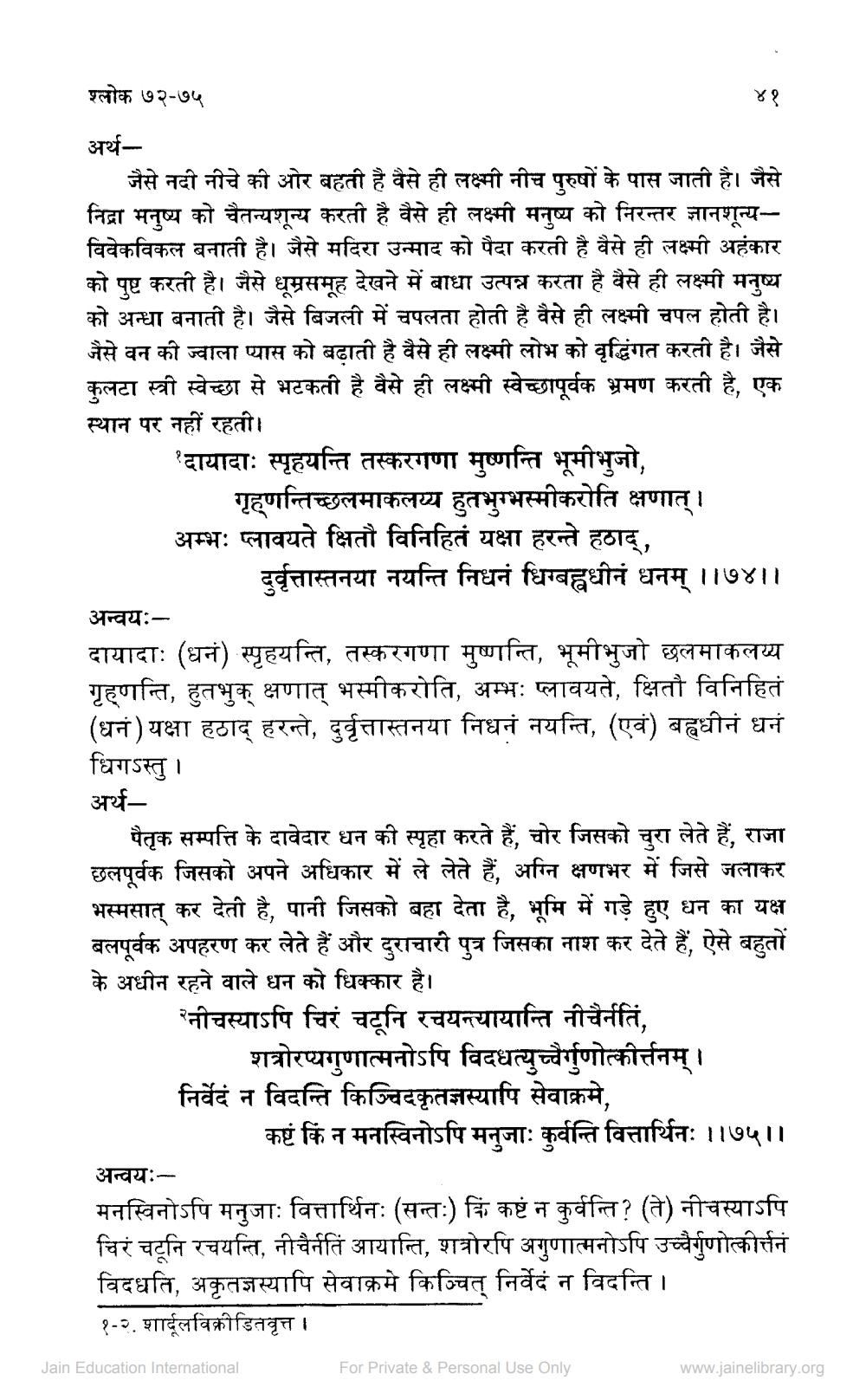________________
श्लोक ७२-७५
अर्थ
जैसे नदी नीचे की ओर बहती है वैसे ही लक्ष्मी नीच पुरुषों के पास जाती है। जैसे निद्रा मनुष्य को चैतन्यशून्य करती है वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को निरन्तर ज्ञानशून्यविवेकविकल बनाती है। जैसे मदिरा उन्माद को पैदा करती है वैसे ही लक्ष्मी अहंकार को पुष्ट करती है। जैसे धूम्रसमूह देखने में बाधा उत्पन्न करता है वैसे ही लक्ष्मी मनुष्य को अन्धा बनाती है । जैसे बिजली में चपलता होती है वैसे ही लक्ष्मी चपल होती है। जैसे वन की ज्वाला प्यास को बढ़ाती है वैसे ही लक्ष्मी लोभ को वृद्धिंगत करती है । जैसे कुलटा स्त्री स्वेच्छा से भटकती है वैसे ही लक्ष्मी स्वेच्छापूर्वक भ्रमण करती है, एक स्थान पर नहीं रहती ।
'दायादाः स्पृहयन्ति तस्करगणा मुष्णन्ति भूमीभुजो,
गृह्णन्तिच्छलमाकलय्य हुतभुग्भस्मीकरोति क्षणात् । अम्भः प्लावयते क्षितौ विनिहितं यक्षा हरन्ते हठाद्,
४१
दुर्वृत्तास्तनया नयन्ति निधनं धिग्बधीनं धनम् ।।७४।।
अन्वयः -
दायादाः ( धनं) स्पृहयन्ति, तस्करगणा मुष्णन्ति, भूमीभुजो छलमाकलय्य गृह्णन्ति, हुतभुक् क्षणात् भस्मीकरोति, अम्भः प्लावयते, क्षितौ विनिहितं ( धनं ) यक्षा हठाद् हरन्ते, दुर्वृत्तास्तनया निधनं नयन्ति ( एवं ) बह्वधीनं धनं धिगस्तु ।
अर्थ
पैतृक सम्पत्ति के दावेदार धन की स्पृहा करते हैं, चोर जिसको चुरा लेते हैं, राजा छलपूर्वक जिसको अपने अधिकार में ले लेते हैं, अग्नि क्षणभर में जिसे जलाकर भस्मसात् कर देती है, पानी जिसको बहा देता है, भूमि में गड़े हुए धन का यक्ष बलपूर्वक अपहरण कर लेते हैं और दुराचारी पुत्र जिसका नाश कर देते हैं, ऐसे बहुतों के अधीन रहने वाले धन को धिक्कार है।
नीचस्यापि चिरं चटूनि रचयन्त्यायान्ति नीचैर्नतिं, शत्रोरप्यगुणात्मनोऽपि विदधत्युच्चैर्गुणोत्कीर्त्तनम् । निर्वेदं न विदन्ति किञ्चिदकृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे,
Jain Education International
कष्टं किं न मनस्विनोऽपि मनुजाः कुर्वन्ति वित्तार्थिनः ।। ७५ ।।
अन्वयः -
मनस्विनोऽपि
'मनुजाः वित्तार्थिनः ( सन्तः ) किं कष्टं न कुर्वन्ति? (ते) नीचस्याऽपि चिरं चटूनि रचयन्ति, नीचैर्नतिं आयान्ति, शत्रोरपि अगुणात्मनोऽपि उच्चैर्गुणोत्कीर्त्तनं विदधति, अकृतज्ञस्यापि सेवाक्रमे किञ्चित् निर्वेदं न विदन्ति ।
१२. शार्दूलविक्रीडितवृत्त ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org