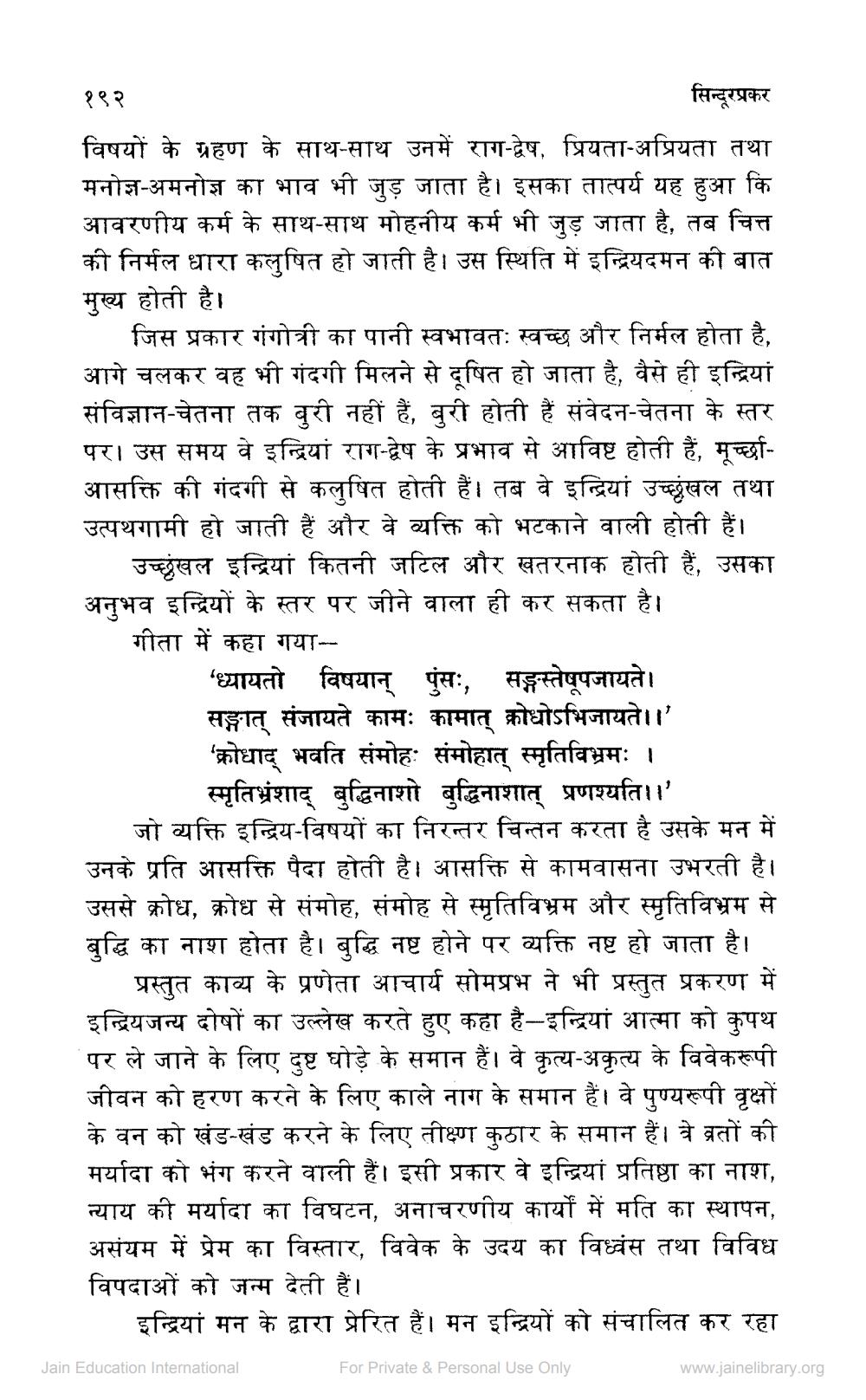________________
१९२
सिन्दूरप्रकर
विषयों के ग्रहण के साथ-साथ उनमें राग-द्वेष, प्रियता-अप्रियता तथा मनोज्ञ-अमनोज्ञ का भाव भी जुड़ जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आवरणीय कर्म के साथ-साथ मोहनीय कर्म भी जुड़ जाता है, तब चित्त की निर्मल धारा कलुषित हो जाती है। उस स्थिति में इन्द्रियदमन की बात मुख्य होती है।
जिस प्रकार गंगोत्री का पानी स्वभावतः स्वच्छ और निर्मल होता है, आगे चलकर वह भी गंदगी मिलने से दूषित हो जाता है, वैसे ही इन्द्रियां संविज्ञान-चेतना तक बरी नहीं हैं, बुरी होती हैं संवेदन-चेतना के स्तर पर। उस समय वे इन्द्रियां राग-द्वेष के प्रभाव से आविष्ट होती हैं, मुर्छाआसक्ति की गंदगी से कलुषित होती हैं। तब वे इन्द्रियां उच्छंखल तथा उत्पथगामी हो जाती हैं और वे व्यक्ति को भटकाने वाली होती हैं।
उच्छंखल इन्द्रियां कितनी जटिल और खतरनाक होती हैं, उसका अनुभव इन्द्रियों के स्तर पर जीने वाला ही कर सकता है। गीता में कहा गया
'ध्यायतो विषयान् पुंसः, सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते।।' 'क्रोधाद् भवति संमोहः संमोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।।' जो व्यक्ति इन्द्रिय-विषयों का निरन्तर चिन्तन करता है उसके मन में उनके प्रति आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामवासना उभरती है। उससे क्रोध, क्रोध से संमोह, संमोह से स्मृतिविभ्रम और स्मृतिविभ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है।
प्रस्तुत काव्य के प्रणेता आचार्य सोमप्रभ ने भी प्रस्तुत प्रकरण में इन्द्रियजन्य दोषों का उल्लेख करते हुए कहा है-इन्द्रियां आत्मा को कुपथ पर ले जाने के लिए दुष्ट घोड़े के समान हैं। वे कृत्य-अकृत्य के विवेकरूपी जीवन को हरण करने के लिए काले नाग के समान हैं। वे पुण्यरूपी वृक्षों के वन को खंड-खंड करने के लिए तीक्ष्ण कुठार के समान हैं। वे व्रतों की मर्यादा को भंग करने वाली हैं। इसी प्रकार वे इन्द्रियां प्रतिष्ठा का नाश, न्याय की मर्यादा का विघटन, अनाचरणीय कार्यों में मति का स्थापन, असंयम में प्रेम का विस्तार, विवेक के उदय का विध्वंस तथा विविध विपदाओं को जन्म देती हैं।
इन्द्रियां मन के द्वारा प्रेरित हैं। मन इन्द्रियों को संचालित कर रहा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org