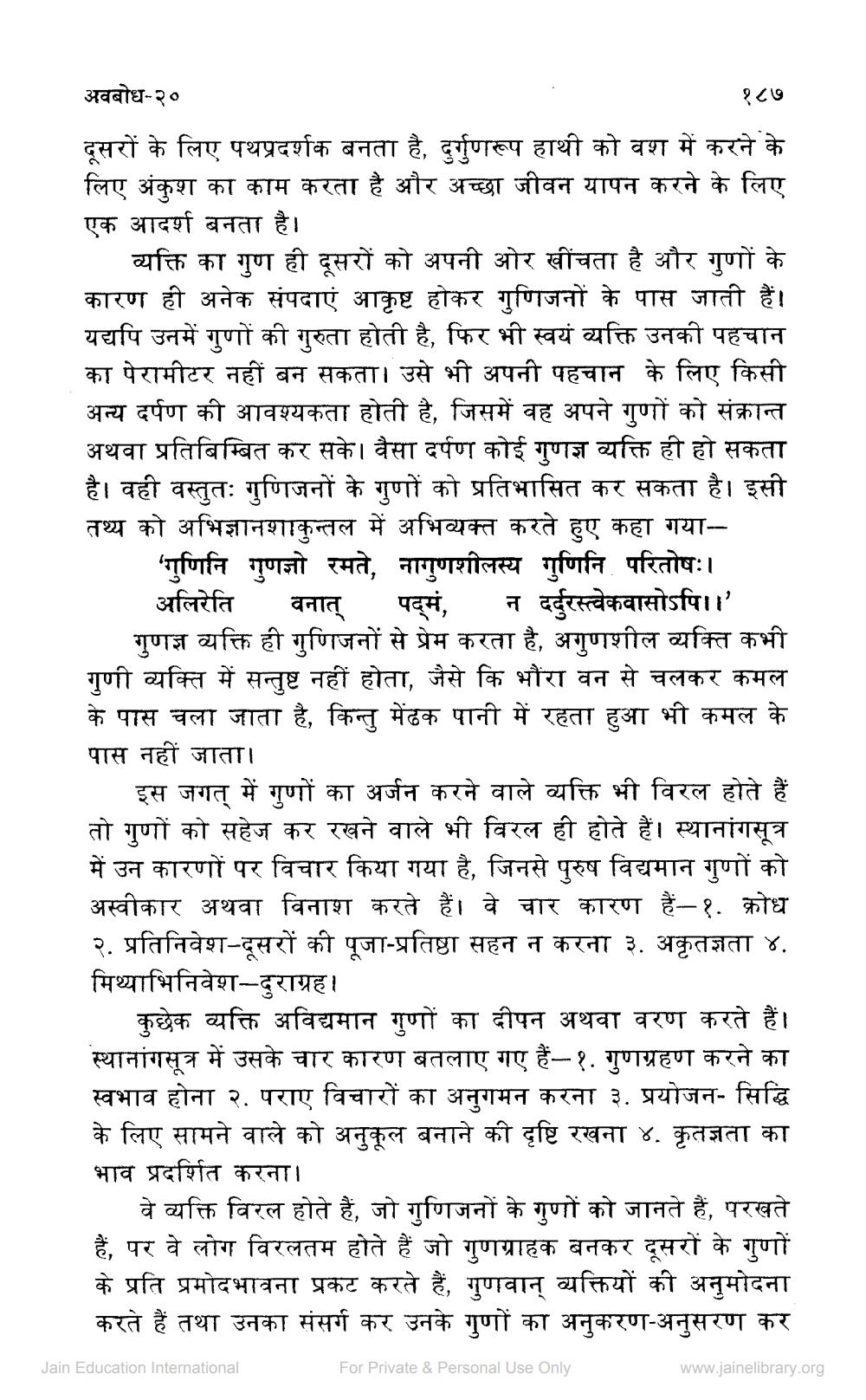________________
अवबोध- २०
१८७
दूसरों के लिए पथप्रदर्शक बनता है, दुर्गुणरूप हाथी को वश में करने के लिए अंकुश का काम करता है और अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक आदर्श बनता है।
व्यक्ति का गुण ही दूसरों को अपनी ओर खींचता है और गुणों के कारण ही अनेक संपदाएं आकृष्ट होकर गुणिजनों के पास जाती हैं। यद्यपि उनमें गुणों की गुरुता होती है, फिर भी स्वयं व्यक्ति उनकी पहचान का पेरामीटर नहीं बन सकता। उसे भी अपनी पहचान के लिए किसी अन्य दर्पण की आवश्यकता होती है, जिसमें वह अपने गुणों को संक्रान्त अथवा प्रतिबिम्बित कर सके। वैसा दर्पण कोई गुणज्ञ व्यक्ति ही हो सकता है । वही वस्तुतः गुणिजनों के गुणों को प्रतिभासित कर सकता है। इसी तथ्य को अभिज्ञानशाकुन्तल में अभिव्यक्त करते हुए कहा गया'गुणिनि गुणज्ञो रमते, नागुणशीलस्य गुणिनि परितोषः । अलिरेति वनात् पद्मं, न दर्दुरस्त्वेकवासोऽपि । । ' गुणज्ञ व्यक्ति ही गुणिजनों से प्रेम करता है, अगुणशील व्यक्ति कभी गुणी व्यक्ति में सन्तुष्ट नहीं होता, जैसे कि भौंरा वन से चलकर कमल के पास चला जाता है, किन्तु मेंढक पानी में रहता हुआ भी कमल के पास नहीं जाता।
इस जगत् में गुणों का अर्जन करने वाले व्यक्ति भी विरल होते हैं तो गुणों को सहेज कर रखने वाले भी विरल ही होते हैं। स्थानांगसूत्र में उन कारणों पर विचार किया गया है, जिनसे पुरुष विद्यमान गुणों को अस्वीकार अथवा विनाश करते हैं। वे चार कारण हैं - १. क्रोध २. प्रतिनिवेश - दूसरों की पूजा-प्रतिष्ठा सहन न करना ३. अकृतज्ञता ४. मिथ्याभिनिवेश - दुराग्रह ।
कुछेक व्यक्ति अविद्यमान गुणों का दीपन अथवा वरण करते हैं। स्थानांगसूत्र में उसके चार कारण बतलाए गए हैं - १. गुणग्रहण करने का स्वभाव होना २. पराए विचारों का अनुगमन करना ३. प्रयोजन- सिद्धि के लिए सामने वाले को अनुकूल बनाने की दृष्टि रखना ४. कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना ।
वे व्यक्ति विरल होते हैं, जो गुणिजनों के गुणों को जानते हैं, परखते हैं, पर वे लोग विरलतम होते हैं जो गुणग्राहक बनकर दूसरों के गुणों के प्रति प्रमोदभावना प्रकट करते हैं, गुणवान् व्यक्तियों की अनुमोदना करते हैं तथा उनका संसर्ग कर उनके गुणों का अनुकरण अनुसरण कर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org