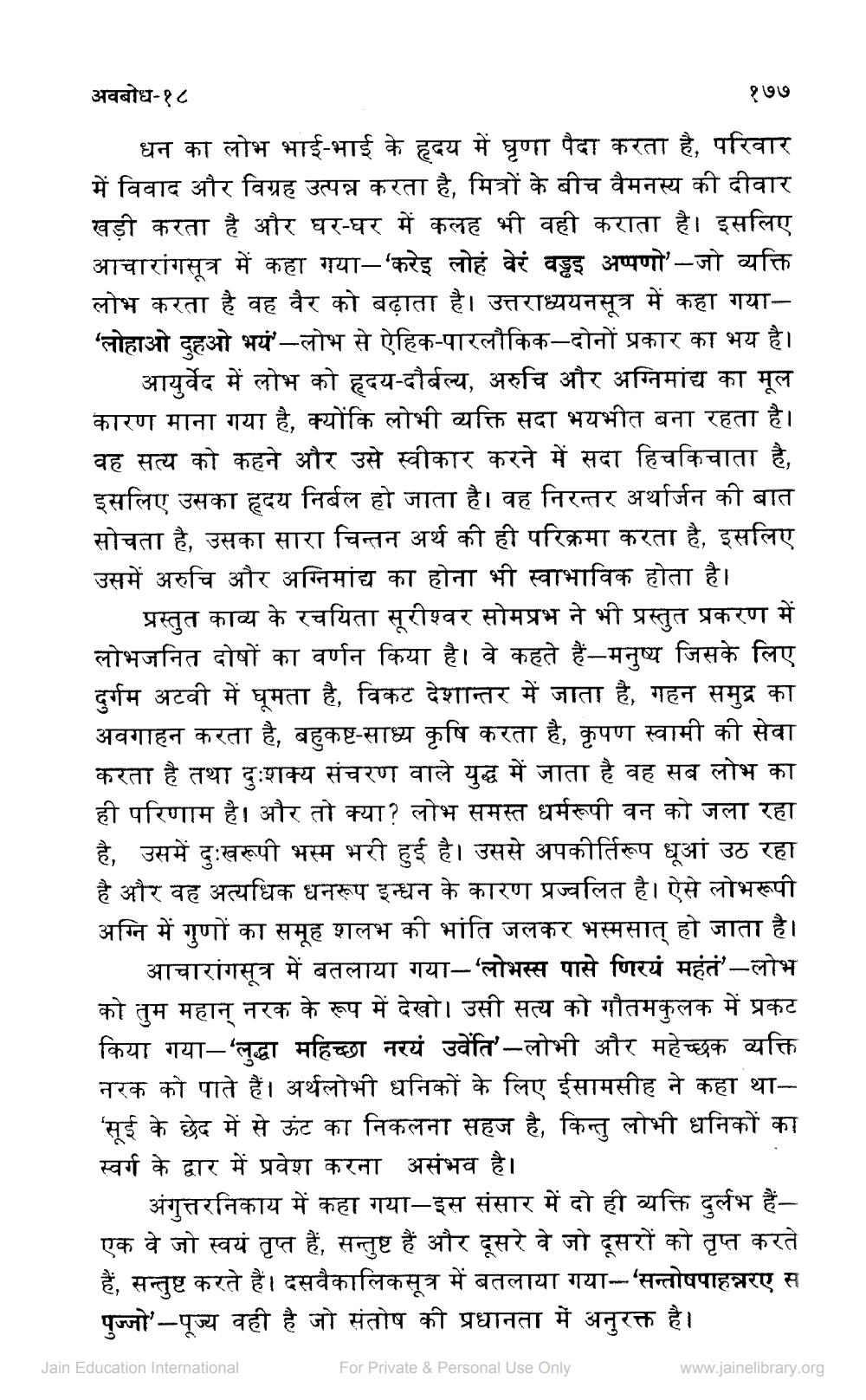________________
अवबोध-१८
१७७
धन का लोभ भाई-भाई के हृदय में घृणा पैदा करता है, परिवार में विवाद और विग्रह उत्पन्न करता है, मित्रों के बीच वैमनस्य की दीवार खड़ी करता है और घर-घर में कलह भी वही कराता है। इसलिए आचारांगसूत्र में कहा गया- 'करेइ लोहं वेरं वड्डइ अप्पणो' -जो व्यक्ति लोभ करता है वह वैर को बढ़ाता है। उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया'लोहाओ दुहओ भयं'-लोभ से ऐहिक-पारलौकिक-दोनों प्रकार का भय है।
आयुर्वेद में लोभ को हृदय-दौर्बल्य, अरुचि और अग्निमांद्य का मूल कारण माना गया है, क्योंकि लोभी व्यक्ति सदा भयभीत बना रहता है। वह सत्य को कहने और उसे स्वीकार करने में सदा हिचकिचाता है, इसलिए उसका हृदय निर्बल हो जाता है। वह निरन्तर अर्थार्जन की बात सोचता है, उसका सारा चिन्तन अर्थ की ही परिक्रमा करता है, इसलिए उसमें अरुचि और अग्निमांद्य का होना भी स्वाभाविक होता है।
प्रस्तुत काव्य के रचयिता सूरीश्वर सोमप्रभ ने भी प्रस्तुत प्रकरण में लोभजनित दोषों का वर्णन किया है। वे कहते हैं-मनुष्य जिसके लिए दुर्गम अटवी में घूमता है, विकट देशान्तर में जाता है, गहन समुद्र का अवगाहन करता है, बहुकष्ट-साध्य कृषि करता है, कृपण स्वामी की सेवा करता है तथा दुःशक्य संचरण वाले युद्ध में जाता है वह सब लोभ का ही परिणाम है। और तो क्या? लोभ समस्त धर्मरूपी वन को जला रहा है, उसमें दुःखरूपी भस्म भरी हुई है। उससे अपकीर्तिरूप धूआं उठ रहा है और वह अत्यधिक धनरूप इन्धन के कारण प्रज्वलित है। ऐसे लोभरूपी अग्नि में गुणों का समूह शलभ की भांति जलकर भस्मसात् हो जाता है। ___ आचारांगसूत्र में बतलाया गया- 'लोभस्स पासे णिरयं महंतं'-लोभ को तुम महान् नरक के रूप में देखो। उसी सत्य को गौतमक्लक में प्रकट किया गया- 'लुद्धा महिच्छा नरयं उति'-लोभी और महेच्छक व्यक्ति नरक को पाते हैं। अर्थलोभी धनिकों के लिए ईसामसीह ने कहा था'सूई के छेद में से ऊंट का निकलना सहज है, किन्तु लोभी धनिकों का स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना असंभव है।
अंगुत्तरनिकाय में कहा गया इस संसार में दो ही व्यक्ति दुर्लभ हैंएक वे जो स्वयं तृप्त हैं, सन्तुष्ट हैं और दूसरे वे जो दूसरों को तृप्त करते हैं, सन्तुष्ट करते हैं। दसवैकालिकसूत्र में बतलाया गया- 'सन्तोषपाहन्नरए स पुज्जो'-पूज्य वही है जो संतोष की प्रधानता में अनुरक्त है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org