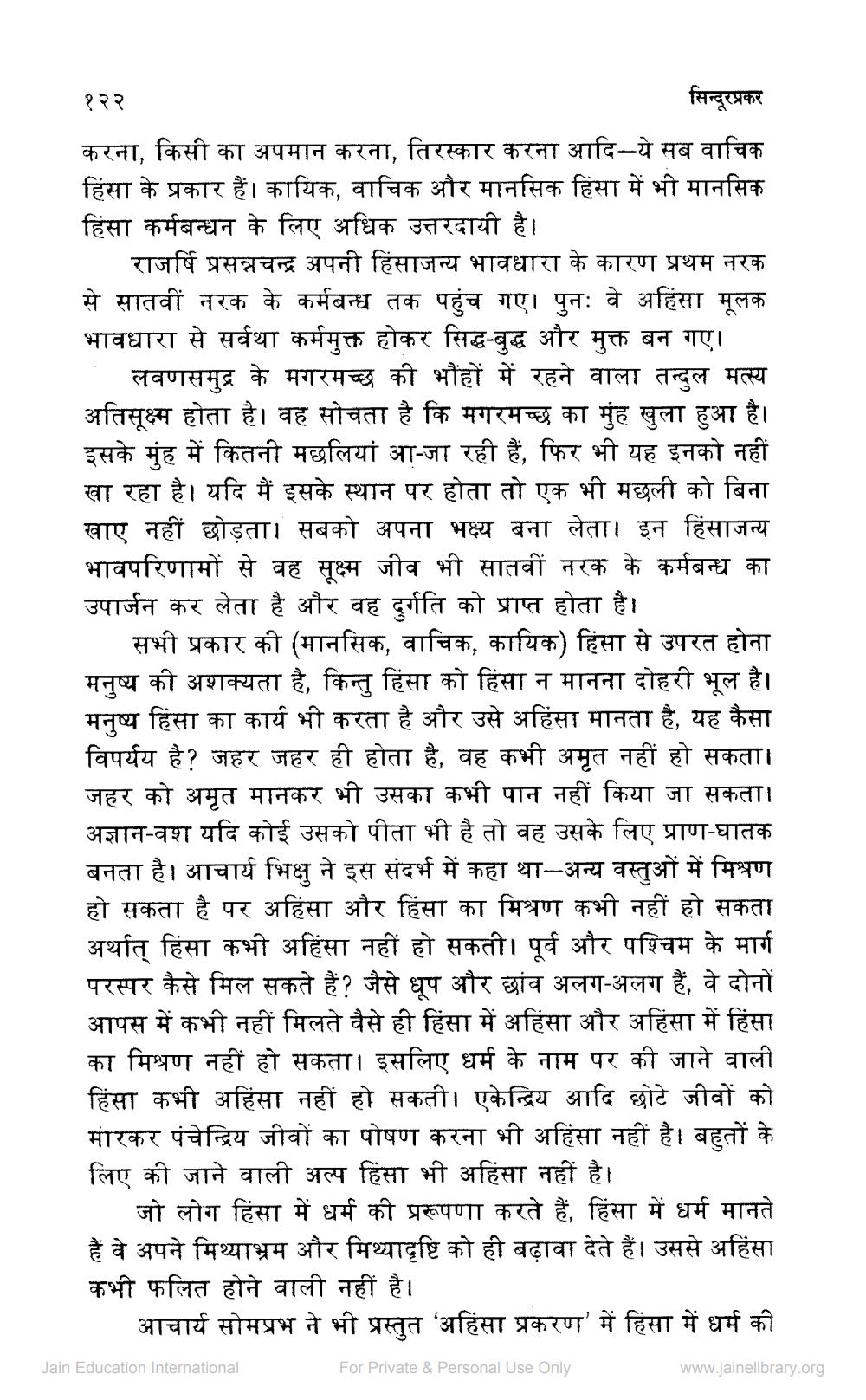________________
१२२
सिन्दूरप्रकर करना, किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना आदि-ये सब वाचिक हिंसा के प्रकार हैं। कायिक, वाचिक और मानसिक हिंसा में भी मानसिक हिंसा कर्मबन्धन के लिए अधिक उत्तरदायी है।
राजर्षि प्रसन्नचन्द्र अपनी हिंसाजन्य भावधारा के कारण प्रथम नरक से सातवीं नरक के कर्मबन्ध तक पहुंच गए। पुनः वे अहिंसा मूलक भावधारा से सर्वथा कर्ममुक्त होकर सिद्ध-बुद्ध और मुक्त बन गए।
लवणसमुद्र के मगरमच्छ की भौंहों में रहने वाला तन्दुल मत्स्य अतिसूक्ष्म होता है। वह सोचता है कि मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है। इसके मुंह में कितनी मछलियां आ-जा रही हैं, फिर भी यह इनको नहीं खा रहा है। यदि मैं इसके स्थान पर होता तो एक भी मछली को बिना खाए नहीं छोड़ता। सबको अपना भक्ष्य बना लेता। इन हिंसाजन्य भावपरिणामों से वह सूक्ष्म जीव भी सातवीं नरक के कर्मबन्ध का उपार्जन कर लेता है और वह दुर्गति को प्राप्त होता है।
सभी प्रकार की (मानसिक, वाचिक, कायिक) हिंसा से उपरत होना मनुष्य की अशक्यता है, किन्तु हिंसा को हिंसा न मानना दोहरी भूल है। मनुष्य हिंसा का कार्य भी करता है और उसे अहिंसा मानता है, यह कैसा विपर्यय है? जहर जहर ही होता है, वह कभी अमृत नहीं हो सकता। जहर को अमृत मानकर भी उसका कभी पान नहीं किया जा सकता। अज्ञान-वश यदि कोई उसको पीता भी है तो वह उसके लिए प्राण-घातक बनता है। आचार्य भिक्षु ने इस संदर्भ में कहा था-अन्य वस्तुओं में मिश्रण हो सकता है पर अहिंसा और हिंसा का मिश्रण कभी नहीं हो सकता अर्थात् हिंसा कभी अहिंसा नहीं हो सकती। पूर्व और पश्चिम के मार्ग परस्पर कैसे मिल सकते हैं? जैसे धूप और छांव अलग-अलग हैं, वे दोनों आपस में कभी नहीं मिलते वैसे ही हिंसा में अहिंसा और अहिंसा में हिंसा का मिश्रण नहीं हो सकता। इसलिए धर्म के नाम पर की जाने वाली हिंसा कभी अहिंसा नहीं हो सकती। एकेन्द्रिय आदि छोटे जीवों को मारकर पंचेन्द्रिय जीवों का पोषण करना भी अहिंसा नहीं है। बहुतों के लिए की जाने वाली अल्प हिंसा भी अहिंसा नहीं है।
जो लोग हिंसा में धर्म की प्ररूपणा करते हैं, हिंसा में धर्म मानते हैं वे अपने मिथ्याभ्रम और मिथ्यादृष्टि को ही बढ़ावा देते हैं। उससे अहिंसा कभी फलित होने वाली नहीं है। आचार्य सोमप्रभ ने भी प्रस्तुत 'अहिंसा प्रकरण' में हिंसा में धर्म की
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org