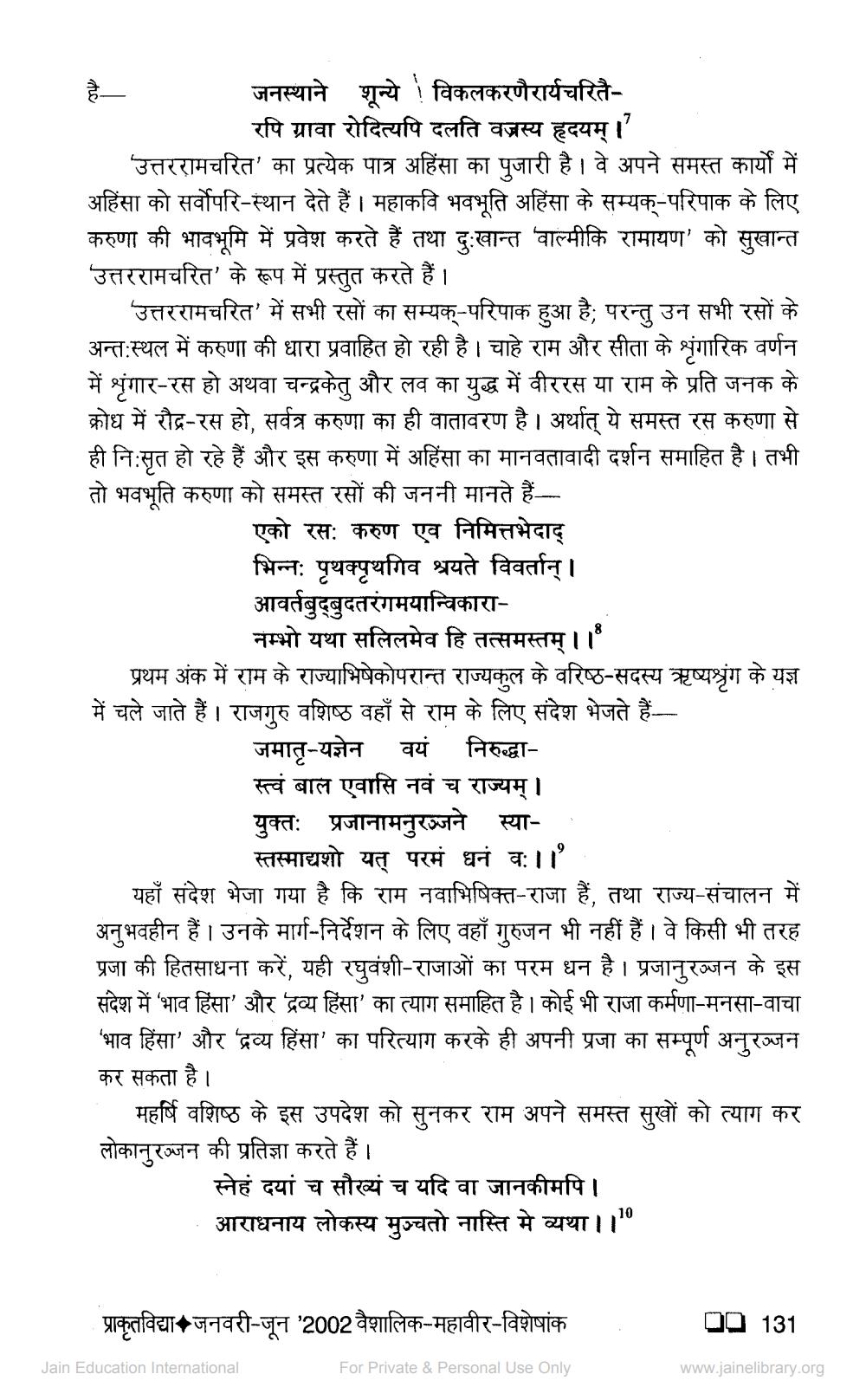________________
जनस्थाने शून्ये । विकलकरणैरार्यचरितै
रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम् ।' 'उत्तररामचरित' का प्रत्येक पात्र अहिंसा का पुजारी है। वे अपने समस्त कार्यों में अहिंसा को सर्वोपरि-स्थान देते हैं। महाकवि भवभूति अहिंसा के सम्यक-परिपाक के लिए करुणा की भावभूमि में प्रवेश करते हैं तथा दु:खान्त वाल्मीकि रामायण' को सुखान्त 'उत्तररामचरित' के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
'उत्तररामचरित' में सभी रसों का सम्यक्-परिपाक हुआ है; परन्तु उन सभी रसों के अन्त:स्थल में करुणा की धारा प्रवाहित हो रही है। चाहे राम और सीता के शृंगारिक वर्णन में श्रृंगार-रस हो अथवा चन्द्रकेतु और लव का युद्ध में वीररस या राम के प्रति जनक के क्रोध में रौद्र-रस हो, सर्वत्र करुणा का ही वातावरण है। अर्थात् ये समस्त रस करुणा से ही नि:सृत हो रहे हैं और इस करुणा में अहिंसा का मानवतावादी दर्शन समाहित है। तभी तो भवभूति करुणा को समस्त रसों की जननी मानते हैं
एको रस: करुण एव निमित्तभेदाद् भिन्न: पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान् । आवर्तबुद्बुदतरंगमयान्विकारा
नम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ।। प्रथम अंक में राम के राज्याभिषेकोपरान्त राज्यकुल के वरिष्ठ-सदस्य ऋष्यश्रृंग के यज्ञ में चले जाते हैं। राजगुरु वशिष्ठ वहाँ से राम के लिए संदेश भेजते हैं
जमातृ-यज्ञेन वयं निरुद्धास्त्वं बाल एवासि नवं च राज्यम् । युक्त: प्रजानामनुरजने स्या
स्तस्माद्यशो यत् परमं धनं वः।। यहाँ संदेश भेजा गया है कि राम नवाभिषिक्त-राजा हैं, तथा राज्य-संचालन में अनुभवहीन हैं। उनके मार्ग-निर्देशन के लिए वहाँ गुरुजन भी नहीं हैं। वे किसी भी तरह प्रजा की हितसाधना करें, यही रघुवंशी-राजाओं का परम धन है। प्रजानुरञ्जन के इस संदेश में भाव हिंसा' और 'द्रव्य हिंसा' का त्याग समाहित है। कोई भी राजा कर्मणा-मनसा-वाचा 'भाव हिंसा' और 'द्रव्य हिंसा' का परित्याग करके ही अपनी प्रजा का सम्पूर्ण अनुरञ्जन कर सकता है। __महर्षि वशिष्ठ के इस उपदेश को सुनकर राम अपने समस्त सुखों को त्याग कर लोकानुरञ्जन की प्रतिज्ञा करते हैं।
स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि। आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ।।"
प्राकृतविद्या-जनवरी-जून '2002 वैशालिक-महावीर-विशेषांक
00 131
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org