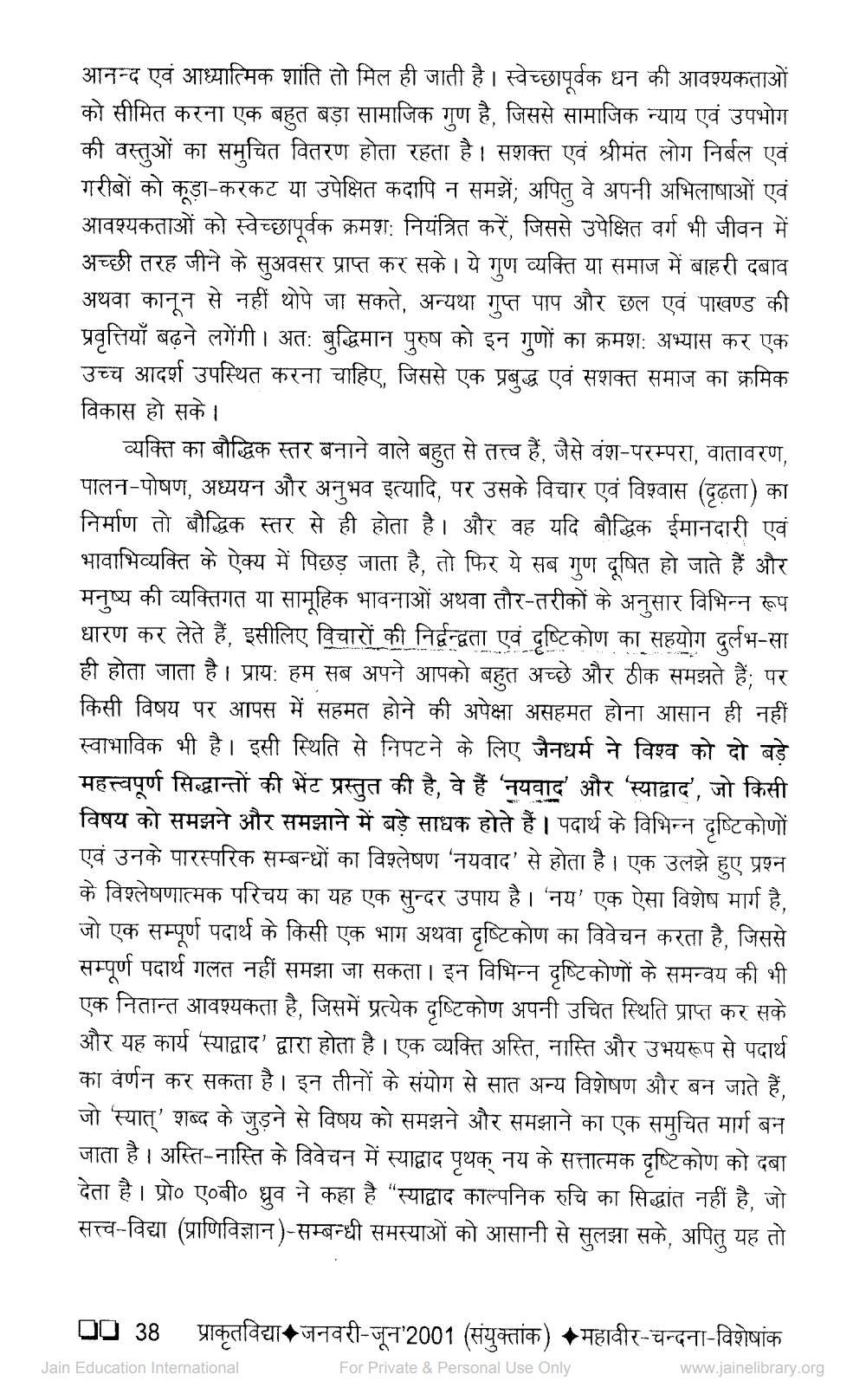________________
आनन्द एवं आध्यात्मिक शांति तो मिल ही जाती है। स्वेच्छापूर्वक धन की आवश्यकताओं को सीमित करना एक बहुत बड़ा सामाजिक गुण है, जिससे सामाजिक न्याय एवं उपभोग की वस्तुओं का समुचित वितरण होता रहता है। सशक्त एवं श्रीमंत लोग निर्बल एवं गरीबों को कूड़ा-करकट या उपेक्षित कदापि न समझें; अपितु वे अपनी अभिलाषाओं एवं आवश्यकताओं को स्वेच्छापूर्वक क्रमश: नियंत्रित करें, जिससे उपेक्षित वर्ग भी जीवन में अच्छी तरह जीने के सुअवसर प्राप्त कर सके। ये गुण व्यक्ति या समाज में बाहरी दबाव अथवा कानून से नहीं थोपे जा सकते, अन्यथा गुप्त पाप और छल एवं पाखण्ड की प्रवृत्तियाँ बढ़ने लगेंगी। अत: बुद्धिमान पुरुष को इन गुणों का क्रमश: अभ्यास कर एक उच्च आदर्श उपस्थित करना चाहिए, जिससे एक प्रबुद्ध एवं सशक्त समाज का क्रमिक विकास हो सके।
__व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बनाने वाले बहुत से तत्त्व हैं, जैसे वंश-परम्परा, वातावरण, पालन-पोषण, अध्ययन और अनुभव इत्यादि, पर उसके विचार एवं विश्वास (दृढ़ता) का निर्माण तो बौद्धिक स्तर से ही होता है। और वह यदि बौद्धिक ईमानदारी एवं भावाभिव्यक्ति के ऐक्य में पिछड़ जाता है, तो फिर ये सब गुण दूषित हो जाते हैं और मनुष्य की व्यक्तिगत या सामूहिक भावनाओं अथवा तौर-तरीकों के अनुसार विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, इसीलिए विचारों की निर्द्वन्द्वता एवं दृष्टिकोण का सहयोग दुर्लभ-सा ही होता जाता है। प्राय: हम सब अपने आपको बहुत अच्छे और ठीक समझते हैं; पर किसी विषय पर आपस में सहमत होने की अपेक्षा असहमत होना आसान ही नहीं स्वाभाविक भी है। इसी स्थिति से निपटने के लिए जैनधर्म ने विश्व को दो बड़े महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों की भेंट प्रस्तुत की है, वे हैं 'नयवाद' और 'स्याद्वाद', जो किसी विषय को समझने और समझाने में बड़े साधक होते हैं। पदार्थ के विभिन्न दृष्टिकोणों एवं उनके पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण 'नयवाद' से होता है। एक उलझे हुए प्रश्न के विश्लेषणात्मक परिचय का यह एक सुन्दर उपाय है। 'नय' एक ऐसा विशेष मार्ग है, जो एक सम्पूर्ण पदार्थ के किसी एक भाग अथवा दृष्टिकोण का विवेचन करता है, जिससे सम्पूर्ण पदार्थ गलत नहीं समझा जा सकता। इन विभिन्न दृष्टिकोणों के समन्वय की भी एक नितान्त आवश्यकता है, जिसमें प्रत्येक दृष्टिकोण अपनी उचित स्थिति प्राप्त कर सके और यह कार्य 'स्याद्वाद' द्वारा होता है। एक व्यक्ति अस्ति, नास्ति और उभयरूप से पदार्थ का वर्णन कर सकता है। इन तीनों के संयोग से सात अन्य विशेषण और बन जाते हैं, जो स्यात्' शब्द के जुड़ने से विषय को समझने और समझाने का एक समुचित मार्ग बन जाता है। अस्ति-नास्ति के विवेचन में स्याद्वाद पथक नय के सत्तात्मक दृष्टिकोण को दबा देता है। प्रो० ए०बी० ध्रुव ने कहा है “स्याद्वाद काल्पनिक रुचि का सिद्धांत नहीं है, जो सत्त्व-विद्या (प्राणिविज्ञान)-सम्बन्धी समस्याओं को आसानी से सुलझा सके, अपितु यह तो
40 38 प्राकृतविद्या-जनवरी-जून'2001 (संयुक्तांक) + महावीर-चन्दना-विशेषांक Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org