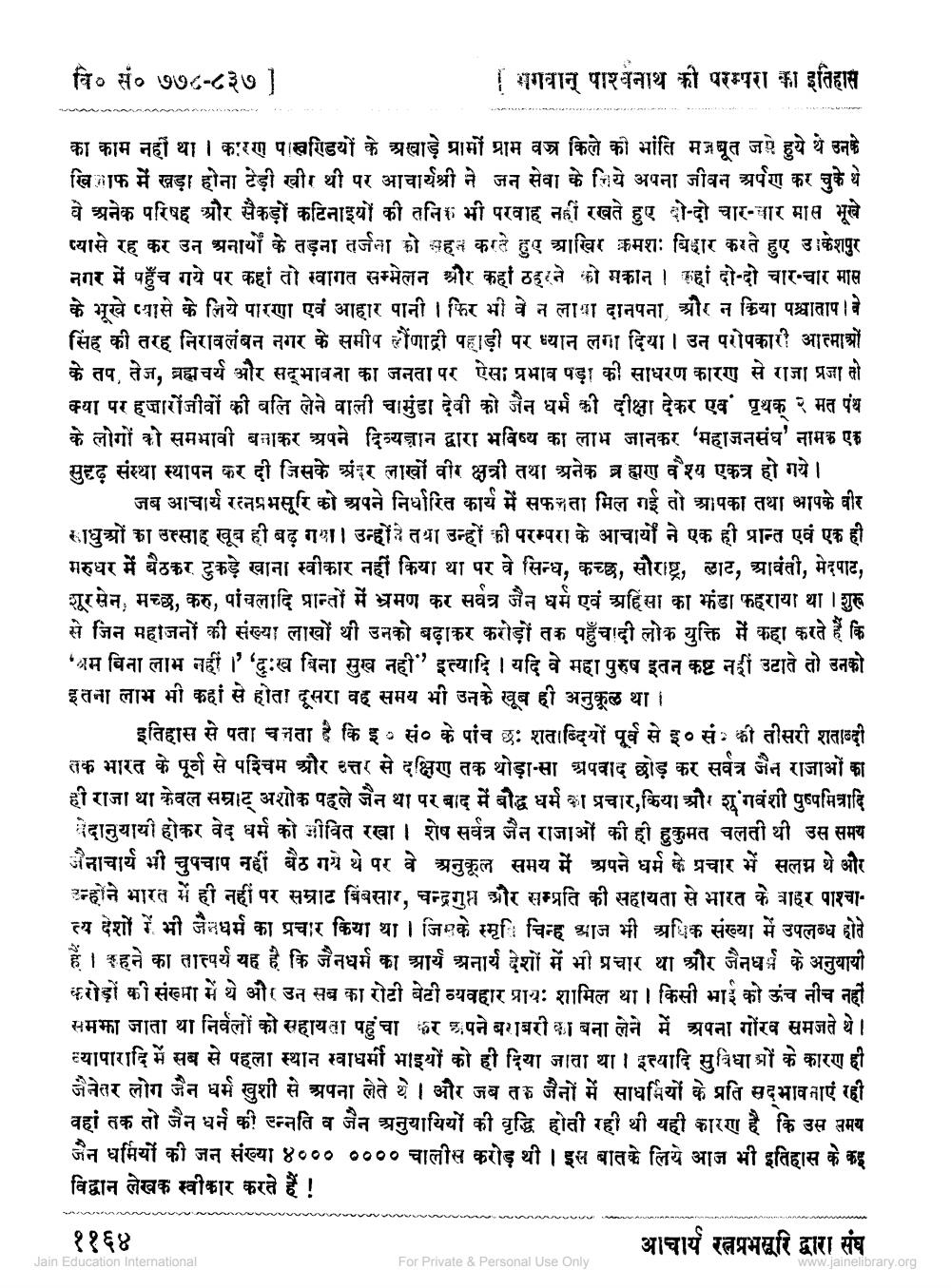________________
वि० सं० ७७८-८३७ ]
। भगवान् पाश्वनाथ की परम्परा का इतिहास
का काम नहीं था । कारण पाखण्डियों के अखाड़े प्रामों प्राम वज्र किले की भांति मजबूत जपे हुये थे उनके खिलाफ में खड़ा होना टेड़ी खीर थी पर आचार्यश्री ने जन सेवा के लिये अपना जीवन अर्पण कर चुके थे वे अनेक परिषह और सैकड़ों कटिनाइयों की तनिक भी परवाह नहीं रखते हुए दो-दो चार-चार मास भूखे प्यासे रह कर उन अनार्यों के तड़ना तर्जना को सहन करते हुए आखिर क्रमशः बिधार करते हुए उकेशपुर नगर में पहुँच गये पर कहां तो स्वागत सम्मेलन और कहां ठहरने को मकान । कहां दो-दो चार-चार मास के भूखे प्यासे के लिये पारणा एवं आहार पानी । फिर भी वे न लाथा दानपना और न किया पश्चाताप । वे सिंह की तरह निरावलंबन नगर के समीप हौंणाद्री पहाड़ी पर ध्यान लगा दिया। उन परोपकारी आत्माओं के तप, तेज, ब्रह्मचर्य और सद्भावना का जनता पर ऐसा प्रभाव पड़ा की साधरण कारण से राजा प्रजा को क्या पर हजारोंजीवों की बलि लेने वाली चामुंडा देवी को जैन धर्म की दीक्षा देकर एवं पृथक् २ मत पंथ के लोगों को समभावी बनाकर अपने दिव्यज्ञान द्वारा भविष्य का लाभ जानकर 'महाजनसंघ' नामक एक सुदृढ़ संस्था स्थापन कर दी जिसके अंदर लाखों वीर क्षत्री तथा अनेक ब्रह्मण वैश्य एकत्र हो गये।
जब आचार्य रत्नप्रभसूरि को अपने निर्धारित कार्य में सफलता मिल गई तो श्रापका तथा आपके वीर साधुओं का उत्साह खूब ही बढ़ गया। उन्होंने तथा उन्हों की परम्परा के आचार्यों ने एक ही प्रान्त एवं एक ही मरुधर में बैठकर टुकड़े खाना स्वीकार नहीं किया था पर वे सिन्ध, कच्छ, सौराष्ट्र, लाट, अावंती, मेदपाट, शूर सेन, मच्छ, करु, पांचलादि प्रान्तों में भ्रमण कर सर्वत्र जैन धर्म एवं अहिंसा का झंडा फहराया था । शुरू से जिन महाजनों की संख्या लाखों थी उनको बढ़ाकर करोड़ों तक पहुँचादी लोक युक्ति में कहा करते हैं कि 'श्रम विना लाभ नहीं ।' 'दुःख बिना सुख नहीं' इत्यादि । यदि वे महा पुरुष इतन कष्ट नहीं उटाते तो उनको इतना लाभ भी कहां से होता दूसरा वह समय भी उनके खूब ही अनुकूल था।
। इतिहास से पता चलता है कि इ० सं० के पांच छः शताब्दियों पूर्व से इ०सं की तीसरी शताब्दी तक भारत के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक थोड़ा-सा अपवाद छोड़ कर सर्वत्र जैन राजाओं का ही राजा था केवल सम्राट अशोक पहले जैन था पर बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार,किया और शुगवंशी पुष्पमित्रादि वेदानुयायी होकर वेद धर्म को जीवित रखा। शेष सर्वत्र जैन राजाओं की ही हुकुमत चलती थी उस समय जैनाचार्य भी चुपचाप नहीं बैठ गये थे पर वे अनुकूल समय में अपने धर्म के प्रचार में सलग्न थे और उन्होंने भारत में ही नहीं पर सम्राट बिंबसार, चन्द्रगुप्त और सम्प्रति की सहायता से भारत के बाहर पाश्चात्य देशों में भी जैनधर्म का प्रचार किया था। जिसके स्मृति चिन्ह आज भी अधिक संख्या में उपलब्ध होते हैं । इहने का तात्पर्य यह है कि जैनधर्म का आर्य अनार्य देशों में भी प्रचार था और जैनधर्म के अनुयायी करोड़ों की संख्मा में थे और उन सब का रोटी बेटी व्यवहार प्रायः शामिल था। किसी भाई को ऊंच नीच नहीं समझा जाता था निर्वलों को सहायता पहुंचा कर छपने बराबरी का बना लेने में अपना गोरव समजते थे। व्यापारादि में सब से पहला स्थान स्वाधर्मी भाइयों को ही दिया जाता था। इत्यादि सुविधाओं के कारण ही जैनेतर लोग जैन धर्म खुशी से अपना लेते थे । और जब तक जैनों में साधर्मियों के प्रति सद्भावनाएं रही वहां तक तो जैन धर्न की उन्नति व जैन अनुयायियों की वृद्धि होती रही थी यही कारण है कि उस समय जैन धर्मियों की जन संख्या ४००० ०००० चालीस करोड़ थी । इस बात के लिये आज भी इतिहास के कई विद्वान लेखक स्वीकार करते हैं ! ११६४
आचार्य रत्नप्रभसरि द्वारा संघ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org