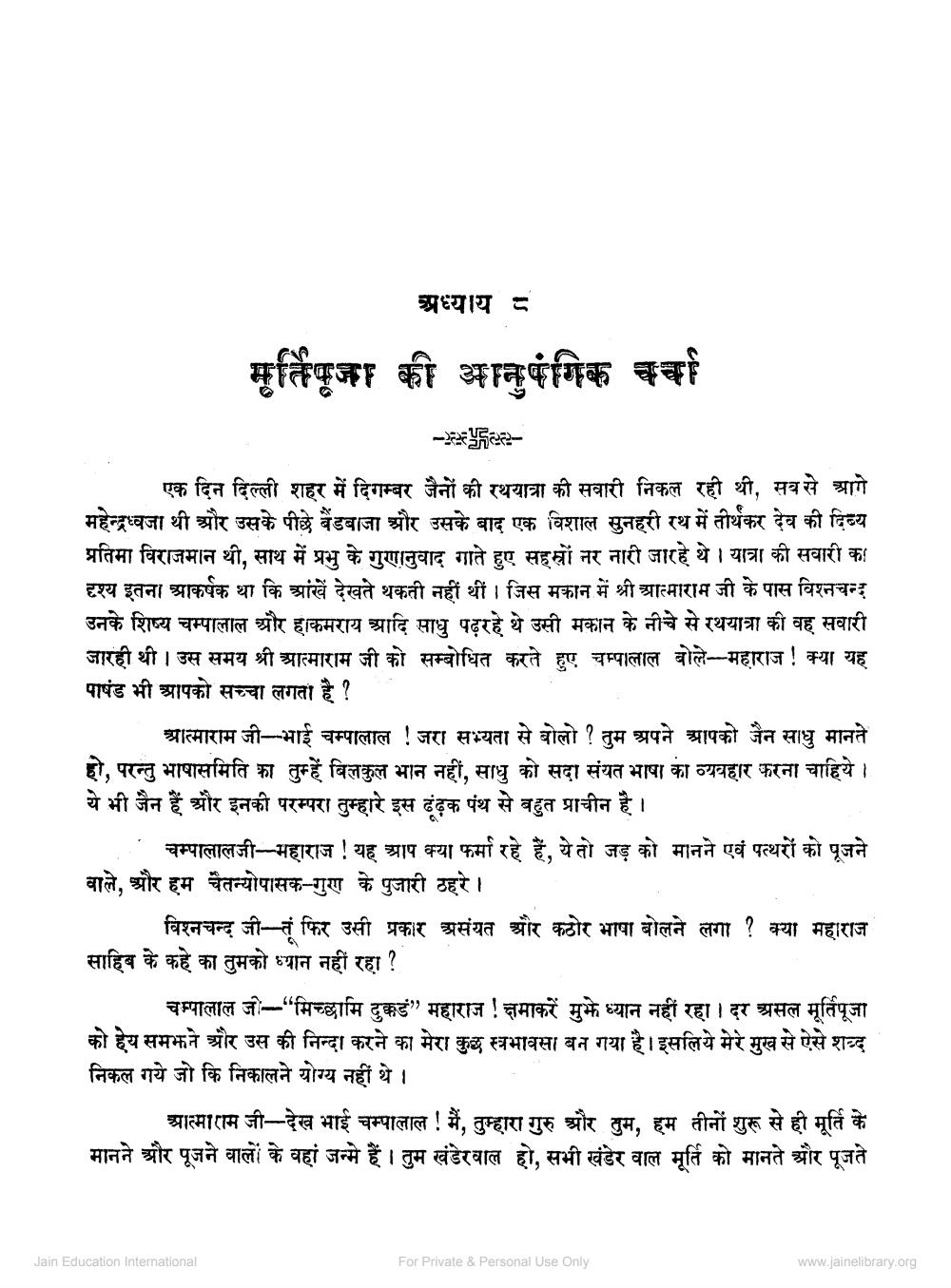________________
अध्याय ८ मूर्तिपूजा की आनुषंगिक चर्चा
एक दिन दिल्ली शहर में दिगम्बर जैनों की रथयात्रा की सवारी निकल रही थी, सबसे आगे महेन्द्रध्वजा थी और उसके पीछे बैंडबाजा और उसके बाद एक विशाल सुनहरी रथ में तीर्थंकर देव की दिव्य प्रतिमा विराजमान थी, साथ में प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए सहस्रों नर नारी जारहे थे । यात्रा की सवारी का दृश्य इतना आकर्षक था कि आंखें देखते थकती नहीं थीं । जिस मकान में श्री आत्माराम जी के पास विश्नचन्द उनके शिष्य चम्पालाल और हाकमराय आदि साधु पढ़रहे थे उसी मकान के नीचे से रथयात्रा की वह सवारी जारही थी। उस समय श्री आत्माराम जी को सम्बोधित करते हुए चम्पालाल बोले-महाराज ! क्या यह पाषंड भी आपको सच्चा लगता है ? ।
श्रात्माराम जी-भाई चम्पालाल ! जरा सभ्यता से बोलो ? तुम अपने आपको जैन साधु मानते हो, परन्तु भाषासमिति का तुम्हें बिलकुल भान नहीं, साधु को सदा संयत भाषा का व्यवहार करना चाहिये । ये भी जैन हैं और इनकी परम्परा तुम्हारे इस ढूंढ़क पंथ से बहुत प्राचीन है।
... चम्पालालजी-महाराज ! यह आप क्या फर्मा रहे हैं, ये तो जड़ को मानने एवं पत्थरों को पूजने वाले, और हम चैतन्योपासक-गुण के पुजारी ठहरे।
विश्नचन्द जी-तुं फिर उसी प्रकार असंयत और कठोर भाषा बोलने लगा ? क्या महाराज साहिब के कहे का तुमको ध्यान नहीं रहा ?
चम्पालाल जो-"मिच्छामि दुक्कडं” महाराज ! क्षमाकरें मुझे ध्यान नहीं रहा । दर असल मूर्तिपूजा को हेय समझने और उस की निन्दा करने का मेरा कुछ स्वभावसा बन गया है। इसलिये मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गये जो कि निकालने योग्य नहीं थे ।
आत्माराम जी-देख भाई चम्पालाल ! मैं, तुम्हारा गुरु और तुम, हम तीनों शुरू से ही मूर्ति के मानने और पूजने वालों के वहां जन्मे हैं । तुम खंडेरवाल हो, सभी खंडेर वाल मूर्ति को मानते और पूजते
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org