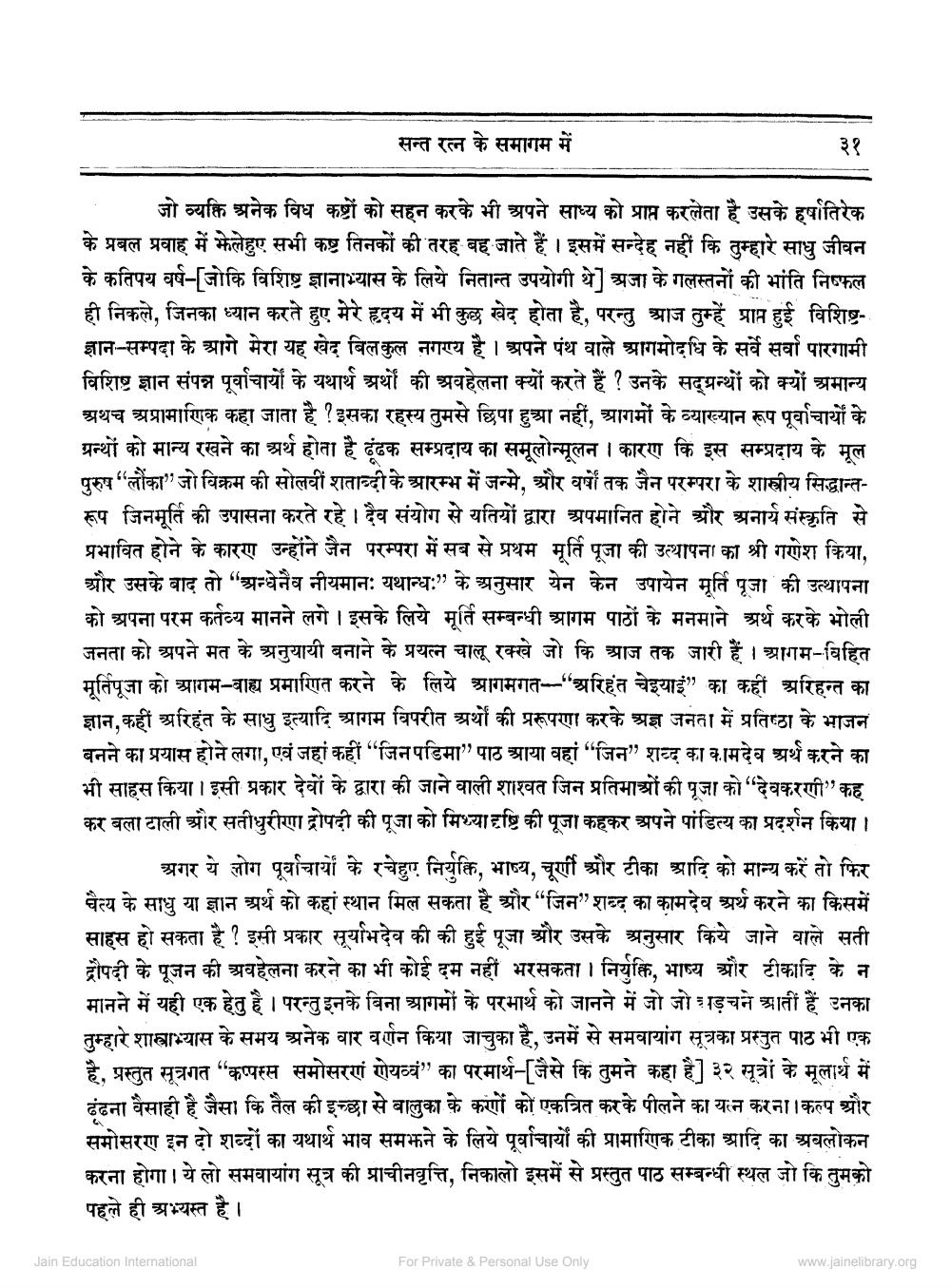________________
सन्त रत्न के समागम में
जो व्यक्ति अनेक विध कष्टों को सहन करके भी अपने साध्य को प्राप्त करलेता है उसके हर्षातिरेक के प्रबल प्रवाह में झेलेहुए सभी कष्ट तिनकों की तरह बह जाते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे साधु जीवन के कतिपय वर्ष-[जोकि विशिष्ट ज्ञानाभ्यास के लिये नितान्त उपयोगी थे] अजा के गलस्तनों की भांति निष्फल ही निकले, जिनका ध्यान करते हुए मेरे हृदय में भी कुछ खेद होता है, परन्तु आज तुम्हें प्राप्त हुई विशिष्टज्ञान-सम्पदा के आगे मेरा यह खेद बिलकुल नगण्य है । अपने पंथ वाले आगमोदधि के सर्वे सर्वा पारगामी विशिष्ट ज्ञान संपन्न पूर्वाचार्यों के यथार्थ अर्थों की अवहेलना क्यों करते हैं ? उनके सद्ग्रन्थों को क्यों अमान्य अथच अप्रामाणिक कहा जाता है ? इसका रहस्य तुमसे छिपा हुआ नहीं, आगमों के व्याख्यान रूप पूर्वाचार्यों के ग्रन्थों को मान्य रखने का अर्थ होता है ढूंढक सम्प्रदाय का समूलोन्मूलन । कारण कि इस सम्प्रदाय के मूल पुरुष “लौंका" जो विक्रम की सोलवीं शताब्दी के आरम्भ में जन्मे, और वर्षों तक जैन परम्परा के शास्त्रीय सिद्धान्तरूप जिनमूर्ति की उपासना करते रहे । दैव संयोग से यतियों द्वारा अपमानित होने और अनार्य संस्कृति से प्रभावित होने के कारण उन्होंने जैन परम्परा में सब से प्रथम मूर्ति पूजा की उत्थापना का श्री गणेश किया,
और उसके बाद तो “अन्धेनैव नीयमानः यथान्धः” के अनुसार येन केन उपायेन मूर्ति पूजा की उत्थापना को अपना परम कर्तव्य मानने लगे। इसके लिये मूर्ति सम्बन्धी आगम पाठों के मनमाने अर्थ करके भोली जनता को अपने मत के अनुयायी बनाने के प्रयत्न चालू रक्खे जो कि आज तक जारी हैं । आगम-विहित मूर्तिपूजा को आगम-बाह्य प्रमाणित करने के लिये आगमगत-"अरिहंत चेइयाई" का कहीं अरिहन्त का ज्ञान,कहीं अरिहंत के साधु इत्यादि आगम विपरीत अर्थों की प्ररूपणा करके अज्ञ जनता में प्रतिष्ठा के भाजन बनने का प्रयास होने लगा, एवं जहां कहीं "जिनपडिमा" पाठ आया वहां “जिन" शब्द का कामदेव अर्थ करने का भी साहस किया। इसी प्रकार देवों के द्वारा की जाने वाली शाश्वत जिन प्रतिमाओं की पूजा को “देवकरणी" कह कर बला टाली और सतीधुरीणा द्रोपदी की पूजा को मिथ्या दृष्टि की पूजा कहकर अपने पांडित्य का प्रदर्शन किया।
अगर ये लोग पूर्वाचार्यों के रचेहुए नियुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका आदि को मान्य करें तो फिर चैत्य के साधु या ज्ञान अर्थ को कहां स्थान मिल सकता है और “जिन" शब्द का कामदेव अर्थ करने का किसमें साहस हो सकता है ? इसी प्रकार सूर्याभदेव की की हुई पूजा और उसके अनुसार किये जाने वाले सती द्रौपदी के पूजन की अवहेलना करने का भी कोई दम नहीं भरसकता । नियुक्ति, भाष्य और टीकादि के न मानने में यही एक हेतु है । परन्तु इनके बिना आगमों के परमार्थ को जानने में जो जो अड़चने आती हैं उनका तुम्हारे शास्त्राभ्यास के समय अनेक वार वर्णन किया जाचुका है, उनमें से समवायांग सूत्रका प्रस्तुत पाठ भी एक है, प्रस्तुत सूत्रगत “कप्पस्स समोसरणं णेयव्वं" का परमार्थ-[जैसे कि तुमने कहा है] ३२ सूत्रों के मूलार्थ में ढंढना वैसाही है जैसा कि तैल की इच्छा से बालुका के कणों को एकत्रित करके पीलने का यत्न करना । कल्प और समोसरण इन दो शब्दों का यथार्थ भाव समझने के लिये पूर्वाचार्यों की प्रामाणिक टीका आदि का अवलोकन करना होगा। ये लो समवायांग सूत्र की प्राचीनवृत्ति, निकालो इसमें से प्रस्तुत पाठ सम्बन्धी स्थल जो कि तुमको पहले ही अभ्यस्त है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org